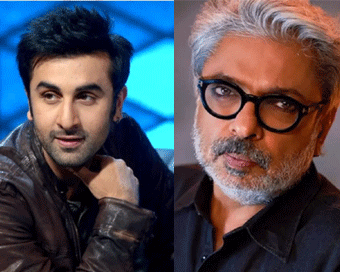विश्लेषण : वहशी भीड़ के खिलाफ
सरकारें जब नक्शे के जरिये देश के सूरतेहाल को बताने की कोशिश करती है तो लोगों को लगता है कि सरकार की यही भाषा है.
 विश्लेषण : वहशी भीड़ के खिलाफ |
देश के लोग इन दिनों देश के नक्शे के उन हिस्सों को लाल रंग करके बता रहे हैं कि किस-किस हिस्से में सांप्रदायिक सैन्य दस्ते खूनी-खेल खेल रहे हैं. जंतर-मंतर को देश के लोगों की नब्ज कहा जाता है. बेहद सूक्ष्म आवाजों को सुन लेने वाला इस नब्ज से बीमारियों को पकड़ लेता है. एक समूह, एक संगठन की जगह समाज का चेहरा जब जंतर-मंतर पर दिखने लगता है तो वह टेलीविजन चैनलों की टीआरपी तंत्र के रडार से बाहर से हो जाता है. जंतर-मंतर पर 28 जून को ‘नॉट इन माई नेम’ के बहाने जमा होने वाले लोग गाय और राष्ट्रवाद के नाम पर देशभर में जगह जगह होने वाले हमलों व हत्याओं की घटनाओं के विरोध में दिख रहे हो लेकिन वह यही तक सीमित नहीं लगती है. हमले और हत्याएं देश में तमाम स्तरों पर व्यक्त किए जा रहे रोष और विक्षोभ की प्राथमिकता जरूर है.
इंदिरा गाधी ने जब आपातकाल लागू किया था और सेंसरशिप को उसकी आवश्यक शर्त बताया तो उनके सामने यह आशंका रत्तीभर भी नहीं थी कि वह उनके लिए इतिहास का वह काला अध्याय साबित होगा. संसदीय इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने वाले राजीव गांधी ने दलबदल विरोधी विधेयक और मानहानि विरोधी विधेयक के जरिये यह भरोसा कर लिया था कि उनकी सत्ता का बाल-बांका तक नहीं हो सकता है. तंत्र अपनी सुरक्षा के लिए समाज के भीतर तोड़ पैदा करता है मगर समाज के भीतर यही चेतना ठोस रूप में कायम है कि आपस की जोड़ ही उसके जिंदा रहने की पहली शर्त है और वह इसी चेतना से तंत्र के कांटों की तोड़ पैदा कर लेता है. उदाहरण है कि मजह दो वर्षो के भीतर एक तरह की कामयाब राजनीतिक गोलंबदी हो जाती है और दूसरी तरफ चंद दिनों में ही उसका गुब्बारा फूटने भी लगता है.
दरअसल, समाज के नब्ज को टटोलने की पद्धति क्या है? एक टीवी चैनल यह पद्धति अपना सकता है कि नरेन्द्र मोदी की सरकार के सच को दिखाने से उसकी टीआरपी गिर सकती है इसीलिए वह सच को दबाता और चौबीस घंटे के लिए वह खुद की सेंसरशिप की कवायद करता है, जिससे कि उसके अर्थतंत्र और टीआरपी के तंत्र का दोस्ताना रिश्ता बना रहें. लेकिन सरकार की समाज के नब्ज को सुनने की पद्धति वह नहीं हो सकती है. जैसे मध्य प्रदेश के एक ग्रामीण ने कहा कि सरकार को अर्थतंत्र चलाना है लेकिन हमें तो अपना समाज चलाना है. लोकतंत्र में अचानक कोई एक विषय सरकार के विरोध का चेहरा नहीं बनता है. विषय-दर-विषय की सतह तैयार होती है. इसीलिए जंतर-मंतर पर होने वाले किसी भी विरोध को टटोलने के लिए यह पद्धति अपनाई जाती है कि उसकी सतह में क्या है? वहां तत्कालिक तौर पर किसान नहीं दिखता है लेकिन उसकी छाया यदि उस विरोध में मौजूद रहती है जो कि कुछ दिनों पहले यहां से तमिलनाडु लौट गया था और जिसका स्वर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के किसानों से मिल रहा है तो उस विरोध को महज सांप्रदायिक सैन्य दस्तों द्वारा दलितों व मुसलमानों के खिलाफ गाय और राष्ट्र के नाम पर हमले और हत्या के विरोध तक सीमित नहीं देखा जा सकता है.
वहां यदि जेएनयू के छात्र भी मौजूद हैं तो उनके साथ शिक्षण संस्थानों में उनके हक हकूकों पर किए जा रहे हमलों का भी स्वर मौजूद है. वहां बारी-बारी से शिक्षण संस्थानों से लेकर सरकारी विभागों से पिछड़े वगरे के लिए आरक्षण को खत्म करने के खिलाफ गुस्सा भी मौजूद है. दिल्ली मेट्रो रेल में बेतहाशा भाड़ा बढ़ाया गया, रेलवे में यात्रियों से ज्यादा-से-ज्यादा पैसे झटकने की पद्धति तैयार कर ली गई है, बैंकों में तरह-तरह के चार्ज के नाम पर ग्राहकों के खाते खाली किए जा रहे हैं आदि को मुख्य सवाल बनाकर यदि लोग सड़कों पर नहीं दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं लगाया जाना चाहिए कि लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया है. सत्ताधारी का तरीका ये होता है कि वह संविधान के समानांतर एक तंत्र को विकसित करने पर जोर देते हैं, जो कि समाज को ज्यादा-से-ज्यादा घुलने-मिलने की इजाजत देने के बजाय उनके भीतर दीवारे खड़ी कर सकें. मौजूदा सत्ताधारी लोगों के उस चेतना के केंद्र पर हमले कर रहा है जो वैचारिक विभाजन पैदा कर दें और सत्ता में हिस्सेदारी के टुकड़े की लालच पर ये विभाजन को आसान समझता है.
सत्ता में हिस्सेदारी के लालच ने ही 1947 से पहले सदियों से मिलजुल कर रहने की विचारधारा में वैचारिक विभाजन पैदा किया और देश बंटकर राष्ट्र बन गया. वैचारिक विभाजन के दो अस्त्र हैं. एक तरफ तो असुरक्षा का भाव पैदा करो और दूसरी तरफ हमलावर होने के लिए तैयार करो. यदि कोई ऐसी पद्धति हो जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि देश का बहुसंख्यक खुद को किन-किन स्तरों पर असुरक्षित महसूस करने लगे हैं तो उसकी वजहों में ये सामने आ सकता है कि संविधान के तंत्र के समानांतर सैन्यप्रवृति के दस्तों का तंत्र विकसित करने की एक प्रक्रिया चल रही है और उसके लिए संविधान के तंत्र का सर्वाधिक इस्तेमाल किया जा रहा है. संसदीय पार्टियां संविधान को धुरी बनाकर आपस में प्रतिद्धंदता करती है तो संसदीय लोकतंत्र के लिए इसे स्वस्थ कहा जा सकता है. लेकिन जब संविधान से इतर की धुरी पर संसदीय पार्टियां नाचने लगती हैं तो संसदीय लोकतंत्र के लिए वह सबसे मुश्किल की घड़ी होती है. इसीलिए संसदीय विपक्ष दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि वह संसद के दरवाजे पर छिपकर खड़ा है कि लोग जैसे ही संसद के बाहर दरवाजे पर पहुंचेंगे वह उसके आगे खड़े होकर नेतृत्व के ढोंग को पूरा कर सकता है.
पार्टियां अपने चरित्र में संसदीय भी नहीं रह गई है. वह नेताओं के समूह के रूप में दिखाई देने लगी है जहां इसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है कि सत्ताधारियों को संसद के दरवाजे से जब बाहर किया जाएगा तो उनमें सबसे आगे कौन होगा? संविधान के समानांतर सैन्य दस्तों को संविधान के तंत्रों की मदद से खड़े करने की इजाजत को इस वक्त सबसे बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है.
| Tweet |