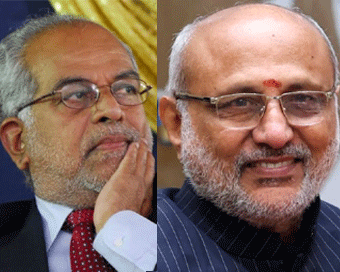प्राकृतिक आपदा : बरपता कहर, बढ़ती दुश्वारियां
भारत, अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविध भौगोलिक संरचना के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। लेकिन हर साल मानसून के आगमन के साथ यह देश प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आ जाता है। भारत में मानसून का मौसम जून से सितम्बर तक रहता है।
 प्राकृतिक आपदा : बरपता कहर, बढ़ती दुश्वारियां |
इस दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं अब आम हैं। हाल के महीनों में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में बादल फटने से भारी तबाही मची जिसमें कम से कम पांच लोगों की मौत हुई और 50 से अधिक लोग लापता हो गए। हिमाचल प्रदेश में भी अगस्त, 2025 में भारी बारिश के कारण दर्जनों सड़कें बंद हो गई और कई लोगों की जान चली गई। इन घटनाओं ने एक बार फिर सवाल उठाया है कि सरकारी तंत्र इन आपदाओं के प्रभाव को कम करने में क्यों विफल है?
बादल फटने की घटनाएं, जिन्हें भारत मौसम विज्ञान विभाग 100 मिमी. प्रति घंटे से अधिक बारिश के रूप में परिभाषित करता है, विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्रों में आम हैं। ये घटनाएं न केवल प्राकृतिक हैं, बल्कि जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों जैसे अनियोजित निर्माण, जंगलों की कटाई और नदियों के प्राकृतिक प्रवाह में हस्तक्षेप के कारण और भी घातक हो गई हैं।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल में अपने बयान में कहा कि पहाड़ी राज्यों में होने वाले निर्माण और नुकसान के लिए ‘घर में बैठकर तैयार की गई फर्जी डीपीआर बनाने वाले दोषी हैं। ये लोग बिना जमीनी हकीकत जाने डीपीआर बना देते हैं, जिससे ऐसे हादसे होते हैं।’ यह बयान न केवल सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि विकास परियोजनाओं में पारदर्शिता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी कितनी घातक हो सकती है। डीपीआर, जो किसी भी योजना का आधार होती है, में भ्रष्टाचार और लापरवाही बरती जाती है, तो इसका परिणाम ऐसे हादसों और त्रासदियों के रूप में सामने आता है। इसे ‘करप्शन ऑफ डिजाइन’ कहा जाता है।
हादसों ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार को पहले से तैयारी की जरूरत है। फिर भी, हर साल न सिर्फ एक जैसी आपदाएं दोहराई जाती हैं, बल्कि राहत और बचाव कार्य में अव्यवस्था भी दिखाई देती है। दूसरा, जल निकासी प्रणालियों की कमी और रखरखाव की अनदेखी भी बड़ा मुद्दा है। दिल्ली-एनसीआर जैसे शहरी क्षेत्रों, जहां 2024 में 108 मिमी. बारिश ने भारी जलभराव पैदा किया, में नालों की सफाई और उचित जल निकासी की कमी साफ दिखाई दी। पहाड़ी क्षेत्रों में नदियों के किनारे अनियोजित निर्माण और अतिक्रमण ने प्राकृतिक जल प्रवाह को बाधित किया है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
तीसरा, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और जागरूकता की कमी भी बड़ी समस्या है। ऐसे में स्थानीय ज्ञान का उपयोग करके सड़क निर्माण हो तो शायद भूस्खलन में रोकथाम हो सके। लेकिन स्थानीय लोगों की सलाह को नजरअंदाज किया जाता है और परियोजनाएं केवल ठेकेदारों और अधिकारियों के हितों को ध्यान में रख कर बनाई जाती हैं। इन समस्याओं का समाधान तभी संभव है, जब सरकार और समाज मिल कर एक समग्र और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। सबसे पहले, डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया को पारदर्शी और वैज्ञानिक बनाना होगा।
भूगर्भीय सर्वेक्षण, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन और स्थानीय विशेषज्ञों की राय को शामिल करना अनिवार्य होना चाहिए। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए स्वतंत्र ऑडिट और निगरानी तंत्र स्थापित किए जाने चाहिए। दूसरा, आपदा प्रबंधन के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करना होगा। इसमें न केवल राहत और बचाव की तैयारी शामिल होनी चाहिए, बल्कि प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, जैसे बादल फटने की निगरानी, को भी मजबूत करना होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग भूस्खलन और जलभराव की संभावना वाले स्थानों की पहचान के लिए किया जाना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास को भी प्राथमिकता देनी होगी। जंगलों की कटाई को रोकना, नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बहाल करना और अंधाधुंध निर्माण पर रोक लगाना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में इको-सेंसिटिव जोन में निर्माण को सख्ती से विनियमित करना होगा।
बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ की त्रासदियां केवल प्राकृतिक नहीं हैं, बल्कि मानवीय लापरवाही और भ्रष्टाचार का भी परिणाम हैं। अब समय है कि सरकार, समाज और विशेषज्ञ मिल कर ऐसी व्यवस्था बनाएं जो न केवल आपदाओं को रोके, बल्कि उनके प्रभाव को कम करने में भी सक्षम हो। टिकाऊ विकास, पारदर्शी प्रशासन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही इस दिशा में बढ़ने का रास्ता है।
(लेख में व्यक्त विचार निजी हैं)
| Tweet |