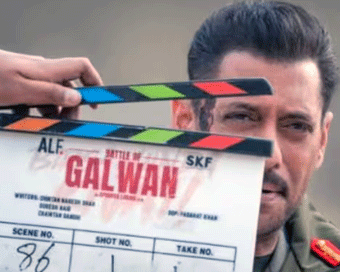विश्लेषण : पहले वाला भारत बनाना होगा
जब भी कोई ख्याति प्राप्त व्यक्ति आत्महत्या करता है तो पूरे देश में मातम का माहौल निर्मिंत किया जाता है। ऐसे हर व्यक्ति के फैन भारी संख्या में होते ही हैं।
 विश्लेषण : पहले वाला भारत बनाना होगा |
सुशांत सिंह के साथ अगर क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े को देखें तो उसी दिन 300 लोगों ने आत्महत्या की होगी। इस आंकडे के अनुसार औसतन एक लाख से ज्यादा लोग प्रतिवर्ष हमारे देश में अपनी जान लेते हैं। हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए महत्त्वपूर्ण होता है। उसके परिवार एवं रिश्तेदारों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि वह बड़ा व्यक्ति था या छोटा। उनके लिए वह जीवन भर का गम और कई परिवारों के लिए जो जीवन तक पर संकट छोड़ जाता है। इसलिए आप सुशांत के साथ उन लोगों के बारे में भी विचार करिए जिन्होंने किन मानसिक स्थितियों में अपनी जीवन लीला समाप्त की।
आत्महत्याओं पर विश्व भर में काफी शोध हुए हैं। आत्महत्या करने वाले व्यक्तियों की पृष्ठभूमि, उसकी संगति, पेशा, रिश्तेदारों-दोस्तों-परिवारजनों के साथ उसका व्यवहार, आत्महत्या के पहले की समस्त स्थितियां तथा अगर उसने कोई पत्र छोड़ा है तो उसके मजमून आदि के आधार पर किए गए अध्ययनों के असंख्य निष्कर्ष हमारे सामने हैं। पुलिस छानबीन की रिपोर्ट भी आपका इस संबंध में काफी ज्ञानवर्धन कर देगी। भारत के बारे में 2015-16 का स्वास्थ्य सर्वेक्षण बताता है कि यहां 15 प्रतिशत लोग किसी-न-किसी मानसिक रोग के शिकार हैं और हर 20 में से एक व्यक्ति किसी न किसी कारण से अवसाद की अवस्था में रहता है। मनोवैज्ञानिक इनका अलग तरह से विश्लेषण करते हैं और इनसे बचने के उपाय भी बताते हैं।
एलोपैथ मेडिकल साइंस इस समय दुनिया में मान्य है और उसके आधार पर मानसिक स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर, अस्पताल आदि से लेकर न जाने कितने प्रकार के सुझाव दिए जाते हैं। यह सच भी है कि मानसिक बीमारियों के उपचार और काउंसलिंग से काफी लोगों को अवसाद या आत्महत्या की भावना से बाहर निकाला गया है। किंतु विज्ञान केवल इसका पहलू नहीं है। भारतीय संदभरे में हमें मानसिक समस्याओं, आत्महत्या आदि का अलग दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। उम्र बढ़ने के साथ सामान्य तौर पर लोगों को इन बातों का ज्ञान हो जाता था कि मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है? यानी हमने मनुष्य के रूप में पैदा लिया तो हमारे कर्तव्य क्या हैं? हमारे लिए अनुकरणीय क्या हैं? अपने, परिवार, समाज, राष्ट्र ही नहीं, विश्व और सम्पूर्ण सृष्टि के प्रति हमारे कुछ दायित्व हैं। प्रकृति या ब्रह्माण्ड की वैविध्यपूर्ण सृजन में हम श्रेष्ठ हैं। जो सम्पूर्ण अध्यात्म की ओर प्रवृत्त हो गए उनके लिए मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य है, मोक्ष प्राप्त करना। यानी जिस महाकाल के हम अंश हैं अंत में हमें उसी में विलीन होने के लिए जीवन में सारे यत्न करने हैं। अपना जीवन समाप्त करना पाप है। भारत में उत्पन्न जितने भी पंथ-संप्रदाय हैं सबने रास्ते अलग-अलग बताए हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है। हमारे यहां निजता की वो कल्पना कभी नहीं रही और न समाज व्यवस्था ऐसी थी, जिसमें इसे महत्त्व दिया जाए जैसे आज के समय किया जाता है।
जब मनुष्य समष्टि के अंग के रूप में धरती पर आया है तो उसका जीवन किसी स्तर पर निजी कैसे हो सकता है? बचपन से चाहे श्रुति परंपरा द्वारा हो या पुस्तकों के माध्यम से ऐसे श्लोक, कविताएं, उपदेश, बोध कथाएं, कीर्तन, भजन आदि द्वारा व्यक्ति को उसकी व्यापकता और मनुष्य के नाते कर्तव्यों का ही बोध तो कराया जाता रहा है। पश्चिमी जीवन शैली और उस पर आधारित पूरी शिक्षा प्रणाली ने लगभग लाखों वर्षो की सभ्यता में विकसित मनुष्य को पूर्ण मनुष्य बनाने की स्वाभाविक प्रणाली को ध्वस्त कर दिया। हमारे यहां जो 40 संस्कार शास्त्रों ने बताए वे सारे इसी पर केंद्रित थे। आपको हर एक संस्कार द्वारा अहसास कराया जाता था कि मनुष्य के रूप में आप सृष्टि के श्रेष्ठतम कृति हो और आपका पूरा आचरण उसी अनुरूप होना चाहिए। जन्म दिवस उनमें से एक प्रमुख संस्कार है। आज जिस तरह जन्म दिवस मनाया जाता है उससे किसी बालक-बालिका को किस बात की प्रेरणा मिलती है?
वर्तमान शिक्षा प्रणाली में शिक्षित एवं जीवन शैली में ढले लोगों को यह बात आसानी से समझ में नहीं आएगी। किंतु आपको प्राचीन भारतीय व्यवस्था में, जिसकी पहले अंग्रेजों ने बाद में मैकाले के मानसपुत्रों और फिर झूठे वामपंथ एवं दलितवाद के नाम पर लानत-मलामत किया गया है, आत्महत्या के उदाहरण न के बराबर मिलेंगे। हमारे यहां जीवन का मूल सिद्धांत ही बताया गया चरैवेती-चरैवेती। ऐतरेय ब्राह्मण का रचयिता इतरा अर्थात शुद्र माता का पुत्र था, जिसे भूमि पुत्र कहा गया और इस कारण नाम ही महीदास पड़ा उसने ही चरैवेति मंत्र दिया। इसका एक ही अर्थ है ‘आगे चलो, आगे चलो, आगे बढ़ो और चलते रहो। चरैवेति मंत्र के अनुसार-‘लंबी प्रगति-यात्रा से थके हुए व्यक्ति में अवर्णनीय भव्यता आ जाती है। चाहे कोई कितना ही महान और महत्त्वपूर्ण व्यक्ति क्यों न हो, यदि वह प्रगति-पथ छोड़कर इस दुनिया में बेकार बैठता है, तो वह तुच्छ बन जाता है। प्रगति-पथ पर जो निरंतर चलता रहता है, परमात्मा उसका सखा और सहयात्री होता है। इसलिए हे यात्री..चलता चल। चलता चल!’ संयुक्त परिवार परंपरा, ग्राम समाज के सहकारी जीवन के विध्वंस के साथ एकाकीपन ही मनुष्य की नियति हो चुकी है। हर व्यक्ति, चाहे वह अपनी विधा में कितना बड़ा बन गया हो, कितना भी नाम और धन अर्जित कर चुका हो, हर क्षण भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। यानी जो कुछ हमने पाया उसे बनाए रखते हुए कैसे और पाया जाए यह सोच का केंद्रबिंदु हो गया है। जिन्हें प्राप्त नहीं हुआ या कोई एक अवसर पर विफल हो गए, पीछे रह गए वे सोचते हैं कि हमारा जीवन ही व्यर्थ हो गया, अब हम क्या करेंगे। जो इनके बीच में हैं यानी थोड़ा पाया वे ज्यादा की चाहत की चिंता में घिरे रहते हैं।
जिनकी पूरी जिंदगी गरीबी में बीत रही है उनकी मजबूरी और एकाकीपन हर क्षण भविष्य की चिंता में ग्रस्त किए रहता है। यही चार स्थितियां आज के मनुष्य की है। यही हर प्रकार की मानसिक व्यथा के पीछे है और उसमें केवल आत्महत्या ही नहीं, समाज एवं अपने प्रति अनेक प्रकार के अपराध कराता है। जिस भारत के बारे में गांधी जी कहते थे कि हम आजादी की लड़ाई दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए लड़ रहे हैं, उस भारत को हमने कहां पहुंचा दिया है इस पर विचार करिए और यह भी सोचिए कि भारत को फिर से कैसे भारत बनाया जाए। यही हमारी बहुतेरी त्रासदियों को रोकने तथा अधिकाधिक समस्याओं से उबरने का रास्ता है।
| Tweet |