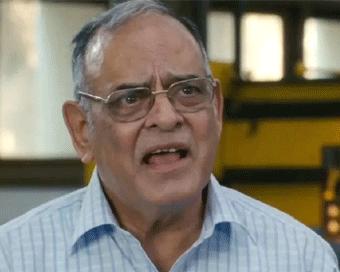कौशल विकास : तकनीकी शिक्षा से इतर
नव उदरावादी वैीकरण के दौर में जब पूंजी राष्ट्रीय सीमाओं से मुक्त हो चुकी है.
 कौशल विकास : तकनीकी शिक्षा से इतर |
बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी इकाइयों को कहां किस देश में स्थापित करेगी और कहां नहीं, काफी हद तक इस बात पर निर्भर है कि उस देश में उपलब्ध श्रम की कार्य कुशलता क्या है? तो ऐसे में अगर ‘इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2018’ अगर कौशल विकास के लिए हो रहे सरकार के प्रयासों की सराहना करता है, तो ये वाकई एक उत्साहजनक स्थिति है. मगर वहीं कुछ ऐसी भी बातें इस रिपोर्ट में है, जो कहीं-न-कहीं यह बता रही है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है.
ऑनलाइन पद्धति से किए सर्वेक्षण में 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के5,200 संस्थानों के 5,100,000 छात्रों के रोजगार कुशलता का आकलन किया गया. रिपोर्ट की अगर हम पहले सकारात्मक पहलुओं की चर्चा पहले करे तो जहां नई सरकार के आने के साल यानी 2014 में 33. प्रतिशत स्नातक रोजगार के लायक थे, वहीं अब 45.6 प्रतिशत हैं. पिछले साल के मुकाबले देखे तो वृद्धि 5.16 प्रतिशत की हुई है. रोजगारकुशल युवाओं के मामले में दिल्ली शीर्ष पर रहा, जिसके बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल का स्थान है.
वैसे योग्यता के स्तर में सुधार पूरे देश में हुआ है. अलग-अलग विषयों में देखें तो इंजीनियरिंग के आधे से ज्यादा , 51.52 प्रतिशत छात्र रोजगार के लायक हैं, वहीं बी.फार्मा के लगभग आधे, 47. 78 प्रतिशत छात्र रोजगार के लायक हैं. पिछले वर्ष के मुकाबले सबसे ज्यादा 12 प्रतिशत का उछाल एमसीए के छात्रों के रोजगारकुशलता में आया है. रिपोर्ट बताती है कि 2014 से 2017 के बीच 20 से 26 मिलियन लोगों को सरकारी योजनाओ, बढ़ी हुई भर्तियां, बढ़ती उद्यमशीलता और स्वतंत्र कार्य के परिणामस्वरूप लाभकारी रोजगारकी प्राप्ति हुई. लेकिन दूसरी तरफ एमबीए के छात्रों के रोजगारकुशलता में 3 फीसद की गिरावट आई है, पिछले साल जहां 42.28 प्रतिशत छात्र रोजगार के लायक थे; इस वर्ष सिर्फ 39.4 प्रतिशत छात्र रोजगार के लायक हैं. बी.कॉम करने वाले सिर्फ एक तिहाई छात्र ही रोजगार के लायक हैं, जबकि पिछले साल ये आकड़े 37. 98 प्रतिशत थे. मगर दो सबसे ज्यादा चिंताजनक पहलू जिन पर रिपोर्ट ध्यान दिलाती हैं; वो है- एक तो कम कुशल, प्रारंभिक चरण के बाद स्कूल छोड़ कर श्रमिकों में शामिल होने वालो अपेक्षाकृत गरीब छात्रों को रोजगारकुशल बनाना अभी भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य बना हुआ है. ऐसे में जब अभी भी देश में उच्च शिक्षा की दर बहुत कम है. राष्ट्रीय प्रशिक्षण परिषद द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर एक बार फिर से ध्यान देने की जरूरत साफ दिखाई दे रही है. दूसरी ओर, पुरु षों की रोजगार क्षमता बढ़ रही है. जहां रोजगार लायक पुरु षों का प्रतिशत पिछले साल के 40 से बढ़ के इस वर्ष 47 प्रतिशत दर्ज किया गया, वहीं महिलाओं के रोजगार क्षमता में पिछले साल के मुकाबले इस साल एक प्रतिशत की कमी दर्ज की गई और ये 40 रह गई है. महत्त्वपूर्ण बात ये भी कि, न सिर्फ रोजगार कुशलता बल्कि श्रमबल में भी महिलाओं की भागीदारी घट रही है. रिपोर्ट में खुद भी माना गया है कि पिछले दशक में महिलाओं की भागीदारी चिंताजनक तरीके से घटी और 2016 में ये सिर्फ 29 प्रतिशत रह गई. दक्षिण एशिया में लैंगिक असमानता को लेकर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पहले भी अपने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 में चिंता जता चुका है. हालांकि कॉपरेरेट सेक्टर लैंगिक समानता को ले कर न सिर्फ संवेदनशील बल्कि प्रयासरत भी दिख रहा है.
पुरु ष-महिला अनुपात जो अभी वर्तमान में 77:23 है, उसे 65:35 करने का लक्ष्य रखा गया है. ‘पीपुल्स स्ट्रांग’ द्वारा किए गए भर्ती आशय सर्वेक्षण में 49 प्रतिशत नियोक्ताओं ने पिछले साल की तुलना में इस साल भर्ती में वृद्धि की उम्मीद की है. इन क्षेत्रों में बैंकिंग और वित्तीय सेवा, बीपीओ, बीमा, यात्रा, आतिथ्य और आईटी विशेष तौर से शामिल हैं. जिन कौशलों की सबसे ज्यादा जरूरत बताई गई है, वो डेटा एनालिटिक्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आर्टििफशियल इंटेलीजेंस, रोबोटिक्स, कॉन्सेप्ट डिजाइन आदि हैं. इन क्षेत्रों में नये रोजगार की सम्भावनाएं हैं. एक और ध्यान देने की बात यह है कि लगभग 69 फीसद नियोक्ता सहमत हैं कि आर्टििफशियल इंटेलीजेंस भविष्य में नौकरियों की संख्या को प्रभावित करेगा. ऐसे में संवाद-कुशलता, नैतिकता, व्यवहार-कुशलता, रचनात्मकता, जैसे गुणों को नियोक्ताओं द्वारा अधिक महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है. जो भविष्य में शिक्षा पद्धति में भी बदलाव की जरूरत होने के तरफ भी इशारा कर रहे हैं.
| Tweet |