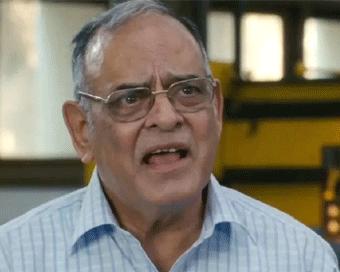स्वास्थ्य क्षेत्र : अविश्वास का इलाज जरूरी
वर्ष 2017 के उत्तरार्ध में दिल्ली और गुड़गांव के निजी अस्पतालों में ज्यादा फीस वसूले जाने तथा लापरवाही के मुद्दों ने मीडिया और आम जनता का खासा ध्यान खींचा.
 स्वास्थ्य क्षेत्र : अविश्वास का इलाज जरूरी |
.jpg) नतीजतन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों से अस्पतालों के सख्त नियमन को कहा. अब कई हफ्तों बाद जैसे सब कुछ भुला दिया गया है, और लगता है कि ‘तौर-तरीके’ पुराने र्ढे पर लौट आए हैं. जनवरी, 2018 के मध्य में किए एक सव्रेक्षण से पता चला कि दस में से नौ लोगों को देश की स्वास्थ्य प्रणाली पर विश्वास नहीं है. स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सुविधाओं और प्रदाताओं के खिलाफ हिंसा की खबरों (जो देश के प्रत्येक हिस्से से मिल रही हैं) से भी इसकी पुष्टि होती है. दिल्ली, गुड़गांव और गोरखपुर की हालिया घटनाओं से लोगों और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच बढ़ते ‘अविश्वास’ की तस्दीक होती है.
नतीजतन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों से अस्पतालों के सख्त नियमन को कहा. अब कई हफ्तों बाद जैसे सब कुछ भुला दिया गया है, और लगता है कि ‘तौर-तरीके’ पुराने र्ढे पर लौट आए हैं. जनवरी, 2018 के मध्य में किए एक सव्रेक्षण से पता चला कि दस में से नौ लोगों को देश की स्वास्थ्य प्रणाली पर विश्वास नहीं है. स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सुविधाओं और प्रदाताओं के खिलाफ हिंसा की खबरों (जो देश के प्रत्येक हिस्से से मिल रही हैं) से भी इसकी पुष्टि होती है. दिल्ली, गुड़गांव और गोरखपुर की हालिया घटनाओं से लोगों और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच बढ़ते ‘अविश्वास’ की तस्दीक होती है.
भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता की बाबत कुछ ज्यादा नहीं कहा जा सकता. अलबत्ता, उपलब्ध जानकारी से संकेत मिलता है कि स्वास्थ्य सेवाएं गुणवत्तापूर्ण नहीं हैं. यह स्थिति सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों में है. लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की मंशा सीमित है. अलबत्ता, हालिया घटनाओं से सबक जरूर सीखे जा सकते हैं, और तद्नुसार काफी कुछ किया जा सकता है. भारत में नियामकीय माहौल और नियम-कायदों का अनुपालन करने में समाज तत्पर नहीं दिखता. स्वास्थ्य क्षेत्र अपवाद नहीं है. आये दिन हम लोगों को यातायात संकेतों की अनदेखी करते देखते हैं, और उनमें ज्यादातर सजा से बच निकलते हैं. सीट बेल्ट और हेल्मेट कानूनन अनिवार्य हैं, लेकिन बड़े शहरों के अलावा इस नियम की शायद ही कहीं अनुपालना होती हो. बल्कि कानून की पालना करने वालों को ऐसी अनुशासनहीनता निरुत्साहित कर देती है. केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए क्लीनिकल एस्टेबलिशमेंट (रजिस्ट्रेशन एंड रेग्यूलेशन) एक्ट, 2010 को अधिकांश राज्यों ने अंगीकृत या क्रियान्वित नहीं किया है. राज्य सरकारें नियमन की दिशा में कोई प्रयास करती हैं, तो चिकित्सा क्षेत्र के शक्तिशाली संगठन विरोध में उतर आते हैं. कहना यह कि नियामक प्रावधान हैं, लेकिन समस्या उनकी अनुपालना कराने की है. सरकार को सबसे पहले सरकारी क्षेत्र के लिए तैयार किए जा चुके इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टेंर्डडस (आईपीएचएस) लागू कराने चाहिए.
अनजाने में ही सही लेकिन सरकारों ने बार-बार संकेत दिए हैं कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उसके दो पृथक पैमाने हैं. जहां दिल्ली के एक निजी अस्पताल (मैक्स शालीमार, 30 नवम्बर, 2017) में चिकित्सकीय चूक या लापरवाही पर अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया (जिसे अदालत ने बहाल कर दिया था) गया तो वहीं करीब-करीब ऐसी ही चूक दिल्ली के एक बड़े सरकारी अस्पताल (सफदरजंग हॉस्पिटल, नई दिल्ली, 18 जून, 2017) में हुई तो प्रतिक्रिया सिरे से अलग थी. गोरखपुर के अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति के अभाव और कथित लापरवाही से बच्चों की मौत वैसी ही त्रासदी है, जैसी दिल्ली के निजी अस्पतालों की त्रासदीपूर्ण घटनाएं.
भारत जैसे देश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए केवल सख्ती (नियम-कायदों) से ही बात नहीं बनेगी बल्कि प्रोत्साहन भी देने होंगे. सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों में प्रोत्साहन मुहैया कराने होंगे और तौर-तरीकों को चुस्त-दुरुस्त करना होगा ताकि गुणवत्ता मानकों और विनियमनों को उत्तरोत्तर लागू कराया जा सके. तथ्य स्वीकारना होगा कि किसी भी क्षेत्र में चिकित्सकीय चूक स्वाभाविक है. सर्वश्रेष्ठ मानी जाने वाली स्वास्थ्य प्रणालियों में भी शून्य चूक संभव नहीं है. स्वास्थ्य सेवाओं और उन्हें प्रदान करने वालों से वास्तविक अपेक्षाओं को तभी पूरा किया जा सकेगा जब जागरूकता बढाई जाए और जागरूक माहौल तैयार किया जाए. भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति लोगों का विश्वास जमाने पर ध्यान देना होगा. निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं और डॉक्टरों को भी स्व-नियमन की तरफ थोड़ा ध्यान देना होगा. चिकित्सकीय चूक की घटनाओं को तंग नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि इन्हें अवसरों के रूप में देखा जाए जिनका उपयोग आम जनता की नजर से ओझल लेकिन चिकित्सकीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पसरीं विसंगतियों को दूर करने में किया जा सकता है. सेवाओं के लिए वाजिब से ज्यादा फीस लिया जाना, रोगियों को अस्पताल के बजाय बाहर से दवाएं खरीदने के लिए विवश किया जाना और नैदानिक और रैफर करने के गलत तौर-तरीकों का इस्तेमाल किया जाना आदि ऐसे मुद्दे हैं, जिन्हें सिलसिलेवार हल किया जाना चाहिए.
भारत में अस्सी प्रतिशत स्वास्थ्य सेवाएं निजी क्षेत्र मुहैया कराता है. इस क्षेत्र पर बहुत ज्यादा नियमन लागू किया गया तो गरीबों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच कम हो जाएगी. न केवल इतना बल्कि उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं महंगी भी हो जाएंगी. ऐसा कुछ भी होता है, वह वांछनीय नहीं होगा. भारत में स्वास्थ्य राज्यों का विषय है, और इसकी प्राय: राज्य सरकारों द्वारा अनदेखी होती है. इस क्षेत्र में विश्वास बहाली के लिए जरूरी है कि सरकार निजी तथा अन्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल के लिए ज्यादा पैसा मुहैया कराए. सरकार के स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा पुख्ता होने से लोगों को मनमाफिक स्वास्थ्य सेवाएं लेने में सहायता मिलेगी. उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं लेने में बर्बाद होने का खतरा भी नहीं रहेगा. चिकित्सकीय चूक की हालिया घटनाओं पर सबका ध्यान गया लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों इसके लिए प्रयास सीमित ही रहे. ऐसे में समझ नहीं आ रहा कि भारतीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में सुधार के लिए किस तरह से आगे बढ़ा जाए? क्या किया जाए कि इस क्षेत्र का कायाकल्प हो जाए? लोगों का स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र से जो विश्वास उठा है, उसे फिर से बहाल करना भारतीय स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. आधे-अधूरे प्रयासों से बात नहीं बनेगी. एक तो यह हो सकता है कि केंद्र तथा राज्य सरकारें स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए निवेश का एक खाका तैयार करें ताकि निजी और सार्वजनिक, दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाया जा सके. ध्यान रहे कि निष्क्रियता भारी पड़ेगी.
(लेख में व्यक्त विचार निजी हैं)
| Tweet |