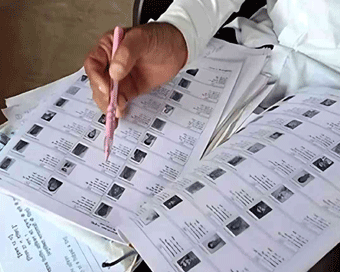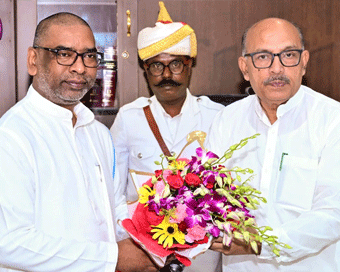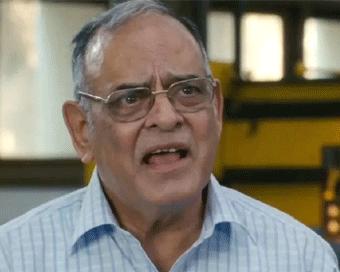मुद्दा : पूर्वाग्रहों से मुक्ति कब?
ब्रिटिश विज्ञान लेखिका एजेंला सैनी अपनी चर्चित किताब ‘इंफिरियर:हाउ साइंस गॉट वूमेन राँग’ अर्थात विज्ञान ने किस तरह महिलाओं के साथ अन्याय किया; अमेरिका के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय येल में हुए एक दिलचस्प अध्ययन का जिक्र करती है.
 मुद्दा : पूर्वाग्रहों से मुक्ति कब? |
.jpg) वैज्ञानिकों के स्तर पर भी किस तरह जेण्डर के मसले पर पूर्वाग्रह काम करते हैं या नहीं करते हैं, इसकी परीक्षा लेने के लिए 100 वैज्ञानिकों के पास लेबोरेटरी मैनेजर की पोस्ट के लिए/काल्पनिक/आवेदन भेजे गए. इन सभी आवेदन योग्यता के मामले में एक जैसे ही थे, मगर उसमें एक चालाकी यह की गई थी कि आधे आवेदन पुरुषों के नाम थे तो बाकी आधे स्त्रियों के नाम थे. गौरतलब था कि अधिकतर ने, जिनमें महिला वैज्ञानिक भी शामिल थीं, उन्हीं आवेदनों को चुना जिनमें पुरुषों का नाम लिखा गया था.
वैज्ञानिकों के स्तर पर भी किस तरह जेण्डर के मसले पर पूर्वाग्रह काम करते हैं या नहीं करते हैं, इसकी परीक्षा लेने के लिए 100 वैज्ञानिकों के पास लेबोरेटरी मैनेजर की पोस्ट के लिए/काल्पनिक/आवेदन भेजे गए. इन सभी आवेदन योग्यता के मामले में एक जैसे ही थे, मगर उसमें एक चालाकी यह की गई थी कि आधे आवेदन पुरुषों के नाम थे तो बाकी आधे स्त्रियों के नाम थे. गौरतलब था कि अधिकतर ने, जिनमें महिला वैज्ञानिक भी शामिल थीं, उन्हीं आवेदनों को चुना जिनमें पुरुषों का नाम लिखा गया था.
विज्ञान के क्षेत्र में भी गहरे रूप में व्याप्त पूर्वाग्रहों के इस अध्ययन ने बरबस एक दूसरे अध्ययन की याद ताजा की, जिसे भारत की अग्रणी कंपनियों में जाति संबंधी संवेदनाओं की पड़ताल करने के लिए अमेरिका के ही दूसरे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय-प्रिन्स्टन यूनिवर्सिटी ने-भारत की ‘इण्डियन इंस्ट्टियूट आफ दलित स्टडीज’ के साथ मिल कर अंजाम दिया था. अमेरिका में अेतों एवं अन्य अल्पसंख्यक तबकों के साथ होने वाले भेदभाव को नापने के लिए बनाई गई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए प्रस्तुत अध्ययन में लगभग पांच हजार आवेदनपत्र भारत की अग्रणी कंपनियों को 548 विभिन्न पदों के लिए भेजे गए.
योग्यताएं एक होने के बावजूद इसके तहत कुछ आवेदनपत्रों के आवेदकों के नाम से यह स्पष्ट हो रहा था कि वह दलित समुदायों से संबंधित हैं. गौरतलब था कि कंपनी की तरफ से ज्यादातर उन्हीं प्रत्याशियों के मामलों में वापस संपर्क किया गया, जिनके नाम उच्चवर्णीय तबके से आते प्रतीत होते थे. दलित सदृश्य नामों वाले प्रत्याशी नौकरी की पहली ही सीढ़ी पर छांट दिए गए थे. इसे विडम्बना ही कहा जाएगा कि सामाजिक तौर पर उत्पीड़ित/वंचित रहे तबकों को अपने यहां तैनात करने के लिए आरक्षण जैसी किसी प्रणाली को लागू करने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज करते हुए मेरिट की वरीयता की बात करने वाले कॉपरेरेट क्षेत्र को बेपर्द करने वाले प्रस्तुत अध्ययन के निष्कषरे पर कभी चर्चा नहीं हुई. बात आई-गई हो गई.
अगर दुनिया के दो बड़े जनतंत्रों में शिक्षा संस्थानों में एवं रोजगार प्रदान करने वाले प्रतिष्ठानों में-जाति एवं जेण्डर जैसे मसलों पर पूर्वाग्रहों की ऐसी स्थिति इक्कीसवीं सदी में भी मौजूद हैं तो अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि इनसे पार पाने के लिए कितना वक्त लगेगा? अगर भारत की बात करें तो यह पूछा जाना समीचीन होगा कि क्या जातिगत पूर्वाग्रहों का बोलबाला इस वजह से बना है कि कापरेरेट क्षेत्र में निर्णयकारी पदों पर सामाजिक विविधता की गहरी कमी है. कड़वी सच्चाई यही है कि भद्र कही जाने वाली जातियों की कापरेरेट बोर्ड में बहुतायत एवं उनमें मौजूद पूर्वाग्रहों के चलते ही वंचित तबकों को उनमें स्थान नहीं मिल पा रहा है. संसदीय समिति की रिपोर्ट और अकादमिक जगत के अध्ययन इसी बात की ताईद करते हैं.
कुछ समय पहले सम्पन्न संसदीय समिति के अध्ययन में एयर इण्डिया में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कम प्रतिनिधित्व को लेकर सरकार की आलोचना की और इस बात की हिमायत की थी कि न केवल उच्च श्रेणी के अधिकारियों के पदों पर अनुसूचित तबकों की नियुक्ति एवं उनके लिए आरक्षण मिलना चाहिए बल्कि सरकार को इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कंपनी के निदेशक बोर्ड में अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य को स्वतंत्र निदेशक के तौर पर स्थान मिलना चाहिए. कमेटी के मुताबिक अनुसूचित तबके के अधिकारियों को भी नेशनल एविएशन कंपनी आफ इण्डिया लिमिटेड के निदेशक मण्डल पर नियुक्त किया जाना चाहिए.
इसे संयोग कहा जा सकता है कि प्रस्तुत रिपोर्ट का जिन दिनों प्रकाशन हुआ, उन्हीं दिनों कनाडा के यूनिवर्सिटी आफ नार्थ कोलम्बिया के विद्वतजनों-डी. अजित, हान दोनकर एवं रवि सक्सेना-की टीम द्वारा भारत के कापरेरेट बोडरे की समाजशास्त्रीय विवेचना सामने आई. अपने अध्ययन में उन्होंने भारत की अग्रणी एक हजार कंपनियों के कापरेरेट बोर्ड का अध्ययन किया, जिनका देश के अग्रणी स्टॉक एक्स्चेंज में दर्ज सभी कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन अर्थात बाजार पूंजीकरण में हिस्सा 4/5 था. बोर्ड की सामाजिक संरचना जानने के लिए उन्होंने ब्लाउ सूचकांक का प्रयोग किया, जिसके मुताबिक कापरेरेट बोर्ड में विविधता बिल्कुल नहीं है और भारत के ये कापरेरेट बोर्ड आज भी ओल्ड बॉयज क्लब बने हुए हैं.
| Tweet |