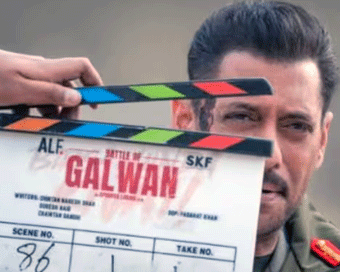गणतंत्र : मुकम्मल कामयाबी से दूर
अपने गणतंत्र के 69 वें वर्ष में प्रवेश करते वक्त हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यही हो सकती है कि क्या वाकई तंत्र और गण के बीच उस तरह का सहज और संवेदनशील रिश्ता बन पाया है जैसा कि एक व्यक्ति का अपने परिवार से होता है?
 गणतंत्र : मुकम्मल कामयाबी से दूर |
.jpg) आखिर आजादी और फिर संविधान के पीछे मूल भावना तो यही थी. महात्मा गांधी ने इस संदर्भ में कहा था- ‘मैं ऐसे संविधान के लिए प्रयत्न करूंगा, जिसमें छोटे-से-छोटे व्यक्ति को भी यह अहसास हो कि यह देश उसका है, इसके निर्माण में उनका योगदान है और उसकी आवाज का यहां महत्त्व है. मैं ऐसे संविधान के लिए प्रयत्न करूंगा, जहां ऊंच-नीच का कोई भेद नहीं होगा, जहां स्त्री-पुरु ष के बीच समानता होगी और इसमें नशे जैसी बुराइयों के लिए कोई जगह नहीं होगी.’ दरअसल, भारतीय गणतंत्र के मूल्यांकन की यही सबसे बड़ी कसौटी हो सकती है.
आखिर आजादी और फिर संविधान के पीछे मूल भावना तो यही थी. महात्मा गांधी ने इस संदर्भ में कहा था- ‘मैं ऐसे संविधान के लिए प्रयत्न करूंगा, जिसमें छोटे-से-छोटे व्यक्ति को भी यह अहसास हो कि यह देश उसका है, इसके निर्माण में उनका योगदान है और उसकी आवाज का यहां महत्त्व है. मैं ऐसे संविधान के लिए प्रयत्न करूंगा, जहां ऊंच-नीच का कोई भेद नहीं होगा, जहां स्त्री-पुरु ष के बीच समानता होगी और इसमें नशे जैसी बुराइयों के लिए कोई जगह नहीं होगी.’ दरअसल, भारतीय गणतंत्र के मूल्यांकन की यही सबसे बड़ी कसौटी हो सकती है.
हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि आजाद भारत का पहला बजट 193 करोड़ का था और हमारा 2017-18 का बजट करीब 21,47,000 करोड़ रु पये का है. यह एक देश के तौर पर हमारी असाधारण उपलब्धि है. इसी प्रकार और भी कई उपलब्धियों की गुलाबी और चमचमाती तस्वीरें हम दिखा सकते हैं. मसलन, 1947 में देश की औसत आयु 32 वर्ष थी, अब यह 68 वर्ष हो गई है. उस समय पैदा लेने वाले 1000 शिशुओं में से 137 तत्काल मर जाते थे. आज केवल 53 मरते हैं. उस समय साक्षरता दर करीब 18 फीसद थी जो आज 68 फीसद से ज्यादा है. ऐसे अनेक क्षेत्र हैं, जिनके आधार पर दुनिया भारतीय गणतंत्र के अभी तक के सफर की सराहना करती है. एक समय दुनिया के जो देश भारत को दीन-हीन मानते थे वे ही इसे भविष्य की महाशक्ति मानकर इसके साथ संबंध बनाने में गर्व महसूस करते हैं.
ये सब फौरी तौर पर तो हमारे गणतंत्र की सफलता का प्रमाण है. लेकिन जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि गणतांत्रिक भारत का हमारा लक्ष्य क्या था तो फिर सतह की इस चमचमाहट के पीछे गहरा अंधेरा नजर आता है. फिर भी यह कहना उचित नहीं होगा कि भारत में गणतंत्र पूरी तरह असफल हो गया. असल समस्या कहीं और है. दरअसल, भारत का गणतंत्र शहरों तक सिमट कर रह गया है और शहरी लोगों के पास कोई राष्ट्रीय परिदृश्य नहीं है. इसीलिए उन्होंने गांवों से नाता तोड़ लिया है. सरकार को किसानों की चिंता हरित क्रांति तक ही थी, ताकि अन्न के मामले में देश आत्मनिर्भर हो जाए. उसके बाद गांवों और किसानों को उनकी किस्मत के हवाले कर दिया गया. यही वजह है कि पिछले एक दशक में दो लाख से भी ज्यादा किसानों के आत्महत्या कर लेने पर भी हमारा गणतंत्र विचलित नहीं हुआ.
इस लिहाज से कह सकते हैं कि हमारा गणतंत्र शहरों में तो अपेक्षाकृत सफल हुआ पर गांवों को विकास की धारा में शामिल करने में पूरी तरह विफल रहा. इस कमी को दूर करने के लिए पंचायती राज शुरू किया गया, मगर ग्रामीण इलाकों में निवेश नहीं बढ़ने से पंचायतें भी गांवों को कितना खुशहाल बना सकती हैं? गांव के लोगों को सामान्य जीवनयापन के लिए भी शहरों का रुख करना पड़ रहा है. गांवों का क्षेत्रफल कितनी तेजी से सिकुड़ रहा है. इसका प्रमाण 2011 की जनगणना है. इसमें पहली बार गांवों की तुलना में शहरों की आबादी बढ़ने की गति अब तक की जनगणनाओं में सबसे ज्यादा है.
शहरों की आबादी 2001 के 27.81 फीसद से बढ़कर 31.16 फीसद हो गई, जबकि गांवों की आबादी 72.19 फीसद से घटकर 68.84 फीसद हो गई. इस प्रकार गांवों की कब्रगाह पर विस्तार ले रहे शहरीकरण की प्रवृत्ति हमारे संविधान की मूल भावना के विपरीत है. हमारा संविधान कहीं भी देहाती आबादी को खत्म करने की बात नहीं करता, पर हमारी आर्थिक नीतियां वही भूमिका निभा रही हैं और इसी से गण और तंत्र के बीच की खाई लगातार गहरी होती जा रही है.
भारतीय गणतंत्र की मुकम्मल कामयाबी की एकमात्र शर्त यही है कि जी-जान से अखिल भारतीयता की कद्र करने वाले तबके की अस्मिता और संवेदनाओं का सम्मान किया जाए. आखिर जो तबका हर तरह से वंचित होने के बाद भी शेषनाग की तरह भारत को टिकाए हुए है, उसकी स्वैच्छिक भागीदारी के बगैर क्या कोई गणतंत्र मजबूत और सफल हो सकता है? जो समाज स्थायी तौर पर विभाजित, निराश और नाराज हो, वह कैसे एक सफल राष्ट्र बन सकता है?
| Tweet |