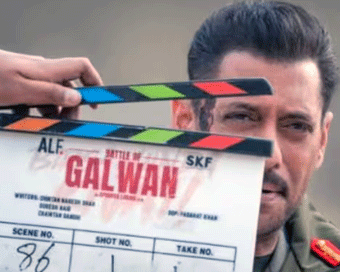राजकोषीय घाटा : कम करना समझदारी नहीं
जब से नरेन्द्र मोदी सरकार ने सत्ता संभाली है, वित्तमंत्री अरुण जेटली लगातर हर बजट में राजकोषीय घाटे को कम रखने के संकल्प का प्रदर्शन किया है.
 राजकोषीय घाटा : कम करना समझदारी नहीं |
.jpg) पिछली यूपीए सरकार के शासन में वैश्विक मंदी का बहाना लेते हुए, सरकार ने अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के नाम पर सरकारी खर्च में जो अनाप-शनाप वृद्धि की, उसके चलते वर्ष 2011-12 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.7 प्रतिशत तक पहुंच गया. वैश्विक मंदी के बहाने जब यूपीए सरकार ने राजकोषीय घाटा बढ़ाया तो जैसे लोक-लुभावन खचरे की बाढ़ सी लग गई. उसका असर यह हुआ कि बड़ी मात्रा में रिजर्व बैंक से ऋण लिया गया और करेंसी की मात्रा बढ़ने से मुद्रास्फीति में भारी वृद्धि हो गई. अर्थव्यवस्था को उससे भारी नुकसान हुआ और जीडीपी ग्रोथ घटने लगी.
पिछली यूपीए सरकार के शासन में वैश्विक मंदी का बहाना लेते हुए, सरकार ने अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के नाम पर सरकारी खर्च में जो अनाप-शनाप वृद्धि की, उसके चलते वर्ष 2011-12 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.7 प्रतिशत तक पहुंच गया. वैश्विक मंदी के बहाने जब यूपीए सरकार ने राजकोषीय घाटा बढ़ाया तो जैसे लोक-लुभावन खचरे की बाढ़ सी लग गई. उसका असर यह हुआ कि बड़ी मात्रा में रिजर्व बैंक से ऋण लिया गया और करेंसी की मात्रा बढ़ने से मुद्रास्फीति में भारी वृद्धि हो गई. अर्थव्यवस्था को उससे भारी नुकसान हुआ और जीडीपी ग्रोथ घटने लगी.
यूपीए शासन के अंतिम वर्ष 2013-14 में जीडीपी ग्रोथ घटकर मात्र 4.5 प्रतिशत ही रह गई. हालांकि यूपीए के वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम ने अंतिम वर्षो में राजकोषीय घाटे को कम करने का प्रयास शुरू किया और 2012-13 में इसे जीडीपी के 4.8 प्रतिशत और 2013-14 में इसे जीडीपी के 4.4 प्रतिशत तक ले आए. अपने अंतिम बजट, जो केवल ‘वोट आन एकाउंट’ था, चिदम्बरम ने राजकोषीय घाटे को कम कर 4.1 प्रतिशत तक लाने का अनुमान दिया. इसे एक चुनौती के रूप में लेते हुए वित्तमंत्री जेटली ने इसी अनुमान का अपने 2014-15 के बजट में समाहित कर लिया. उसके बाद राजकोषीय घाटा को 2016-17 में 3.5 प्रतिशत और 2017-18 के बजट में 3.2 प्रतिशत तक घटा लिया था. लेकिन जैसे संकेत आ रहे हैं, जीडीपी में अपेक्षित वृद्धि न होने और विमुद्रीकरण एवं जीएसटी के कारण 2017-18 बजट के सरकारी राजस्व के लक्ष्य पूरे नहीं हो पाएंगे, इसलिए संभव है कि 2017-18 के राजकोषीय घाटे के 3.2 के लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सकेगा. लेकिन जैसा वित्तमंत्री के पुराने बजट भाषणों से लगता है कि वे 2018-19 वर्ष में भी राजकोषीय घाटे को कम करने और उसे जीडीपी के 3.0 प्रतिशत तक लाने के लिए प्रयास करेंगे.
राजकोषीय घाटा के ज्यादा बढ़ने के नुकसानों से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे महंगाई बढ़ने और जीडीपी ग्रोथ घटने का खतरा होता है. लेकिन उसके बावजूद प्रश्न यह है कि क्या राजकोषीय घाटा कम करना ही बजट निर्माण का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए? क्या घाटे को लक्ष्य रखकर बजट में खचरे को समायोजित किया जाना चाहिए? जानकार लोग जानते हैं कि बजट में 90 प्रतिशत से भी ज्यादा खर्च ऐसा होता है, जिसे कम नहीं किया जा सकता. उदाहरण के लिए, प्रशासनिक खर्च, पुलिस, प्रतिरक्षा आदि. बल्कि महंगाई, पेंशन आदि वेतन बढ़ोत्तरी के चलते इनमें वृद्धि भी करनी पड़ती है. पिछले कजरे पर ब्याज की अदायगी एक अन्य ऐसा खर्च है, जो कम हो ही नहीं सकता. सामाजिक क्षेत्र जैसे-शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, पेयजल, अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक कल्याण आदि ऐसे मद हैं, जहां खर्च को अधिकतम करना ही चाहिए, और इन्हें किसी भी हालम में कम नहीं किया जा सकता. स्थायी खचरे में समायोजन के अभाव में जब बजट घाटा कम रखने का प्रयास होता है, तो उसका पहला शिकार वे खर्च होते हैं जो सबसे जरूरी हैं, जैसे-पूंजी निर्माण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा.
इसलिए हर साल बजट के आकार को बढ़ाकर इन खचरे को बढ़ाना बहुत जरूरी है. मगर पिछले बजटों का अनुभव बताता है कि वित्तमंत्री द्वारा स्वयं पर राजकोषीय घाटे को लक्षित रखने के अंकुश के चलते वर्ष 2014-15 और 2017-18 के बीच बजट का आकार तीन वर्षो में केवल 29 प्रतिशत की बढ़ा. वर्ष 2007-08 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 2.5 प्रतिशत तक घटा भी लिया गया था. लेकिन उसके बाद से यूपीए शासनकाल के दौरान यह घाटा बढ़ता ही रहा और 2011-12 तक 5.7 प्रतिशत पहुंच गया. हालांकि 2012-13 से फिर से एफआरबीएम अधिनियम की सुध ली गई, लेकिन राजकोषीय घाटे को वास्तव में अंकुश में लाने का श्रेय वर्तमान वित्तमंत्री को जाता है, जो उसे 3.2 प्रतिशत तक लाने में कामयाब हुए.
समझा जा सकता है कि राजकोषीय घाटा बढ़ने से सरकार पर खर्च बढ़ता है, जिसके कारण अगले बजटों में ऋण और ब्याज की अदायगी भी बढ़ती है. इससे आने वाले वर्षो में बजट बनाना और मुश्किल होता जाता है, यदि राजकोषीय घाटा ज्यादा हो जाता है तो उसकी भरपाई रिजर्व बैंक से उधार लेकर करनी पड़ती है, जो नोट छापकर उसे पूरा करता है.
इससे मुद्रास्फीति बढ़ने का खतरा होता है. हालांकि बहुत अधिक राजकोषीय घाटा अच्छी नीति नहीं है, लेकिन हमें समझना होगा कि राजकोषीय घाटे में अत्यधिक कमी आ जाने के कारण हमारा पूंजीगत खर्च और शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर खर्च अत्यधिक प्रभावित हो रहा है. गत कई वर्षो से नरेन्द्र मोदी सरकार ने घाटे को कम रखने का हालांकि सराहनीय प्रयास किया है, लेकिन इसके कारण पूंजी निर्माण और शिक्षा व स्वास्थ्य पर खर्च प्रभावित हुआ है. हमें समझना होगा कि सामाजिक सेवाओं पर खर्च हमारे मानव विकास का मूल आधार होता है. जबसे एनडीए सरकार बनी है, निजी निवेश बढ़ ही नहीं पा रहा, जिसका असर यह है कि पूंजी निर्माण की दर घटकर जीडीपी के 30 प्रतिशत से भी नीचे पहुंच रही है. निजी क्षेत्र का कहना है कि निवेश के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ऊंची ब्याज दरों के चलते निजी कंपनियां अपने अधिशेषों पर भारी ब्याज कमा रही हैं. उधर राजकोषीय घाटे को लक्षित करने की कवायद से सरकारी निवेश नहीं हो पा रहा है. इसलिए सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद जीडीपी ग्रोथ नहीं बढ़ पा रही. वर्ष 2017-18 में सरकार के राजस्व में कमी और अगले साल की स्थिति में बहुत सुधार की संभावनाएं नहीं होने के कारण, बजट के संसाधन दबाव में होंगे.
ऐसे में लक्षित घाटे की तरफ बढ़ा जाएगा तो आशंका यह है कि सबसे बड़ा प्रभाव पूंजीगत निवेश पर होगा और दूसरा बड़ा प्रभाव शिक्षा एवं स्वास्थ्य खर्च पर होगा. इसलिए जरूरी शर्त यह है कि वित्तमंत्री लक्षित राजकोषीय घाटे पर आगे बढ़ने के जुनून से बचते हुए राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.5 प्रतिशत तक ले जाएं. इस बाबत दो साल पहले गठित एन.के. सिंह कमेटी ने भी परिस्थितियों के अनुसार लोचशील राजकोषीय लक्ष्यों के लिए सिफारिश की थी.
| Tweet |