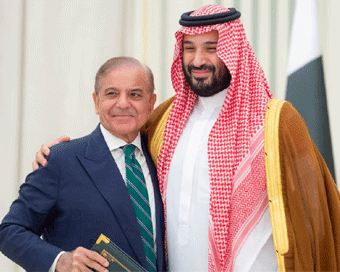सपा-विवाद : चुनाव आयोग की भूमिका
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में यकायक घटे घटनाक्रम ने आने वाले दिनों में होने वाले विधान सभा चुनाव को लेकर चुनाव पंडितों द्वारा की गई भविष्यवाणियों या कहें कि आकलनों को पटरी से उतार दिया है.
 सपा-विवाद : चुनाव आयोग की भूमिका |
हालिया घटनाक्रम में दो गुटों ने एक दूसरे को पार्टी से निकाल दिया है. मेरे पास तमाम जिज्ञासाएं मीडिया के मित्रों की तरफ से आई हैं. इस बाबत कि इन घटनाक्रमों का आने वाले चुनाव पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा. यह भी जिज्ञासा है कि तमाम नाटकीय घटनाक्रमों के बीच निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका हो सकती है. निर्वाचन आयोग मीडिया में प्रकाशित या प्रसारित हो रहीं पार्टीगत आरोप-प्रत्यारोपों की खबरों से किसी भी सूरत में बाबस्ता नहीं है. निर्वाचन आयोग ऐसे मामलों में स्वत: संज्ञान नहीं लेता. अपने स्तर से कोई कार्रवाई नहीं करता. उसकी भूमिका तभी आरंभ होती है, जब कोई एक पक्ष अपने किसी दावे के साथ निर्वाचन आयोग के पास पहुंचता है.
किसी पक्ष के पहुंचने पर ही आयोग न्यायिक तकाजों के अनुरूप कार्यवाही आरंभ करता है. इलेक्शन सिम्बल्स (रिजव्रेशन एंड अलॉटमेंट) ऑर्डर, 1968 की धारा 15 के तहत एक पक्ष के दावे या आपत्ति के मद्देनजर दूसरे पक्ष को नोटिस जारी करता है, ताकि उसका पक्ष भी जाना जा सके. जाहिर है कि दोनों ही पक्ष स्वयं को वास्तविक पक्ष बता रहे होते हैं. दोनों पक्षों द्वारा स्वयं को वास्तविक होने का दावा करने के चलते निर्वाचन आयोग के लिए जरूरी हो जाता है कि दोनों पक्षों के तर्कों को जान लिया जाए. इसलिए निर्वाचन आयोग दोनों पक्षों को तलब करता है. उनसे अपने-अपने दावों के समर्थन में प्रमाण पेश करने को कहता है. इस बाबत दोनों पक्षों को अपने-अपने दावों के समर्थन में शपथपत्र भी पेश करने होते हैं.
यहां इलेक्शन सिम्बल्स (रिजव्रेशन एंड अलॉटमेंट) ऑर्डर, 1968 की धारा 15 पर गौर करना उपयोगी रहेगा. इसके अनुसार : आयोग अपने तई प्राप्त जानकारी से संतुष्ट होने पर कि किसी मान्यताप्राप्त पार्टी में परस्पर विरोधी पक्ष या गुट उस पार्टी का हिस्सा होने का दावा करते हुए परस्पतर विरोधी दावे कर रहे हैं, तो आयोग संबद्ध मामले में तमाम परिस्थितियों और उपलब्ध तथ्यों पर गौर करते हुए और इन गुटों या पक्षों के प्रतिनिधियों या किसी भी उस व्यक्ति, जो इस मामले में अपना पक्ष रखना चाहता हो, का तर्क सुनकर फैसला देता है कि उनमें परस्पर विरोधी गुटों या पक्षों में से कौन सा पक्ष या गुट मान्यताप्राप्त पार्टी का हिस्सा है.
निर्वाचन आयोग का फैसला ऐसे सभी परस्पर विरोधी गुटों या पक्षों पर बाध्यकारी होता है. निर्वाचन आयोग दावों और प्रति दावों की जांच-परख करके तय करेगा कि किसी गुट या पक्ष का पार्टी में बहुमत है. इस मामले में पार्टी के विधायकों, विधान पाषर्द और पदाधिकारियों के मद्देनजर गौर किया जाता है. हमारा अनुभव रहा है कि दोनों तरफ के गुट या पक्ष प्राय: सवाल उठा देते हैं कि दूसरे पक्ष ने अपने समर्थकों की सूची को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है. समर्थन के लिए जाली हस्ताक्षर करा लिए गए हैं. हस्ताक्षरों की सच्चाई जान लेना निर्वाचन आयोग के लिए बेहद पेचीदा कार्य होता है. दोनों पक्षों की सुननी होती है.
इस समूची प्रक्रिया में तीन से पांच महीने लग सकते हैं. तो कहना यह कि आने वाले चुनाव में क्या होना है, उसे मात्र कुछेक दिनों में तय किया जाना है. कोई न कोई अंतरिम व्यवस्था की जानी होगी. चूंकि दोनों पक्ष पार्टी के नाम तथा चुनाव चिह्न पर दावा कर रहे होंगे इसलिए हो सकता है कि आयोग की तरफ से इस बाबत फैसला फ्रीज या लंबित कर लिया जाए. इस बीच, दोनों पक्षों को अस्थायी नाम दिए जा सकते हैं जैसे कि एसपी (अला) तथा एसपी (फ्लां). इसके अलावा, दोनों पक्षों को अस्थायी रूप से चुनावी चिह्न भी आवंटित किया जाएगा. यह कोई नई बात नहीं है. पहले भी तमाम ऐसे मामले आए हैं, जब किसी पार्टी में टूट होने पर दो पक्षों ने स्वयं को वास्तविक पार्टी होने संबंधी दावे किए थे. इस मामले में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदाहरण भुलाया नहीं जा सकता. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1969 में टूट हुई थी.
और यह करके पार्टी के उस विभाजन से दो पार्टियां-कांग्रेस (ओ) तथा कांग्रेस (आई)-उभरीं. तथ्य यह है कि कांग्रेस में 1978 में एक बार फिर से विभाजन हुआ और यह कांग्रेस (इंदिरा) तथा कांग्रेस (तिवारी) में बंट गई. 1980 के दशक में तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक दो हिस्सों में बंटी. एक का नेतृत्व एमजीआर की पत्नी जानकी कर रही थीं, तो दूसरे हिस्से का जे. जयललिता. बात में जनता दल भी इसी तरह से जद(यू) तथा जद (स) में विभाजित हुआ. ज्यादा दिन नहीं हुए जब 2012 के चुनाव से पूर्व हमें उत्तराखंड में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली. उत्तराखंड क्रांति दल में विभाजन हुआ. और निर्वाचन आयोग ने पूर्व में वर्णित तरीके को अपनाते हुए अपना फैसला दिया था.
आयोग दो बातों पर ध्यान देता है. पहली, पार्टी के संविधान तथा दूसरी, पार्टी में बहुमत का दावा करने वाले पक्षों की पार्टीगत ताकत. ऐसे तमाम मामले आखिर में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. सुप्रीम कोर्ट का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण फैसला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मामले में आया. शीर्ष अदालत ने बहुमत का परीक्षण करने संबंधी भारत निर्वाचन आयोग के आदेश की ही तस्दीक की थी. जहां तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का मामला है, तो पार्टी संविधान और तद्नुरूप कार्रवाई महत्त्वपूर्ण तरीका होगा. बहुमत को परखने, इस तरीके की शीर्ष अदालत तस्दीक कर चुकी है, के तरीके को तो तवज्जो दी ही जानी है. चूंकि इन तमाम तरीकों या प्रक्रिया से न्यायिक तकाजे भी जुड़े हैं, इसलिए यकीनन फैसला होने में चार-पांच महीने लग सकते हैं. तब तक दोनों पक्षों या गुटों को उनकी पहचान के लिए अस्थायी व्यवस्था करते हुए कुछ नाम दिए जा सकते हैं. साथ ही, इन दोनों पक्षों या गुटों को अस्थायी चुनाव चिह्न भी आवंटित किया जाएगा. अभी तो कुछ ऐसा ही परिदृश्य उभर रहा है.
| Tweet |