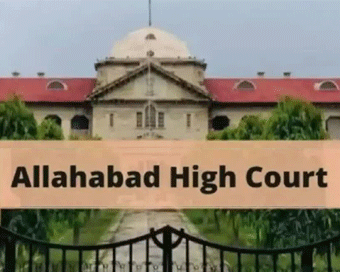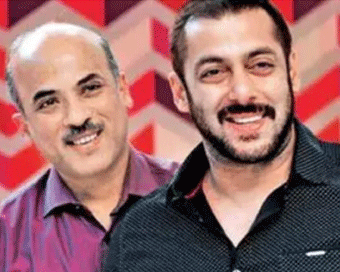चीन से निकटता : नफा-नुकसान कितना!
प्रधानमंत्री मोदी की हालिया चीन यात्रा को दोस्ती की शुरुआत के तौर पर प्रचारित किया गया। लेकिन असली हालात इतने आसान नहीं हैं, जैसे बताए जा रहे हैं। भारत और चीन की नजदीकी असल में अस्थायी रु कावट जैसी है, न कि भरोसेमंद रिश्ते की नई शुरुआत।
 |
कूटनीतिक जानकार इस नई दोस्ती पर फूंक-फूंक कर कदम बढ़ाने की सलाह दे रहे हैं क्योंकि चीन के साथ भारत के आयात-निर्यात में भारी असमानता है। इसलिए जल्दबाजी में जोखिम की अधिक आशंकाएं जताई जा रही हैं।
नि:संदेह प्रधानमंत्री की यात्रा से चीन के साथ रिश्तों की बर्फ पिघली है। दोनों देशों के बीच इस निकटता से कुछ क्षेत्रों में सहयोग के संकेत जरूर मिले। चीन ने कहा कि वह इलेक्ट्रॉनिक्स और गाड़ियों के क्षेत्र में भारत के साथ नये सिरे से काम करेगा। सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने, वीजा नियम आसान करने और कुछ निर्यात पाबंदियां हटाने का वादा किया। अमेरिका के भारी टैक्सों के दबाव में फंसे भारत के लिए ये कदम थोड़ी राहत लेकर आए।
मोदी और शी जिनपिंग ने कहा कि भारत और चीन ‘साझेदार हैं, दुश्मन नहीं।’ इससे दोस्ती का माहौल बना, लेकिन असली समस्या वहीं की वहीं खड़ी दिखती है। चीन लगातार पाकिस्तान का समर्थन करता है। पाकिस्तान में अरबों डॉलर लगाता है, सैन्य और परमाणु मदद देता है और उसकी ढाल बनता है। इससे भारत के लिए दो तरफ से सुरक्षा का खतरा हमेशा बना रहता है, जिसे कोई भी मुलाकात नहीं बदल सकती।
चीन की बेल्ट एंड रोड योजना भी भारत के लिए चिंता का कारण है। श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार तक चीन अपने प्रोजेक्ट्स फैला रहा है। ये सिर्फ विकास के काम नहीं हैं, बल्कि एक तरह का घेरा हैं, जिससे भारत का प्रभाव अपने ही पड़ोस में कम हो रहा है। आर्थिक स्थिति भी भारत के अनुकूल नहीं है।
चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 90 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुका है। भारत चीन से बहुत ज्यादा सामान खरीदता है, लेकिन चीन भारत से बहुत कम खरीदता है। इससे भारत चीन पर निर्भर हो जाता है, लेकिन उसे उतना फायदा नहीं मिलता। उड़ानों या वीजा में ढील जैसी चीजें इस बड़े घाटे और अमेरिकी टैक्स से हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर सकतीं।
भारत-चीन-रूस धुरी की चर्चा ज्यादा नाटकीय कथा जैसी लगती है, इस नई जुगलबंदी में दूरगामी और व्यावहारिक कूटनीतिक संतुलन जैसी नहीं बात नहीं लगती। भारत और चीन एशिया में फिर से अपना प्रभाव बढ़ाने के मामले में अतीत से ही प्रतिद्वंद्वी हैं। जाहिर है इनकी बुनियादी दृष्टि परस्पर विरोधी है।
चीन वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, पाकिस्तान को समर्थन देता है और भारत के पड़ोस में प्रभाव बनाना चाहता है। वहीं भारत इसका जवाब अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड जैसे बहुपक्षीय गठबंधनों से देता है। रूस, जो यूक्रेन युद्ध के बाद चीन पर और अधिक निर्भर हो गया है, इस धुरी में और भी असंतुलन पैदा करता है। ऐसी स्थिति में भारत के एक ‘छोटे खिलाड़ी’ की तरह सिमट जाने का खतरा है। इस स्थिति को भारत कभी गवारा नहीं करता।
देश के भीतर कई विदेश मामलों के जानकार मानते हैं कि भारत ने यह जो नया रास्ता पकड़ा है, वह वास्तव में गुटनिरपेक्ष और मुद्दा-आधारित परंपरा से भटकाव है। यह विरोधाभास प्रधानमंत्री की हालिया चीन यात्रा में साफ दिखाई दिया। सात साल बाद मोदी की चीन यात्रा एक अहम पड़ाव रही। मोदी और शी ने सहमति जताई कि मतभेदों को विवादों में नहीं बदलने दिया जाएगा और आपसी भरोसा, सम्मान और संवेदनशीलता भविष्य के रिश्तों की नींव होंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा पर शांति को द्विपक्षीय रिश्तों की ‘बीमा पॉलिसी’ बताया। दोनों पक्षों ने हालिया डिसइंगेजमेंट और स्थिर माहौल को सकारात्मक कदम के रूप में रेखांकित किया। रिश्तों में आई नरमी से जो ठोस कदम उठते दिखे उनमें शामिल रहे: लिपुलेख, शिपकी ला और नाथू ला दरे से सीमा व्यापार का पुन:आरंभ। दोनों नेताओं ने कहा कि उनकी अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक व्यापार में स्थिरता की भूमिका निभाती हैं।
व्यापार असंतुलन दूर करने के लिए रणनीतिक दृष्टि से सहयोग बढ़ाने का वादा किया गया। मोदी ने शी को 2026 में भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा-पार आतंकवाद का मुद्दा उठाया और सहयोग की जरूरत पर जोर दिया। यह भी दोहराया कि भारत-चीन संबंधों को किसी तीसरे देश के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की वकालत की।
विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया तीखी रही। जयराम रमेश ने मोदी पर ‘ड्रैगन के आगे झुकने’ और आतंकवाद पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। अमेरिका में व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने मोदी की आलोचना करते हुए कहा ‘वे दो सबसे बड़े अधिनायकवादी नेताओं’ के साथ निकटता बना रहे हैं।
कई विश्लेषकों ने एससीओ की सैन्य परेड में मोदी की उपस्थिति को कूटनीतिक सफलता नहीं, बल्कि छवि की समस्या माना-जैसे भारत पश्चिमी लोकतांत्रिक खेमे से दूर हो रहा हो। यात्रा में सद्भावना दिखी, लेकिन कोई ठोस बाध्यकारी समझौते नहीं हुए। मोदी, शी और पुतिन की साझा तस्वीरों को कई लोगों ने वास्तविक उपलब्धि की बजाय केवल संदेश देने वाला प्रतीकवाद माना।
एक ओर चीन से एससीओ और व्यापार के जरिए जुड़ना और दूसरी ओर अमेरिका-झुकाव वाले क्वाड और ब्रिक्स में सक्रिय रहना-आलोचकों को असंगत लगता है। चीन के साथ गहरी प्रतिद्वंद्विता भारत की इस रणनीति पर हमेशा सवाल उठाती है। इस चीन यात्रा का स्वागत करने वालों का मानना है कि मोदी की चीन यात्रा ने एक बार फिर दिखा दिया कि भारत अपने पड़ोसी के साथ संबंधों में शांति और स्थिरता चाहता है, खासकर सीमा और व्यापार के मोर्चे पर।
यात्रा से कुछ व्यावहारिक लाभ मिले लेकिन ठोस समझौतों की कमी और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय आलोचना ने कूटनीतिक सफलता को सीमित कर दिया। असली सवाल है कि क्या भारत इस बहुस्तरीय कूटनीति को ठोस रणनीति में बदल पाएगा या यह अमेरिकी टैरिफ दबाव से मुक्त होने की प्रतीकात्मक बयानबाजी और पैंतरेबाजी तक सिमट कर रह जाएगी!
(लेख में व्यक्त विचार निजी हैं)
| Tweet |