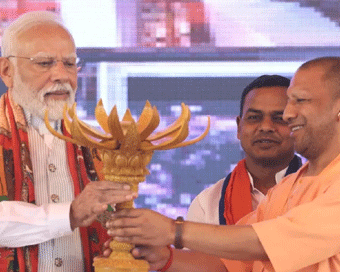मुद्दा : समय पर न्याय मिलना जरूरी
भारत की न्यायिक व्यवस्था अब बदलाव की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा चुकी है। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अब महीने में दो अतिरिक्त कार्य दिवस जोड़ने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
 मुद्दा : समय पर न्याय मिलना जरूरी |
यानी अब दूसरे और चौथे शनिवार को भी सुप्रीम कोर्ट खुलेगा और नियमित मामलों की सुनवाई करेगा। यह फैसला केवल अदालत के काम के घंटे बढ़ाने का मामला नहीं है, बल्कि एक ऐसे समय में आया है जब देशभर में न्याय का बोझ बहुत बढ़ गया है। देश में वर्तमान समय में करीब 5 करोड़ मुकदमे अदालतों में लंबित हैं। इनमें से अकेले सुप्रीम कोर्ट में 72,000 से अधिक मामले पेंडिंग हैं।
हाईकोर्ट में यह संख्या लगभग 60 लाख के करीब है और सबसे ज्यादा भार तो निचली अदालतों पर है, जहां 4 करोड़ 30 लाख से अधिक मुकदमे वर्षो से फैसले की राह देख रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की यह पहल एक संकेत है कि न्यायपालिका अब खुद भी अपनी कार्य संस्कृति को बदलने को तैयार है और यह बदलाव केवल अदालतों के भीतर नहीं, बल्कि पूरे समाज में फैलना चाहिए, लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है कि क्या अदालतों के कार्य दिवस बढ़ा देने भर से समस्या हल हो जाएगी? जवाब है नहीं।
जब तक समाज, सरकार, मीडिया, पुलिस, प्रशासन और आम नागरिक सभी अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, तब तक अदालतों पर बढ़ता बोझ कम नहीं होगा। आज जरूरत इस बात की है कि आम आदमी खुद यह सोचे कि क्या हर विवाद अदालत तक ले जाना जरूरी है? अक्सर मामूली झगड़े जैसे कि जमीन के छोटे विवाद, पारिवारिक तनाव, लेन-देन की छोटी बातें भी कोर्ट तक पहुंचा दिए जाते हैं, जिन्हें बातचीत, पंचायत, मीडिएशन या लोक अदालत के जरिये सुलझाया जा सकता है।
आम जनता को समझना होगा कि हर मामला न्यायालय में ले जाना ही समाधान नहीं, कई बार यह समस्या को और उलझा देता है। वकीलों की भूमिका भी कम अहम नहीं है। वे मुकदमे की दिशा तय करते हैं, मुकदमा लड़ा जाए या सुलझाया जाए। अगर वे केवल जीत-हार की सोच से ऊपर उठकर न्याय दिलाने की भावना से काम करें, तो लाखों मामले अदालत तक पहुंचने से पहले ही सुलझ सकते हैं। साथ ही, यह भी जरूरी है कि वकील फर्जी या दुर्भावनापूर्ण मामलों को दर्ज करने से परहेज करें और मुवक्किल को वास्तविक कानूनी रास्ता दिखाएं। इसी तरह पुलिस और जांच एजेंसियों की भी सीधी भूमिका है। जब समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं होती, जब जांच अधूरी रहती है, जब गवाहों की सुरक्षा नहीं होती, तब मामला खिंचता चला जाता है। न्याय प्रक्रिया तभी प्रभावी हो सकती है जब जांच समयबद्ध, निष्पक्ष और तकनीकी रूप से मजबूत हो। कई मामलों में पुलिस की लापरवाही ही न्याय में देरी की सबसे बड़ी वजह बनती है। प्रशासनिक अधिकारियों को भी अपनी भूमिका को गंभीरता से लेना होगा।
जब भूमि विवाद, जाति प्रमाण पत्र, किराएदारी या राजस्व से जुड़े मामूली मसले प्रशासन द्वारा समय पर न सुलझाए जाएं, तो जनता के पास अदालत जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। ऐसे में तहसीलदार, एसडीएम और अन्य अधिकारी अपने स्तर पर सक्रिय रहेंगे तो कोर्ट का बहुत सारा भार हल्का किया जा सकता है।
वहीं मीडिया, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है, उसे भी जिम्मेदारी निभानी होगी। अक्सर देखा गया है कि मीडिया कुछ मामलों को इस तरह से उछाल देता है कि वह ‘ट्रायल बाय मीडिया’ बन जाता है। इससे न केवल न्याय की प्रक्रिया प्रभावित होती है, बल्कि जनता का भ्रम भी बढ़ता है। मीडिया का काम है जनता को न्यायिक प्रक्रियाओं की जानकारी देना, कोर्ट के फैसलों को सही संदर्भ में प्रस्तुत करना और जन-जागरूकता फैलाना है।
यदि मीडिया सकारात्मक भूमिका निभाए, तो न्यायपालिका और समाज के बीच की दूरी को पाटने का सबसे सशक्त माध्यम बन सकता है। और अंत में, सरकार और नीति-निर्माताओं की भूमिका इस पूरी तस्वीर में केंद्रीय है। यदि जजों की संख्या पर्याप्त नहीं होगी, यदि अदालतों की इमारतें खस्ताहाल रहेंगी, यदि कोर्ट स्टाफ की ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो कितने भी कार्य दिवस क्यों न बढ़ा दिए जाएं, नतीजे नहीं आएंगे। सरकार को न्यायिक बजट में बढ़ोतरी करनी चाहिए, ई-कोर्ट जैसी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाना चाहिए और न्यायिक नियुक्तियों को प्राथमिकता के साथ निपटाना चाहिए।
| Tweet |