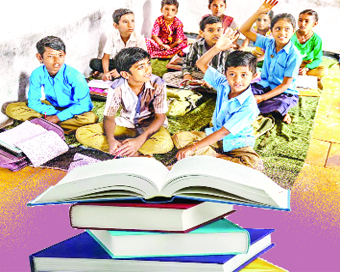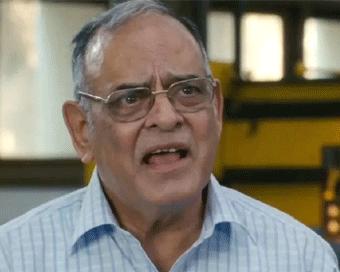मीडिया : बहस का पतन
हिंदी के खबर चैनलों में खबरें कम बहसें अधिक होती हैं। ये तर्कशील की जगह कुतर्की बनाती हैं। इसका कारण हमारी समकालीन राजनीति है।
 मीडिया : बहस का पतन |
जिस मिजाज की राजनीति है वैसे मिजाज की बहसें हैं। अधिकांश बहसें ‘राजनीतिक छीनझपट’ और ‘धींगामुश्ती’ की तरह बन चली हैं। इनमें न नये राजनीतिक ‘विचारों’ का निर्माण होता है, न नये तरह के ‘तर्क-वितर्क’ या ‘वाद-विवाद-संवाद’ की गुंजाइश बचती है। एंकर इन राजनीतिक कुश्तियों के किसी निरीह और कमजोर ‘रेफरी’ की तरह नजर आते हैं। कुश्ती के ‘जोड़ों’ को ‘लड़ाने’ और फिर उन्हें ‘छुड़वाने’ भर का काम करते दिखते हैं।
ऐसी हर बहस कुछ इस तरह से शुरू और खत्म होती है : एंकर के सीटी बजाते ही हर दल का प्रवक्ता अपने पक्ष को पेश करने की अपेक्षा दूसरे पर हमला बोल देता है तो दूसरा भी शुरू हो जाता है। जब कोई एंकर उनको समझाने लगता है कि आप बारी आने पर बोलें तो वे शुरू हो जाते हैं कि अगर ये गलत बोलेगा, मेरे नेता के खिलाफ बोलेगा/बोलेगी तो मैं चुप न रहूंगा/रहूंगी और बोलूंगा/बोलूंगी। यह धमकी होती है। बार-बार मना करने पर भी कोई चुप नहीं होता तो एंकर को कहना पड़ता है कि देखिए, आप एक दूसरे के बीच बोलते रहेंगे तो हमारे दर्शकों तक आपकी बात कैसे पहुंचेगी। इसलिए बीच में न बोलिए। आपको टाइम मिलेगा। जवाब में उसे किसी का ‘एजेंट’ होने का ‘खिताब’ तक दे दिया जाता है। कभी-कभी एंकरों को उनकी सांस्कृतिक-धार्मिक पहचान और आधार पर भी कटु-कटाक्षों का सामना करना पड़ता है कि तुम ये हो वो हो, तुम इस-उसके दलाल हो। इसलिए मुझे रोक रहे हो और उसे इतनी देर तक बोलने दे रहे हो।
हिंदी चैनलों में से कई ने अपने बहस कार्यक्रमों के नाम ‘दंगल’, ‘हुंकार’, ‘हल्ला बोल’ या ‘शंखनाद’ ‘डंके की चोट’ या ‘रणभेरी’ रखे हैं, जिनकी विशेषताएं उनके नामों से ही स्पष्ट हैं। कुछ बरसों में टीवी की बहसों की संरचना ‘वैचारिक’ न रहकर ‘राजनीति की ‘सत्तामूलक’ होकर रह गई है। अब बहसों में दलीय नेता या प्रवक्ता होते हैं, ‘आम नागरिक’ या ‘नागरिक विचारक’ नहीं होते जो ‘आम जनता’ की बात कह सकें। इस बीच, चैनलों ने ‘तुरंता फीडबैक’ के नाम पर अपनी बहसों को सोशल मीडिया की आवारगी से जोड़कर रही-सही ‘विचारपरकता’ को भी विदा कर दिया है। चैनल अक्सर अपने-अपने ‘ऐप्पों’ के जरिए ऐसी लाइव बहसों के समांतर दर्शकों की ‘प्रतिक्रियाओं’ को दिखाते रहते हैं और यहां प्राय: ‘एक्टिविस्टों’ का बोलबाला रहता है, जो उन ‘ऐप्पों’ रिएक्ट करते रहते हैं। यहां जैसी भाषा होती है, एकदम ‘गलीछाप’ होती है। किसी विचार या तर्क-वितर्क की जगह सिर्फ ‘पटेबाजी’ दिखती है। कई लोग प्रतिक्रिया के नाम पर किसी न किसी दल का पक्ष लेने लगते हैं, या जो ‘नापसंद’ है, उसे गालियां देने लगते हैं।
अगर आप ऐसी बहसों को अपने ‘लैपटॉप’ या ‘मोबाइल’ पर देखते हैं, तो आपको ऐसी ‘उपबहसें’ खूब दिखेंगी जो टीवी की बहसों से अधिक आपका ध्यान खींचती रहती हैं। एक प्रकार की ‘समांतर ट्रॉलिंग’ होती हैं। फिर, इन दिनों के अधिकांश प्रवक्ता लोग पहले के ‘स्वायत्त प्रवक्ताओं’ की तरह तैयारी करके नहीं आते। उनको ‘प्रॉम्प्ट’ करने वाले उनके मोबाइल पर कुछ न कुछ लिखकर भेजते रहते हैं, जिसे पढ़कर वे ‘वाक्युद्ध’ में भिड़ते रहते हैं। इन बहसों के बरक्स ‘बीबीसी’ या ‘सीएनएन’ या अल जजीरा’ या ऐसे ही खबर चैनलों को देखें तो वहां अपने-अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट एक दूसरे को चुप करने की जगह एक दूसरे के मत-विमत को सुनते-सहते हैं, और बारी आने पर ही बोलते हैं, और जो बोलते हैं, उसके पीछे कोई न कोई आधार होता है। हम उनसे सहमत हों या न हों लेकिन उनकी बहसें, ‘बहसों’ की तरह होती हैं, जहां एंकर सारी बातचीत को अपने कंट्रोल में रखता है क्योंकि वह स्वयं उस विषय पर पूरी तैयारी करके आता है, और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं, जिनसे बड़े नेता तक डरते हैं।
इनके मुकाबले देखें। हिंदी चैनलों की बहसें ‘नागरिक बहसें’ न होकर ‘डब्ल्यूडब्ल्यूएफ’ की कुश्ती की तरह होती हैं। इसका असर यह हुआ है कि स्कूलों के छात्रों की बहसें भी ऐसी ही सतही व उच्छृंकल सी दिखने लगी हैं। इस प्रक्रिया में विचार और तर्कशक्ति की हानि तो होती ही है, एक दूसरे को सुनने-सहने की संस्कृति भी नष्ट हो रही है, और एक नई असहनशील कुतर्की संस्कृति बन रही है। कहने की जरूरत नहीं कि हिंदी बहसों का यह नया ‘पतनविंदु’ है। क्या खबर चैनलों ने बहसों को इसलिए शुरू किया था?
| Tweet |