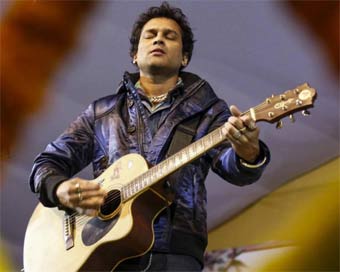लोकतंत्र या ज्ञानतंत्र
लोकतंत्र के बारे में वे सारे शक सही निकले जो उसकी शुरु आत में बहुत-से लोगों के मन में थे. सब से भारी तर्क यह था कि लोकतंत्र में एक विद्वान के वोट का मूल्य एक मूर्ख जितना ही होता है.
 लोकतंत्र या ज्ञानतंत्र |
.jpg) यह एक अलग प्रश्न है कि विद्वानों ने दुनिया का कितना भला किया है और कितना बुरा? मूखरे के बारे में कहा जा सकता है कि उनमें स्वयं को छोड़ कर किसी और का नुकसान करने की क्षमता ही नहीं होती. क्या लोकतंत्र भीड़तंत्र होता है? इसका जवाब हां में देते हुए उर्दू के महान शायर अकबर इलाहाबादी ने कहा था: जम्हूरियत इक तर्जे-हुकूमत है कि जिसमें, बंदों को गिना करते हैं तौला नहीं करते.
यह एक अलग प्रश्न है कि विद्वानों ने दुनिया का कितना भला किया है और कितना बुरा? मूखरे के बारे में कहा जा सकता है कि उनमें स्वयं को छोड़ कर किसी और का नुकसान करने की क्षमता ही नहीं होती. क्या लोकतंत्र भीड़तंत्र होता है? इसका जवाब हां में देते हुए उर्दू के महान शायर अकबर इलाहाबादी ने कहा था: जम्हूरियत इक तर्जे-हुकूमत है कि जिसमें, बंदों को गिना करते हैं तौला नहीं करते.
सरल हिन्दी में, लोकतंत्र वह शासन पद्धति है, जिसमें आदमियों को गिना जाता है, तौला नहीं जाता. यानी यह नहीं देखा जाता कि किसकी बात में कितना वजन है, फैसला यह गिन कर किया जाता है कि कितने हाथ प्रस्ताव के पक्ष में उठे हुए हैं. हाथ दिमाग पर भारी पड़ते हैं. फिर भी लोकतंत्र को व्यापक स्तर पर अपनाया गया तो इसीलिए कि दुनिया की कोई भी अन्य शासन पद्धति इससे बेहतर नहीं है. यह समस्या आज भी बनी हुई है. लोकतंत्र की सीमाएं उजागर हो चुकी है, यह देखा जा चुका है कि लोकतंत्र की सीढ़ियां चढ़ते हुए हिटलर जैसा आदमी भी शासन में आ सकता है, लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर जॉर्ज बुश इराक पर हमला कर सकता है, ट्रंप जैसे कट्टरतावादियों को भी बहुमत से चुना जा सकता है और लोकतंत्र में जनता का मुख्य काम हो जाता है एक भ्रष्ट शासक को दूसरे भ्रष्ट से बदलना. यह अनुभव तीसरी दुनिया का ही नहीं है, पश्चिम में भी लोकतंत्र फेल हो चुका है. वहां भी समाज एक तरफ जा रहा है और शासन दूसरी तरफ. तीसरी दुनिया के लोगों को विकल्प की सब से ज्यादा जरूरत है, पर वहीं विकल्प की चेतना सब से कम है. एक मिसरा कहता है कि ‘मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी सब से कम था’.
यह स्थिति हम तो स्वीकार कर लेते हैं, पर पश्चिम के दिमाग में कोई-न-कोई कीड़ा हमेशा कुलबुलाता रहता है. नई-नई चीजें सोचने में वे आगे हैं. इस मामले में उनका उत्साह देखते ही बनता है. पश्चिमी चिंतकों में कुछ वर्षो से यह बहस चल रही है कि लोकतंत्र को क्यों न ज्ञानतंत्र में बदला जाए? भारत में भी ज्ञान-आधारित समाज बनाने की मुहिम छिड़ी हुई है. माना जा रहा है कि जिसकी पहुंच कंप्यूटर या इंटरनेट तक है, वह ज्ञानी है. ज्ञान और सूचना के संबंध की बात छोड़ दी जाए, तो ज्ञानतंत्र के समर्थकों का कहना यह है कि चूंकि लोकतंत्र कोई सीधी-सरल व्यवस्था नहीं है और सरकार को बहुत ही जटिल स्थितियों में निर्णय लेना पड़ता है, इसलिए आज के लोकतंत्र को मूर्ख और अज्ञानी नहीं चला सकते. वे जितना अधिक सूचना-संपन्न होंगे, उतने ही विवेक से वोट दे सकते हैं और सरकार चुन सकते हैं. वोटर का अज्ञान राजनीतिज्ञ के अहंकार को मजबूती देता है. इसलिए प्रस्ताव यह है कि सभी वोटरों के मत को एक जैसा मान न दिया जाए. जो मतदाता ज्यादा सूचना-संपन्न है, उसकी राय को बीस-पचीस प्रतिशत अधिक मूल्यवान माना जाए. मतदाताओं को सूचना-संपन्न बनाने के लिए अभियान चलाया जाए. समय-समय पर परीक्षाएं आयोजित की जाएं, यह देखने के लिए कि किसकी सूचना-संपन्नता का स्तर क्या है?
राज्य तंत्र पर सब से ज्यादा विचार करने वाले प्लेटो ने दार्शनिक राजा की कल्पना की थी और कहा था कि कोई दार्शनिक ही राजा होने के योग्य है. इस तरह, लोकतंत्र को ज्ञानतंत्र में बदलने वाले उत्साहियों का मानना यह है कि दार्शनिक राजा की कल्पना तभी साकार हो सकती है, जब नागरिक भी दार्शनिक हों. ज्ञानी नागरिक ही ज्ञानी शासकों का चुनाव कर सकते हैं. लोकतंत्र की अस्तित्वगत बुराई यह नहीं है कि शासक भ्रष्ट हैं, बुराई यह है कि मतदाता अक्षम हैं. वे सही प्रतिनिधियों का चुनाव करना नहीं जानते. इसलिए लोकतंत्र को सुधारना है तो सब से पहले नागरिकों में सुधार लाना होगा वे ही लोकतंत्र की नींव हैं. कोई भी विचार किसी एक जगह पैदा नहीं होता. ज्ञानतंत्र की अनुगूंज हमारे यहां भी सुनी जाने लगी है. बल्कि पंचायतों में तो इस पर अमल भी शुरू हो गया है.
पंच-सरपंच से ले कर जिला परिषद के सदस्यतों और पदाधिकारियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित कर दी गई है. कुछ राज्यों में तो यह शर्त भी है कि जो पंचायत का चुनाव लड़ेगा उसके घर में पक्का शौचालय होना चाहिए. कहने की जरूरत नहीं कि यह सांड़ को सींग से नहीं, उसकी पूंछ से पकड़ने की कवायद है. बजाय सभी नागरिकों के लिए शिक्षा और स्वच्छता की सुविधाएं जुटाने की, हम लायक पंचायत अधिकारियों का चुनाव करने में लग गए हैं. यह लोकतंत्र को सिर के बल खड़ा कर देना है; नागरिक राजा को नहीं चुन रहे हैं, राजा नागरिकों को चुन रहे हैं. यह सर्वतंत्र को कुछतंत्र में बदलने की साजिश है, जिसकी ओर न्यायालयों का भी ध्यान नहीं गया है और उन्होंने इस तरह की ऊलजलूल शतरे को न्यायिक वैधता प्रदान कर दी है. लेकिन जो लोग लोकतंत्र को ज्ञानतंत्र में बदलने का उत्साह दिखा रहे हैं, वे षड्यंत्रकारी नहीं हैं. उनकी चिंता लोकतंत्र को पूर्ण बनाने की है. उन्हें कौन बताए कि मनुष्य की तरह लोकतंत्र भी अपूर्ण होने को बाध्य है. लोकतंत्र की खूबसूरती ही इस मान्यता में है कि हर आदमी बराबर है. इस बराबरी को मिटा दिया जाए, तो एक ऐसी विषमता का निर्माण होगा, जो नई-नई विषमताओं की रचना करेगी.
इतनी ही महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सूचना-संपन्न होना ही ज्ञानी होना नहीं है. सट्टा बाजार के खिलाड़ी बहुत अधिक सूचना संपन्न होते हैं. उन्हें अर्थव्यवस्था और राजनीति में होने वाले छोटे-मोटे परिवर्तनों की भी जानकारी होती है. लेकिन वे अपनी इस जानकारी का उपयोग राष्ट्रहित में नहीं करते हैं. यदि हम ज्ञानतंत्र के नाम पर लोकतंत्र को एक विशिष्ट तबके तक सीमित कर देंगे, तो हो सकता है तकनीकी अर्थ में लोकतंत्र बेहतर हाथों में हों, पर बहस और विचार की स्वतंत्रता सीमित हो जाने पर बेहतर कब बदतर में बदल जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता. जिन्हें अपने ज्ञान पर बहुत गर्व है, उनसे यही निवेदन किया जा सकता है कि वे उसे जन-जन तक ले जाएं, इसी में उसकी सार्थकता है. लोकतंत्र भी इसे ही कहते हैं.
| Tweet |