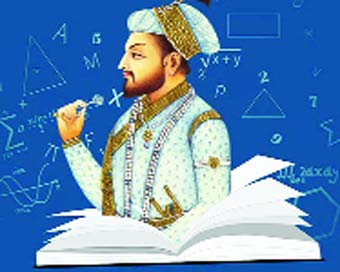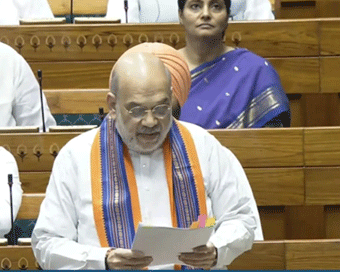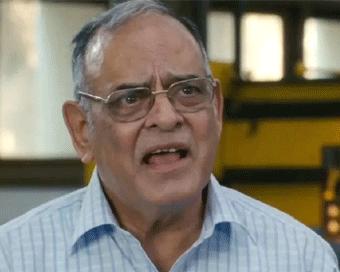परत-दर-परत : बहुजन समाज का साहित्य बोध
यह भ्रम है कि बहुजन समाज को सिर्फ वही साहित्य पढ़ना चाहिए जो खास तौर से उसके लिए लिखा गया है.
 परत-दर-परत : बहुजन समाज का साहित्य बोध |
उदाहरण के लिए हिन्दी क्षेत्र में महात्मा फुले, घासीराम, डॉ. अंबेडकर, पेरियार, नारायण स्वामी, कांशीराम, कंवल भारती, डॉ. धर्मवीर, तुलसीराम, ओमप्रकाश वाल्मीकि आदि का साहित्य बहुजनों को तो पढ़ना ही चाहिए क्योंकि ये वे लोग हैं, जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक परंपरा का मंथन कर ऐसे सूत्र और सिद्धांत निकाले हैं, जो उसके छद्म, दुहरेपन, कहनी-करनी का विरोध, सिद्धांत और व्यवहार के अंतर्विरोध, अन्यायपरस्ती, शोषणपरस्ती आदि का उद्घाटन करते हैं. वैसे प्राचीन साहित्य में भी ऐसे लेखक और कवि रहे हैं, जिनने हिन्दू चित्त में भरे विषों को अपनी रचना का विषय बनाया, जैसे हिन्दी में कबीर, रैदास, दादू, मीरा आदि.
हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में दलित विद्रोह की धारा दलित साहित्य से ही फूटी थी. बेशक, इसकी पृष्ठभूमि में महात्मा फुले और डॉ. अंबेडकर का साहित्य और कर्तृत्व था, लेकिन विचार की अपेक्षा साहित्य समाज में जल्दी फैलता है. लेकिन आज भी दलित और बहुजन साहित्यकार अपने समाज के लिए कम लिखते हैं, उस समाज में सम्मान पाने के लिए ज्यादा लिखते हैं, जिसमें उनके प्रति पूर्वाग्रह अभी भी कम नहीं हुआ है.
शोषण और अन्याय का विरोध मनुष्य के मन में दोनों स्तरों पर फूटता है, विचार के स्तर पर भी और संवेदना के स्तर पर भी. लेकिन विचार के लिए जैसी मानसिक तैयारी या परिपक्वता चाहिए, वह युगों से पढ़ाई-लिखाई और ज्ञान के अन्य सोतों से वंचित रखे जाने के कारण इस वर्ग के कम लोगों में पाई जाती है, यही कारण है कि पूरी दुनिया में साधारण मनुष्य का दुख-सुख तथाकथित मुख्यधारा की बनिस्बत लोक साहित्य में ज्यादा फूटा है. लोक साहित्य वे रचनाएं हैं, जिनके लेखक का नाम है क्योंकि यह वास्तव में लोक साहित्य है, जिसे कई-कई पीढ़ियों के स्त्री-पुरु षों ने लिखा, गाया, मांजा और चमकाया है. भारत के लोक साहित्य में स्त्री की वेदना सशक्त ढंग से व्यक्त हुई है. लेकिन किसानों, धोबियों, सूदखोरी के शिकार परिवारों, नीची मानी वाली जातियों की पीड़ा भी बहुत ही मार्मिंक रूप से मुखरित हुई है. दलित और बहुजन समाज को अपनी पीड़ा से निस्तार पाने की आकुलता होती तो वह अपने दर्द को कलात्मक ढंग से प्रगट करने के विविधरंगी प्रयास करता. इसी में उसकी मुक्ति भी है.
गालिब का मशहूर शेर है, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना. अब हमें अपने दर्द को सिर्फ सहलाना नहीं है, उसे टोपी की तरह सिर पर प्रतिष्ठित करना है, आभूषण की तरह पहनना है. दर्द को कला रूप में सामने रख देने पर उसका परिताप आंखों के रास्ते से बह निकलता है, और समाज को शुद्ध और प्रांजल करता है. इसलिए देश भर में हर महीने सैकड़ों ऐसे कार्यक्रम-गीत, संगीत, नाटक, प्रहसन आदि-होने चाहिए जो हमारे लोक साहित्य में दबी पड़ी व्यथा, पीड़ा, प्रवंचना बोध और अन्याय चेतना को बहुत ही कलात्मक ढंग से पेश करते हों. सिर्फ आरक्षण के लिए लड़ना ही बहुजन का संघर्ष नहीं है. उन परिस्थितियों को उभारना भी इस संघर्ष का हिस्सा है जिनके परिणामस्वरूप आरक्षण जैसी सतह पर अतार्किक जान पड़ने वाली तरकीब उच्चतम किस्म की तार्किकता दिखाई पड़ने लगे. लेकिन हमें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जिसे सवर्ण साहित्य कहते हैं, वह सब का सब कूड़ा नहीं है. हर साहित्य में, अगर वह साहित्य है भड़ैती या पोर्नोग्राफी नहीं है, मूल्यों का कुछ स्पर्श होता ही है, नहीं तो उसमें हृदय को स्पर्श करने की क्षमता नहीं आ सकती.
दूसरी बात यह है कि जिसे हम सवर्ण राजनीति कहते हैं, उसमें भी पूरा का पूरा सवर्णवाद नहीं होता. संवेदना एक जटिल चीज है. वह समाज में प्रचलित विभिन्न धाराओं के सूक्ष्म तत्वों से निर्मिंत होती है. यही कारण है कि बहुजन समाज के एक वर्ग में महात्मा गांधी के प्रति गुस्सा मौजूद होने के बावजूद यह भूलने लायक नहीं है कि अस्पृश्यता के खिलाफ उन्होंने कठिन संघर्ष चलाया था, और इसके चलते कई बार मरते-मरते बचे थे. एक ओर डॉ. अंबेडकर हिन्दू धर्म ग्रंथों में अन्याय और विषमता के सूत्र खोज रहे थे, तब गांधी जी घोषणा कर रहे थे कि जिस शास्त्र में अस्पृश्यता का समर्थन है, उसे मैं शास्त्र नहीं मानता. उस समय के हिन्दू समाज में यह एक युगांतरकारी घोषणा थी.
इसी तरह हमें सवर्ण साहित्य में जहां-जहां सवर्णवादी मूल्यों का विरोध दिखाई देता है. जिस रामचरितमानस में यह कहा गया है कि सूद्र गंवार ढोल पसु चारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, उसी रामचरितमानस में स्त्री के भाग्य का चितण्रकरते हुए एक विवाहित स्त्री कहती है, पराधीन सपनेहुं सुख नाहीं. पराधीनता के इस दुख का विस्तार करते हुए क्या हम इस देश की अधिकांश पराधीन जो अब भी पराधीन हैं, जनता पर लागू नहीं कर सकते? भारत में स्त्रियां पराधीन हैं, तो क्या पुरु ष भी पराधीन नहीं हैं? फिर कला का भी सवाल है. बेशक, संघर्ष से भी कला का विकास होता है, और फुरसत से भी. लेकिन कोई समाज हमेशा संघषर्रत नहीं रहता. फुरसत के समय वह गाता, बजाता और नाचता भी है. इसलिए हमें अपनी अभिव्यक्ति को मांजने के लिए अपने से भिन्न वगरे और समाजों का बेहतर साहित्य भी जरूर पढ़ना चाहिए. जहां उचित लगे, उसमें रस लेना चाहिए, जहां अनुचित लगे, उसका तिरस्कार करना चाहिए और सीखना तो हर रचना से चाहिए. निश्चय ही मानव जाति में द्वंद्व हैं पर क्या मानवता नाम की कोई साझी विरासत नहीं है?
| Tweet |