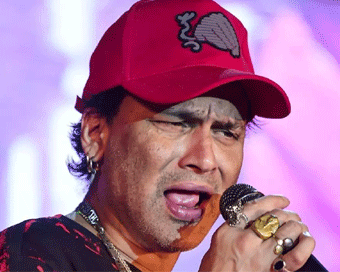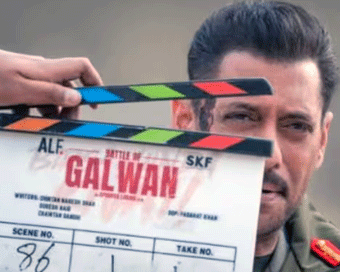गणतंत्र : आत्मावलोकन आवश्यक
भारतीय गणतंत्र के सफर पर यदि हम नजर डालें, तो जल्दी ही समझ में आ जाता है कि हमारा गणतंत्र संविधान निर्माताओं की अपेक्षा के अनुरूप नहीं चल पाया है.
 गणतंत्र : आत्मावलोकन आवश्यक |
.jpg) आज भी गणतंत्र में लोगों की सहभागिता अपूर्ण है, क्योंकि हमारे गणतंत्र को संचालित करने वाले देश के लोगों को नागरिक के रूप में तब्दील करने में असफल ही रहे हैं. देश के नागरिक बनने की जगह हमारे देश में जाति और समूह ही ज्यादा महत्त्वपूर्ण हैं. इसलिए गर्व की बड़ी-बड़ी बातों की घोषणा और समारोह के बीच हमें देश की नाजुक गणतांत्रिक संस्कृति को लेकर आकलन की जरूरत है, जो हमारे गणतंत्र की औपचारिक इमारत को कमजोर कर सकता है और कर भी रहा है. गणतांत्रिक विचार के संदर्भ में मुख्य रूप से चार चुनौतियों की पहचान की जा सकती है.
आज भी गणतंत्र में लोगों की सहभागिता अपूर्ण है, क्योंकि हमारे गणतंत्र को संचालित करने वाले देश के लोगों को नागरिक के रूप में तब्दील करने में असफल ही रहे हैं. देश के नागरिक बनने की जगह हमारे देश में जाति और समूह ही ज्यादा महत्त्वपूर्ण हैं. इसलिए गर्व की बड़ी-बड़ी बातों की घोषणा और समारोह के बीच हमें देश की नाजुक गणतांत्रिक संस्कृति को लेकर आकलन की जरूरत है, जो हमारे गणतंत्र की औपचारिक इमारत को कमजोर कर सकता है और कर भी रहा है. गणतांत्रिक विचार के संदर्भ में मुख्य रूप से चार चुनौतियों की पहचान की जा सकती है.
पहली चुनौती यह दिखाई दे रही है कि समय के साथ हमारा लोकतंत्र विकृत होता जा रहा है. आज बहुसंख्यकवाद, गैरकानूनी और गैरसंवैधानिक पहरु आवाद और सांस्थानिक क्षरण में लगातार वृद्धि हो रही है. सच तो यह है कि हमारा लोकतंत्र आज संख्या बल में तब्दील हो गया है, जहां बातचीत और सौदा-समझौता करने की क्षमता संख्या की चिल्ल-पों में गुम होता जा रहा है. कानून का शासन अपनी किस्मत पर रो रहा है और गैरकानूनी पहरु ओं की संख्या और उनके उत्पात लगातार बढ़ते जा रहे हैं. इससे कानून और संविधान की संस्थाओं का क्षरण हो रहा है. सच कहें, तो आज हमारा गणतंत्र एकांगी सांस्कृतिक वफादारियों का कैदी बनता जा रहा है. दूसरी बड़ी चुनौती स्वयं नागरिकता से संबंधित है.
डॉ. अम्बेडकर ने संविधान सभा के दौरान ही चेताया था कि नागरिकता के स्वरूप के निर्धारण में जाति और समूह हस्तक्षेप करते हैं. पिछले 70 सालों में जाति और समूह के किले और भी अभेद्य बनते गए हैं दलितों और अल्पसंख्यकों के अलावा महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में भी इजाफा ही हुआ है. सामाजिक समरसता पर ग्रहण लग गया है. इसे तीसरी चुनौती के रूप में रेखांकित किया जा सकता है. चौथी चुनौती आर्थिक है. विकास का जो मॉडल हमने आपनाया है, उससे आर्थिक विषमता में जमकर इजाफा हुआ है. 67 करोड़ भारतीयों के धन में कुल इजाफा केवल एक प्रतिशत ही हुआ है, जबकि देश एक प्रतिशत धनियों के तिजोरी में देश का 73 प्रतिशत धन जमा है. कहने की आवश्यकता नहीं कि ऊपर से नीचे की तरफ धन का रिसाव नहीं हो रहा है.
आज के भारत में कोई भी व्यक्ति दूसरे समूह की परंपराओं और व्यवहारों पर टिप्पणी नहीं कर सकता, यदि वह उसी समूह से संबंधित नहीं है. दूसरी तरफ समूह से संबंधित लोग केवल अपने समूह के व्यवहारों, परंपराओं और प्रतीकों का जश्न मना सकते हैं. आज समूह बहस और आलोचना से परे हो चले हैं. उनका वजूद पवित्र है, जहां अजनबी का प्रवेश वर्जित है, जबकि समूह के लोग उस पवित्रता के घेरे में कैद हैं. एक समूह के लोगों का दूसरे समूह के लोगों पर से विश्वास उठ चुका है. यह केवल हिंदू-मुस्लिम संबंधों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जातियां भी इससे मुक्त नहीं है. जातीय आंदोलन के दौरान हमने इसे बार-बार देखा है, महसूस किया है. धार्मिंक अल्पसंख्यक दंगों की विभीषिका से डरे हुए हैं. पूंजीवाद के प्रसार से आदिवासी आक्रांत हैं, उनका दमन किया जा रहा है, जबकि उच्च जातियों द्वारा दलितों के खिलाफ हिंसा और उन्हें अपमानित किया जाना बदस्तूर है. नतीजतन उसके सदस्य अपनी सामूहिक पहचान से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं या अपनी सामूहिक पहचान को नागरिक के रूप में पहचान से जोड़ नहीं पा रहे हैं. जाति और समूह आधारित विलगाव, संदेह और हिंसा ने नागरिक विचार को कल्पनातीत बना कर रख दिया है. सामाजिक न्याय के एजेंडे को आगे नहीं बढ़ाने के चलते जातीय गतिविधि बहुधा अपनी जातीय पहचान स्थापित करने, प्रतीकों का निर्माण करने तथा सांस्कृतिक दुनिया से बनी सीमाओं की रचना को प्रोत्साहित करने में गुम हो जाता है.
ऐसी स्थिति में सर्वजन की बेहतरी से संबंधित किसी विचार का पैदा होना लगभग असंभव ही दिखाई देता है. तीसरी चुनौती सार्वजनिक हित में साझा दृष्टिकोण के अभाव से पैदा होती नजर आ रही है. यानी सार्वजनिक हित खेमों में बंट गया है. ऐसे में यही पता करना मुश्किल हो रहा है कि आखिर सार्वजनिक हित है क्या? आम आदमी के समूहों में विखंडन और आम हित की संभावना की संपूर्ण कमी के चलते सभी राजनीति और नीति निर्धारण प्रतिस्पर्धी आकांक्षाओं को संतुलित करने के एक विक्षिप्त अभ्यास का रूप धारण कर लेते हैं. इस प्रक्रिया का सबसे विद्रूप परिणाम यह है कि आज सार्वजनिक हित के लिए कोई जगह ही नहीं बची है, जो गणतंत्र की मूल अवधारणा है.
और अंत में सबसे चिंतनीय यह कि हमारा गणतंत्र सार्वजनिक विवेक को विकसित करने में अक्षम हो रहा है. विधायिका बहस करने में विफल हो रही है, मीडिया बहस करने की जगह चीखने-चिल्लाने का मंच बन कर रह गया है, पाठ्यक्रम की पुस्तकों में बहस या आलोचनात्मक विषयों को नहीं रखा जा सकता और अकादमिक सेमिनारों पर नजर रखी जा रही है कि उसमें कौन-कौन लोग हिस्सा लेंगे. इसी तरह विरोधी विचार रखने वालों की बैठकों-बहसों पर हमले किए जा रहे हैं और कला, साहित्य और अकादमिक मूल्यों को प्रतिबंधित किया जा रहा है.
स्पष्ट है कि गणतंत्र की स्थापना स्वर्ग में नहीं होती और न वह हमेशा रेडीमेड सामाजिक एकरूपता से विकसित होती है. भारतीय गणतंत्र की रचना वास्तव में एक साहसिक प्रयास था, क्योंकि यहां अनेक तरह की सामाजिक विसंगतियां रही थीं. लेकिन इतनी तो आशा थी ही कि भविष्य के नेता और जनता इस साहसिक प्रयास को कायम रखेंगे. गणतंत्र को मजबूत व समावेशी बनाने में योगदान देंगे. लेकिन हमारे राष्ट्रपति तक ने इन उक्त प्रवृत्तियों पर जुबान नहीं खोली. उनकी नजर में देश में सबसे बड़ी समस्या यह है कि किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाए बिना असहमत होना. जाहिर है कि उनकी चिंता में हमारे गणतंत्र की सफलता का मूलमंत्र यानी समावेशी विकास और समावेशी दृष्टिकोण का कोई खास महत्त्व नहीं है.
| Tweet |