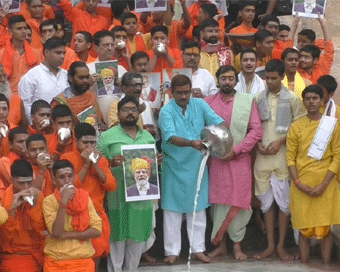प्रसंगवश : मूल्यवान जीवन की ओर
आज आमतौर पर मूल्यहीनता को लेकर समाज के हर वर्ग में चिंता व्यक्त की जा रही है.
 गिरिश्वर मिश्र, लेखक |
मूल्य एक ऐसे प्रेरक तत्व के रूप में समझे जाते हैं, जो हमें विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में प्रवृत्त करते हैं और सामजिक चेतना को जगाए रखते हैं. भिन्न संस्कृतियों में ‘मूल्य’ को अलग-अलग नजरिए से देखा गया है. भारतीय संस्कृति के आधार पर मूल्य को देखने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष ये चार व्यापक मूल्य उभर कर आते हैं. इसमें पहला और केन्द्रीय मूल्य है ‘धर्म’.
धर्म को धारण करने या जीने के साथ जोड़ा गया है. धीरज, क्षमा, चोरी न करना, पवित्रता, अपने ऊपर नियंत्रण, सत्य और क्रोध न करने आदि व्यवहारों को धर्म का लक्षण बताया गया है. ऐसे और भी कई विचार हैं, जिन्हें ले कर धर्म को परिभाषित किया गया है, जैसे ‘अहिंसा परमो धर्म:’ ‘आचार: परमो धर्म:’. एक जगह कहा गया कि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है ‘निह सत्यात परो धर्म:’. ये सभी हमें अच्छे व्यवहार के लिए प्रेरित करते हैं और सभी मतों में परिगणित हैं. यह भी कहा गया है कि जो धारण करने योग्य है, जो करणीय है, वही धर्म है और वही सबसे बड़ा मानव मूल्य है. यह हमें अपने स्व के बारे में ध्यान दिलाता है कि हम खुद के बारे में कैसा सोचते हैं और दूसरों के साथ किस तरह जुड़ते हैं और बर्ताव करते हैं.
आखिर कोई भी आदमी इस दुनिया में निपट अकेला नहीं होता, जीने के क्रम में उसके लिए शेष दुनिया भी काफी महत्त्व रखती है. सच तो यह है कि हम दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, यह इस पर निर्भर करता है कि हम खुद अपने बारे में कैसा सोचते हैं, दूसरों को किस रूप में ग्रहण करते हैं और खुद को दूसरों से किस तरह जोड़ते हैं. हमारे बनने बनाने में दूसरों की खास भूमिका होती है, पर दूसरों को देखने के हमारे नजरिए कई तरह के होते हैं. हम दूसरों को अपनी ही तरह का आदमी सोच सकते हैं या फिर और चीजों की तरह ही एक और उपभोग की वस्तु.
इसीलिए विश्व के प्रमुख विचारक इस अपने आप को या ‘स्व’ को जानने समझने पर जोर देते हैं. पर इसका स्वरूप बेहद व्यापक है. आजकल ‘स्व’ या ‘व्यक्ति’ शब्द प्रयोग में चल निकला है परन्तु भारतीय शब्दावली में ये शब्द नहीं है. इसके स्थान पर ‘आत्म’ शब्द का प्रयोग किया गया है. दूसरे शब्दों में यह दृष्टि एक खास तरह के स्व की बात करती है. इसका पैमाना सीमित स्व के अर्थ में न होकर व्यापक है. इस व्यापक स्व में दूसरे भी शामिल हैं और परिवेशज की चीजे भी शामिल हैं. इसमें मेरा (निज) और पराया (पर) को विभाजित करने वाली जो रेखा है, वह ऐसी छिद्रों वाली (पोरस) होती है, जिसमें से अंदर बाहर आ जा सकना संभव होता है. यह अकेले व्यक्ति के विस्तार या इगो (अहंकार) के अपरिमित संबर्धन से कम सबके विकास और कल्याण से जुड़ा है .
भारतीय सोच में इसीलिए अहंकार को एक समस्या के रूप में देखा गया है और यह माना गया है कि अहंकार एक भ्रम है और अपने अहं को खत्म कर या उसे विसर्जित करते हुए ही समग्र का विकास हो सकता है. इस तरह के समावेशी स्व में दूसरे को भी प्रस्फुटित और विकसित होने के लिए अवसर बना रहता है. व्यक्ति अविभाज्य (इंडिविजुअल) इकाई न होकर कई तत्वों की संघटना होता है. इस तरह का स्व या आत्म का विचार संबंधों पर बल देता है और एक हद तक उन्हीं से परिभाषित होता है और वैधता प्राप्त करता है. आत्मकेंद्रिकता के खिलाफ व्यापक आत्म के विकास के आधुनिक उदाहरण महात्मा गांधी हैं. वे अंदर और बाहर एक रखने के पक्ष में थे. कथनी और करनी में भेद नहीं करते थे. गांधी जी ने 6 अगस्त, 1925 को ‘यंग इंडिया’ में लिखा था ‘ मैं इस पृथ्वी पर स्थित किसी भी मनुष्य से घृणा करने की क्षमता नहीं रखता है. यह गुण मैंने बहुत बड़े साधना के आधार पर प्राप्त किया है. मैंने 40 वर्षो तक किसी से घृणा नहीं की है. मैं जानता हूं कि यह एक बहुत बड़ा दावा है. यह मानवता के गुण के बगैर संभव नहीं है’.
यह समावेशी ‘स्व’ का एक बेहतरीन उदाहरण है. इस स्थिति में एक-दूसरे के बीच की सीमा रेखा टूट जाती है और स्व इतना विस्तृत हो जाता है कि दूसरे भी उसमें समाहित हो जाते हैं, जगत के कल्याण का भाव आता है, समानता का बोध होता है. इस दृष्टि से मूल्य की साधना समष्टि के हित की साधना होगी. वह मूल्य ऐसा नहीं हो सकता, जिसमें मेरा हित हो और दूसरे का अहित हो. इसमें सबके कल्याण की बात होगी. धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना इसी तरह की है. इस सोच में बार-बार इस बात को रेखांकित किया गया है कि धर्म की परिधि में आचरण करो, उससे सबका भला होगा.
Tweet |