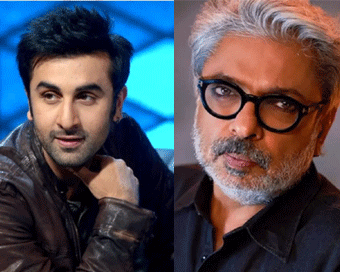गठबंधन राजनीति का अतिवाद
यूपीए सरकार के लिए विपक्ष की तुलना में सहयोगी दल ही मुसीबत बन गये हैं.
 |
पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में लगे झटके से कांग्रेस अभी उबर भी नहीं पायी थी कि बजट सत्र के शुरूआत में ही तृणमूल कांग्रेस ने उसकी मुसीबतें बढ़ा दी हैं. रेल किराया बढ़ाने को लेकर ममता बनर्जी आग बबूला हैं. उन्होंने अपने कोटे के रेल मंत्री को हटाने का फरमान जारी किया है.
उनके इस आचरण से सरकार की फजीहत हुई है. सत्ता के गलियारों में यह चर्चा आम हो चुकी है कि आये दिन तृमूकां की धमकियों से कांग्रेस आजिज आ चुकी है. इसलिए वह नई राजनीतिक संभावनाओं को तलाशने में जुट गयी है ताकि बात-बात में सहयोगी दलों के धमकी भरे तेवरों से बचा जा सके.
पिछले दो दशक से राष्ट्रीय दलों की कमजोरी के कारण केंद्र की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का महत्व काफी बढ़ गया है. तब से केंद्र में एक नयी प्रवृत्ति ‘गठबंधन की राजनीति’ का उभार हुआ है. इसकी शुरुआत का श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी को दिया जा सकता है. राजग के बैनर तले उन्होंने तेईस दलों को एकत्र कर सरकार बनायी थी. उस समय भी ममता, समता और जयललिता (सभी सहयोगी दल) सरकार की परेशानी के सबब थे. अपनी मनमर्जी के मुताबिक सरकार न चलने को लेकर जयललिता ने वाजपेयी की तेरह महीने की सरकार अप्रैल, 1999 में गिरा दी थी.
इसलिए ममता की इस राजनीतिक शैली से किसी को आश्चर्य भी नहीं है. वह वाजपेयी सरकार में भी इसी तरह का संकट पैदा करती रही थीं किंतु वाजपेयी ने कई अवसरों पर उनकी अनसुनी भी की थी. जयललिता की सौदेबाजी में न आकर उन्होंने सरकार गंवाना पसंद किया था, जिसका उन्हें 1999 के मध्यावधि चुनाव में लाभ भी मिला था और जयललिता को चुनाव में बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी.
अब सवाल यह है कि कांग्रेस सहयोगी दलों की इस राजनीतिक सौदेबाजी से कैसे उबरती है? उसे दृढ़ता दिखानी होगी ताकि सरकार की साख पर लगा बट्टा मिट सके. क्योंकि पहले टूजी स्पेक्ट्रम मामले में सहयोगी दल द्रमुक के मंत्रियों की भूमिका को लेकर उसकी छवि पर बट्टा लग चुका है, जिसका दंश वह अभी भी भुगत रही है. रिटेल में एफडीआई, बांग्लादेश के साथ होने वाली तीस्ता जलसंधि तथा राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र पर अड़ंगा लगाने के बाद ममता अब रेल बजट के भाड़ा वृद्धि के प्रस्ताव को पलटने में लग गयी हैं.
बढ़े रेल भाड़े पर आग-बबूला होने वाली ममता बनर्जी की आम बजट पर सकारात्मक टिप्पणी चौंकाने वाली है. यह उनकी पार्टी में चल रही कशमकश की ओर इंगित करती है. दिनेश त्रिवेदी को पहले से पता था कि वह अपनी सुप्रीमो का विश्वास खोते जा रहे हैं, आज नहीं तो कल इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. इसीलिए उन्होंने एक निर्भीक कदम उठाना ज्यादा उचित समझा. ममता को आशंका थी कि त्रिवेदी कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं.
रेल भाड़ा बढ़ने के बाद उनका यह शक यकीन में बदल गया. इसलिए उन्हें त्रिवेदी को हाशिये पर डालने का अच्छा अवसर मिल गया है. उन्होंने अब जिस मुकुल राय को रेलमंत्री बनाने के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, यह वही महानुभाव हैं, जो पिछले वर्ष रेल राज्यमंत्री की हैसियत से असम में ट्रेन दुर्घटना के बाद मौके पर जाने के प्रधानमंत्री के निर्देश को ठुकरा चुके हैं. गठबंधन धर्म की इस मजबूरी को प्रधानमंत्री को तोड़ना होगा.
क्षेत्रीय दलों की स्वभावगत कमजोरी है कि वे अपनी क्षेत्रीय आकांक्षाओं को ही अधिक महत्व देते हैं. उनके राजनीतिक दृष्टिकोण में राष्ट्रीय राजनीति की सोच प्राथमिकता में नहीं होती. इसलिए क्षेत्रीय राजनीति को अपने अनुकूल बनाये रखने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकते हैं.
‘मां, माटी और मानुस’ की दुहाई देने वाली ममता इसलिए भी रेल भाड़ा बढ़ाने पर नाराज हैं कि वह किसी भी कीमत पर भाड़ा बढ़ने की तोहमत अपने माथे पर नहीं चाहती हैं. इसीलिए वह साधारण दज्रे की भाड़ा वृद्धि की वापसी चाहती हैं और अपने मतदाताओं को यह संदेश देना चाहती हैं कि आम आदमी के हित से इतर जाने पर उन्होंने अपने मंत्री तक की कुर्बानी दे दी है.
रूठना, मनाने पर मान जाना और कभी-कभी तो गठबंधन से अलग हो जाना जैसी आदतें क्षेत्रीय दलों के लिए नयी नहीं है. वाजपेयी सरकार में भी जयललिता अपने एक मंत्री पर अचानक नाराज हो उठी थीं और उन्होंने भी ममता की ही तरह उसे हटाने का फरमान जारी किया था, जिसके अनुपालन में उस समय तनिक देर भी नहीं हुई थी.
उस समय यह तर्क दिया गया था कि घटक दलों को अपने कोटे के मंत्री तय करने और हटाने का अधिकार है. इसी राजनीतिक शैली के तहत ही संभवत: ममता ने भी यह कदम उठाया है. वैसे क्षेत्रीय दलों की पूरी राजनीति अपने क्षत्रपों के इर्द-गिर्द घूमती है. क्षत्रप अपने किसी भी नेता की अलग पहचान नहीं बनने देते. जाने-अनजाने में जब भी पार्टी के किसी नेता की अलग पहचान बनने लगती है तो उसके पर कतर दिये जाते हैं. इसलिए क्षत्रप अपने कमजोर नेताओं को ही महत्वपूर्ण पदों पर बिठाना पसंद करते हैं. चंद्रबाबू नायडू इसके उदाहरण रहे हैं.
वह वाजपेयी सरकार में महत्वपूर्ण सहयोगी थे किंतु उन्होंने अपने कोटे से किसी को मंत्री बनने नहीं दिया था. बसपा भी ऐसा ही करती है. उनकी बैठकों और रैलियों में केवल एक ही कुर्सी होती है. ऐसे में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर कांग्रेस को अपने सहयोगी दलों के क्षत्रपों को मनाना होगा. उन्हें विश्वास में लिये बगैर कोई कदम उठाना उल्टा ही पड़ेगा. कांग्रेस को इस राजनीतिक मर्म को अच्छी तरह समझना होगा. तभी वह आये दिन होने वाली फजीहत से बच सकती है.
वैसे राजग सरकार और यूपीए सरकार में एक अहम अंतर है, जिसके कारण कांग्रेस को अपने सहयोगी दलों से ज्यादा परेशानी हो रही है. कांग्रेस के सहयोगी दलों का जिन राज्यों में प्रभाव है, वहां उसकी मजबूत उपस्थिति है. क्षेत्रीय दलों के असाधारण उभार के कारण ही वह कमजोर हुई है. ऐसे में क्षेत्रीय दल अपने क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान में रखकर ही राजनीति करते हैं. वह उससे किसी तरह का समझौता नहीं करते. उनकी राजनीति का सारा ताना-बाना क्षेत्रीय जनाकांक्षाओं के इर्द-गिर्द ही घूमता है.
इसीलिए जहां भी उनका राजनीतिक हित आड़े आ रहा है, टकराव हो रहा है. वह केंद्र की सत्ता में शामिल होकर लाभ तो चाहते हैं पर अपने वोट बैंक पर तनिक आंच आने नहीं देना चाहते. यही संकट का बड़ा कारण है. जबकि राजग सरकार में शामिल ऐसे अधिकतर दल थे, जहां भाजपा थी ही नहीं अथवा जहां थी वहां उसकी राजनीतिक स्थिति काफी कमजोर थी.
यह सच है कि वर्तमान राजनीतिक हालात में कांग्रेस दबाव में है. राज्यों में कमजोर प्रदर्शन के कारण सहयोगी दलों के हौसले बढ़ गये हैं. ऐसे में ममता द्वारा उत्पन्न किया गया यह राजनीतिक संकट अंतिम नहीं है. ममता के बाद सहयोगी दल द्रमुक भी कांग्रेस के लिए मुसीबत बनने वाली है. वह संयुक्त राष्ट्र में श्रीलंका सरकार के खिलाफ तमिलों के प्रति ज्यादती के संबंध में अमेरिका समर्थित प्रस्ताव का सरकार से समर्थन चाहती है.
क्योंकि तमिल उसका मजबूत वोट बैंक हैं. इसलिए सरकार को इस सवाल को बड़ी सतर्कता से हल करना होगा अन्यथा यह बड़ा बन सकता है. इसलिए उसे ऐसी युक्तिपूर्ण राजनीतिक रणनीति बनानी होगी ताकि सरकार की साख पर कम से कम आंच आये. वैसे विस चुनाव से पूर्व कांग्रेस ने रालोद को अपने गठबंधन में शामिल किया है. अब उत्तर प्रदेश में हार के बाद बसपा भी कमजोर पड़ गयी है.
बदले राजनीतिक हालात में उत्तराखंड में वह कांग्रेस को समर्थन दे रही है. केंद्र सरकार को सपा और बसपा दोनों बाहर से समर्थन दे रही हैं. ऐसे में सपा से नजदीकियां और प्रगाढ़ होने के संकेत मिल रहे हैं. देखना है राजनीति किस करवट बैठती है. क्योंकि उत्तर प्रदेश में सपा की बहुमत की सरकार बनने के साथ ही मुलायम सिंह की राजनीतिक हैसियत राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ गयी है. अचानक तीसरे मोच्रे की सुगबुगाहट के बीच वह केंद्रबिंदु बन गये हैं.
इन स्थितियों में कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती ममता की सौदेबाजी को रोकने की है. क्योंकि वह उसके आर्थिक सुधार के कार्यक्रमों को रोकने की राह में बड़ी रोड़ा बन गयी हैं. क्या सरकार बजट के उन निष्कर्ष की अनदेखी करने को तैयार है, जिनमें सब्सिडी कम करने पर बल दिया गया है. गठबंधन की मजबूरियां होती हैं, पर उसकी एक लक्ष्मण रेखा भी होती है. अगर यूपीए के सहयोगी दल उसके पार जा रहे हैं तो नेतृत्वकर्ता दल यानी कांग्रेस को सुनिश्चित करना होगा कि राजधर्म की परंपरा अक्षुण्ण बनी रहे, तभी सहयोगी दलों के अतिवाद से बचा जा सकेगा.
| Tweet |