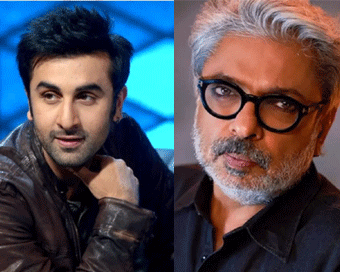अब सबके केंद्र में मुलायम
विधानसभा चुनावों के परिणाम राष्ट्रीय दलों को असहज करने वाले हैं.
 |
उत्तर प्रदेश और पंजाब में सपा और शिरोमणि अकाली दल की ऐतिहासिक सफलता की चकाचौंध में कांग्रेस और भाजपा कांतिहीन हो गई हैं. इन दोनों राज्यों के मतदाताओं ने क्षेत्रीय दलों पर अपना भरोसा जताया है.
इसीलिए इन राज्यों में राष्ट्रीय दल धीरे-धीरे सिमटते जा रहे हैं जिसके दूरगामी राजनीतिक निहितार्थ हैं. उत्तर प्रदेश में सपा की चमत्कारिक जीत और अखिलेश का विधायक दल का नेता चुना जाना भारतीय राजनीति का एक निर्णायक मोड़ कहा जा सकता है. अब केंद्र में गठबंधन के राजनीतिक दौर में क्षेत्रीय दलों का जो स्पेस बचा है, उसे मुलायम सिंह भरने की कोशिश करेंगे और केंद्र में तीसरे मोर्चे की कवायद शुरू हो जाएगी.
तृणमूल कांग्रेस के मध्यावधि चुनाव के बयान को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए लेकिन बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री क्या अपने सहयोगी दलों को नाराज करके कुछ कठोर फैसला ले पाते हैं, इसी बात पर यूपीए के सहयोगी दलों का रुख निर्भर करेगा, जो मध्यावधि चुनाव की अटकलों को तेज या खारिज करेगा.
लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों ने यह तो स्पष्ट कर ही दिया है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस और भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टियों का जनता के बीच आकषर्ण कम हो सकता है. इसलिए गैर-कांग्रेस और गैर-भाजपा दलों के समीकरण की चर्चा अब तेज होगी.
केंद्र में तीसरे मोर्चे की कवायद की संक्षिप्त भूमिका के बाद हमें कांग्रेस और भाजपा के पराभव के कारणों को समझना जरूरी है. कांग्रेस, उप्र में अपने कमजोर संगठन और बड़बोलेपन के कारण इस दुर्गति को पहुंची है.
उसके रणनीतिकारों ने जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर चुनावी रणनीति बनाई और राहुल गांधी को दांव पर लगा दिया. चुनाव से पूर्व टिकट वितरण और प्रचार के दौरान भी पार्टी ने जो हथकंडे अपनाए वह मतदाताओं पर असर छोड़ने में नाकाम रहे. उस समय पार्टी के बड़े नेताओं ने सोशल इंजीनियरिंग के तहत जिताऊ और टिकाऊ लोगों को टिकट देने का तर्क दिया था.
इसलिए दूसरे दलों से आए 216 लोगों को कांग्रेस ने टिकट दिए, जिनमें से नौ ही जीत सके, जबकि 138 पुराने कांग्रेसी उम्मीदवारों में से 19 विजयी रहे. मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के पुत्र और रिश्तेदार भी जीत नहीं सके. इतना ही नहीं, कांग्रेस के 18 फ्रंटल संगठनों को भी चुनाव में नहीं उतारा गया.
यह बताता है कि रणनीतिकारों ने पार्टी को कैसे नुकसान पहुंचाया. दूसरे, महंगाई और भ्रष्टाचार के आरोपों ने उसके ताबूत में एक और कील ठोकने का काम किया. पार्टी का चुनाव अभियान भी कमजोर रणनीति का शिकार हो गया. उत्तर प्रदेश बदलने के नारे के साथ कांग्रेस ने राहुल गांधी को ‘एंग्री एंग मैन’ के रूप में उतारा था लेकिन उनके भाषणों को नौजवानों ने भरोसे लायक नहीं माना.
इसके विपरीत सपा ने अखिलेश यादव को युवा चेहरे के रूप में चुनाव प्रचार की कमान सौंपी जिन्होंने साइकिल चलाकर युवकों, नौजवानों और किसानों से सीधा संवाद बनाया. नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप, बेहतर शिक्षा आदि देने के वादे किए. साथ ही साथ पिछली गलतियां न दोहराने और शालीन प्रचार शैली के जरिये लोगों का भरोसा जीत लिया. यहीं राहुल गांधी चूक गए और अखिलेश उन पर भारी पड़े. सपा मतदाताओं की पहली पसंद बनी.
सवाल यह है कि कमजोर राजनीतिक आधार की जानकारी के बावजूद कांग्रेस के रणनीतिकारों ने राहुल गांधी को दांव पर क्यों लगाया? पूर्व मंत्री मणिशंकर अय्यर और एनसीपी के प्रमुख कृषि मंत्री शरद पवार ने भी राहुल को इस तरह दांव पर न लगाने का सुझाव दिया था पर तब तक काफी देर हो चुकी थी.
क्या चुनाव के रणनीतिकार चुनावी असफलता का ठीकरा राहुल के सिर फोड़कर खुद बचना चाहते थे? सवाल यह भी है कि क्या उधार के प्रत्याशियों की बदौलत पार्टी खड़ी होगी? इस हकीकत को राहुल गांधी को समझना होगा. प्रदेश में जमीन से जुड़े नेताओं को आगे लाना होगा.
ऊपर से नेता थोपने की प्रथा बंद करनी होगी. दिल्ली की दौड़ लगाने वाले नेताओं से तौबा करनी होगी. वैसे कांग्रेस को 2012 में 2007 की तुलना में 5.5 प्रतिशत ज्यादा मत (कुल 14 प्रतिशत) मिले हैं. मतों में इस बढ़ोतरी का श्रेय राहुल गांधी को दिया जा सकता है पर पिछड़े और मुसलमानों को जोड़ने की उनकी कोशिश नाकाम रही. इसीलिए कांग्रेस प्रदेश में चौथे दर्ज की पार्टी बनकर रह गई.
भाजपा, कांग्रेस की छायाप्रति (फोटो कॉपी) हो गई है. चाल-चरित्र-चेहरे की बात करने वाली यह पार्टी ठीक इसके उलट आचरण करने के कारण ही लोगों का विास जीत नहीं पा रही है. 2007 की तुलना में इस चुनाव में उसके मत प्रतिशत में 2 फीसद की गिरावट आई है. ऐन चुनाव के दौरान उमा भारती और संजय जोशी को चुनाव की कमान सौंपे जाने से पार्टी में दिग्भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी.
कुशवाहा के चलते उसकी खूब फजीहत हुई. पिछड़ों को जोड़ने की इस कोशिश में अगड़े भी उससे छिटक गए. साथ ही चुनाव के दौरान यह चर्चा आम हो गई थी कि यदि बसपा को बहुमत नहीं मिला तो वह भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाएगी. इस तरह का संदेश दोनों पार्टियों की ओर से दिया जा रहा था.
आम जनता बसपा के कुशासन से पहले से ही नाराज थी, इसलिए उन्होंने भाजपा को गंभीरता से लिया ही नहीं. अब अयोध्या का मामला ठंडा पड़ गया है. अत: भाजपा के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं था, जो मतदाताओं को बीच उसकी अलग पहचान बनाता और उन्हें एकजुट होने के लिए विवश करता. इन्हीं राजनीतिक अदूरदर्शिता के चलते ये दोनों बड़े दल बौने होते जा रहे हैं और क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है.
कांग्रेस और भाजपा जैसे राष्ट्रीय दलों के विपरीत यदि सपा के चुनावी प्रदर्शन पर नजर डालें तो पाते हैं कि वह बसपा के कुशासन, भ्रष्टाचार और मूर्ति व पाकरे के मोह के खिलाफ पांच वर्षो तक सड़कों पर उतरती रही.
उसकी इस लड़ाकू छवि ने आमजन को ज्यादा आकषिर्त किया. बसपा के खिलाफ उपजे जनाक्रोश के चलते सपा उनकी पहली पसंद बन गई. पार्टी का मजबूत आधार तैयार करने में मुलायम सिंह यादव ने शिल्पी की भूमिका निभाई तो अखिलेश यादव, डीपी यादव को टिकट न देकर यह संदेश देने में सफल रहे कि सपा बदल रही है, जिसे सभी वर्ग के मतदाताओं ने पसंद किया. 2007 की तुलना में उसे 5.5 प्रतिशत अधिक मत मिले हैं.
वर्ष 1984 में गठन के बाद 2007 में बहुमत की सरकार बनाने वाली बसपा मायावती के अहंकार के चलते 2012 में बुरी तरह पराजित हुई है. इसके बावजूद बसपा प्रदेश में एक प्रमुख ताकत के रूप में बनी रहेगी. उसके वोट प्रतिशत में मात्र दो फीसद की गिरावट आई है. इसलिए चाहे राज्य हो या राष्ट्रीय राजनीति, बसपा एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रहेगी.
इसी तरह, पंजाब में अकाली दल-भाजपा ने मतदाताओं के बदलते मिजाज को समय रहते पहचान लिया. अकाली दल ने विकास का मॉडल रखा जबकि कांग्रेस ने ‘डेरों’ के समर्थन पर यकीन किया. कांग्रेस ने अकालियों के कल्याणकारी कार्यक्रमों का भी मजाक उड़ाया. कांग्रेसी नेता यह नहीं समझ सके कि जनता ऐसी सरकार पसंद करती है जो उनकी जरूरतों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो. लिहाजा, कांग्रेस सत्ता से दूर रह गई. उत्तराखंड में कांग्रेस सत्ता बनाने की ओर है लेकिन यहां जिसकी भी सरकार बनेगी, अस्थिरता की तलवार उस पर लटकती रहेगी.
इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये चुनावी परिणाम केंद्र की राजनीति को भी प्रभावित करेंगे. यूपीए सरकार की मुश्किलें बजट सत्र के साथ शुरू हो जाएंगी क्योंकि इन चुनावों में बेहतर प्रदर्शन न कर पाने के चलते उस पर सहयोगी दलों का दबाव बढ़ सकता है. ऐसे में मुलायम सिंह को साथ लेने की उसकी मजबूरी बढ़ जाएगी. राष्ट्रपति चुनाव तथा तीसरे मोर्चे के लिए होने वाले ध्रुवीकरण में भी मुलायम सिंह की अहम भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता.
चुनाव परिणामों के पहले ऐसी उम्मीद थी कि राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका कम होगी, किंतु उप्र व पंजाब के जनादेश ने राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों के महत्त्व को बढ़ा दिया है. ऐसे में राष्ट्रीय राजनीति के क्षितिज पर मुलायम सिंह यादव कद्दावर नेता के रूप में उभरे हैं.
| Tweet |