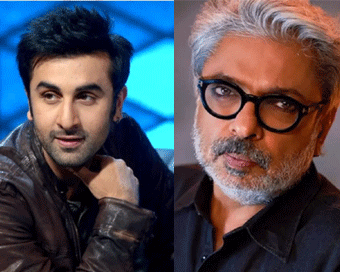कई मिथक तोड़ेगा जनादेश
शनिवार को अंतिम दौर के मतदान के साथ ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की गहमागहमी थम गई.
 |
अब सभी की निगाहें उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों (उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा) के चुनाव परिणामों पर टिक गई हैं. जनादेश होली से एक दिन पहले आ रहा है.
ऐसे में किसकी होली रंगीन और किसकी फीकी मनेगी, इसे लेकर अटकलों के बाजार तेज हो गए हैं. भारी मतदान क्या गुल खिलाएगा, इस बाबत भी राजनीतिक पार्टियां हलकान हैं. सभी इसे अपने-अपने तरीके से परिभाषित कर रहे हैं. यहां 2009 के बाद बढ़े एक करोड़ 40 लाख नए युवा मतदाताओं के वोट काफी निर्णायक माने जा रहे हैं.
इस बढ़े मतदान के प्रतिशत में इनकी अहम भूमिका रही है. अत: हर कोई इस बार अप्रत्याशित जनादेश का कयास लगा रहा है. चूंकि उत्तर प्रदेश अन्य चार चुनावी राज्यों की तुलना में बड़ा है तथा लोकसभा-विधानसभा की सबसे अधिक सीटें यही हैं. अत: इतने बड़े कद के प्रदेश होने के कारण यह देश के भी राजनीतिक समीकरणों को आसानी से प्रभावित कर लेने की क्षमता रखता है. लिहाजा, सत्ता और विपक्ष, सभी को इस खास परिणाम की उत्सुकतापूर्ण प्रतीक्षा है.
उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम इसलिए भी महत्त्वपूर्ण हो गया है कि कांग्रेस के ‘युवराज’ राहुल गांधी ने इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ रखा है. उनकी आक्रामक प्रचार शैली ने कांग्रेस को चुनावी संघर्ष में लाकर मुकाबले को चतुष्कोणीय बना दिया है. इससे पहले दो या तीन पार्टियां-समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बसपा-ही मुख्य मुकाबले में रहा करती थीं. गौरतलब है कि राहुल ने 48 दिन में 211 रैलियां और 18 रोड शो कर लगभग दो दशक पहले जनाधार खो चुकी कांग्रेस को जनता की स्मृति में गहरे बिठाने की पूरी कोशिश की है.
राहुल की तरह समाजवादी पार्टी के युवा प्रदेशाध्यक्ष अखिलेश यादव भी अपने पिता की राजनीतिक विरासत के समक्ष उत्तराधिकारी साबित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं. उन्होंने भी सूबे में घूम-घूम कर 200 रैलियां कर लोगों को आश्वस्त करने की कोशिश की है कि सपा ज्यादा परिमार्जित होकर जनसरोकारों के प्रति और जोर-शोर से प्रतिबद्ध हुई है. अब देखना है कि छह मार्च इन दोनों युवा नेताओं के कैसा राजनीतिक भविष्य तय करता है.
इन दोनों युवा प्रसंगों के अलावा भी कई कसौटियां हैं. चुनाव की जातिवादी राजनीति की भी परीक्षा होनी है, जो दीर्घकालिक विकास पर आम सहमति बनाने के लिए जद्दोजहद करने के बजाए इसे पीछे धकेल देती है. ताजा चुनाव और इसमें भाग ले रहे दल इनके अपवाद नहीं हैं. इस बार पार्टियों ने भी हर विधानसभा क्षेत्र के जातीय गणित को ध्यान में रखकर ही उम्मीदवार उतारे हैं.
कसौटी पर तो मायावती का सर्वजन फामरूला भी है. यह कितना कारगर होता है अथवा उनकी सरकार के कामकाज पर आम जन की नाराजगी चुनाव परिणामों पर भारी पड़ते हैं, यह भी देखा जाना है. युवा मतदाताओं को अपने पक्ष में होने का दावा करने वाली भाजपा के लिए भी यह जनादेश आइना दिखाने का काम करेगा.
चुनाव विश्लेषकों का कहना है कि बहुकोणीय संघर्ष होने पर मतों के अंतर और सीटों के रिश्ते दम तोड़ देते हैं क्योंकि एक प्रतिशत वोट के नफा-नुकसान से लगभग 20 सीटों पर फर्क पड़ जाता है. पिछले आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं. वर्ष 2007 में सपा को 2002 की तुलना में ज्यादा वोट मिले थे किंतु उसकी 46 सीटें घट गई थीं.
इसी तरह, 1989 के चुनाव में जनता दल को 29.7 प्रतिशत मत में ही 208 सीटें मिल गई थीं जबकि 27 फीसद से अधिक मत पाकर भी कांग्रेस कुल 94 सीटों पर सिमट गई थी. इसी तरह, 1991 में साढ़े 31 प्रतिशत मत पाकर भाजपा सत्ता में आ गई थी जबकि 1993 में 33 प्रतिशत से अधिक मत पाकर भी वह सत्ता से दूर हो गई थी. वैसे माना जा रहा है कि जो भी दल 28 प्रतिशत से अधिक मत हासिल करेगा, बहुमत उसी के साथ होगा.
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी जहां चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी नेताओं के बड़बोलेपन से हुए नुकसानों का आकलन कर बिफरी हुई हैं. इससे बेपरवाह सूबे के नेता जीत और सरकार बनाने के रोजाना नए दावे करने से बाज नहीं आ रहे हैं. उन्हें नहीं मालूम कि ऐसा करके वह अपनी फजीहत ही करा रहे हैं.
कांग्रेस के इन नेताओं के दावे के विपरीत तथ्यों के आधार पर सभी मान कर चल रहे हैं कि इस चुनावी महासमर में अन्य किसी भी दल की तुलना में सपा काफी मजबूत स्थिति में है क्योंकि मायावती सरकार से आमजन की नाराजगी का लाभ उसे भरपूर मिल रहा है. दूसरी बात जो उसके पक्ष में जाती है कि उसने पांच सालों तक सक्षम विपक्ष की भूमिका को बखूबी निबाही है. सपा के लिए फायदे की यह स्थिति बसपा के लिए नुकसानदेह बन गई है.
पहली बात तो यह कि एंटी-इंकन्वेंसी बसपा के विरुद्ध मजबूत फैक्टर बना हुआ है. जनता का गुस्सा कम करने के लिए चुनाव के ऐन पहले नाकाबिल और भ्रष्ट विधायकों-मंत्रियों को हटाने या उन्हें टिकट से वंचित करने का उसका दांव उल्टा पड़ा है. मंत्री नसीमुद्दीन को बचाकर मायावती ने जनता की नजरों में अपनी साख और छवि और भी गिरा ली है. उधर, भाजपा अपनों से लड़ रही है. भितरघात उसे दीमक की तरह चाट रहा है. फिर भी उमा भारती और बसपा से निष्कासित बाबू सिंह कुशवाहा को साथ लेकर वह चुनावी करिश्मा होने के सपने देख रही है.
जिन्हें शनिवार देर शाम एनआरएचएम घोटाले में गिरफ्तार कर लिया गया. यद्यपि चुनाव आयोग ने कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल को भले ही क्लीन चिट दे दिया हो किंतु उनके इस कथन को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था ‘उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी. नहीं तो फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा’. बयान के राजनीतिक निहितार्थ एकदम स्पष्ट हैं कि खंडित जनादेश होने की दशा में कांग्रेस ऐसा ही खेल-खेल सकती है, जिसकी वह पुरानी खिलाड़ी रही है.
इतिहास गवाह है कि वर्ष 1996 में भाजपा को सरकार बनाने का अवसर था तो केंद्र के इशारे पर राज्यपाल ने उससे समर्थन देने वालों की बाकायदा सूची मांगी थी. भाजपा सूची नहीं दे पाई तो सूबे में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था. इसी तरह, 2002 में सपा ने सदन में बहुमत साबित करने का दावा किया था. तब विधानसभा को निलम्बित रखा गया था और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू था. उस समय सपा के दावे को राजभवन ने खारिज कर दिया था. यद्यपि बाद में वह सरकार बनाने में सफल हो गई थी.
कांग्रेस का एक वर्ग आज चाहता है कि खंडित जनादेश आने की दशा में दिल्ली से उत्तर प्रदेश का शासन चलाया जाए. ऐसी-ऐसी कल्याणकारी योजनाएं लागू की जाएं ताकि वोटर खुश हो जाएं. फिर उचित अवसर देखकर चुनाव कराए जाएं और मिजाज बदले मतदाताओं के जरिए भरपूर चुनावी लाभ उठाया जा सके. किंतु केंद्र सरकार की जो मौजूदा स्थिति है, उसे देखते हुए उसके लिए इस तरह का कदम उठाना आसान नहीं दिखता.
दूसरे चुनाव प्रचार के दौरान एक केंद्रीय मंत्री के बयान से अन्य दलों के नेताओं को अपने मतदाताओं को गोलबंद करने का बढ़िया मौका दे दिया. उत्तर प्रदेश के जनादेश से यह भी तय होगा कि अल्पसंख्यक किसे अपना रहनुमा मानते हैं. कांग्रेस के मुकाबले में आने से पहले वह समाजवादी पार्टी पर अपना विश्वास रखते आए हैं. अल्पसंख्यक कोटा डबल किए जाने के कांग्रेसी केंद्रीय मंत्रियों के बयान का लाभ पार्टी को कहां तक मिलता है, इस पर भी फैसला हो जाएगा. अंतिम चरण में 10 जिलों की 60 सीटों पर हुए मतदान में मुस्लिम मतदाता निर्णायक हैं.
यहां 25 से लेकर 51 फीसद मतदाता इसी सम्प्रदाय के हैं. पिछले चुनाव में यहां बसपा को 27 और सपा को 17, भाजपा को नौ और कांग्रेस को महज एक सीट मिली थी. इस बार कांग्रेस की सक्रियता से कभी आगे रहे दल चिंतित हो गए हैं. इसके अलावा, उप्र में अन्ना फैक्टर की टेस्टिंग होनी है. अगर बसपा के भ्रष्ट और कुशासन के चलते उसका सूपड़ा साफ हो जाता है तो माना जाएगा कि जनता अब ऐसी सरकार को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है चाहे वह जिस भी नारे या समीकरणों पर सत्ता में आए.
हालांकि विकास के बावजूद यही बात उत्तराखंड, पंजाब और उस छोटे से गोवा में भी लागू है; जहां करोड़पति उम्मीदवार भारी तादाद में हैं. जाहिर है, ऐसे में मतदाताओं का जनादेश कई मिथक तोड़ेगा. वैसे उत्तर प्रदेश को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में सीधी टक्कर है. इसलिए उन राज्यों में स्थिति कमोबेश स्पष्ट है. किंतु बहुकोणीय संघर्ष के चलते उत्तर प्रदेश का चुनावी परिदृश्य धुंधला है. क्या 2012 का चुनाव परिणाम 2007 की तरह ही चमत्कारिक होगा; इसी पर सबकी निगाहें टिकी हैं.
| Tweet |