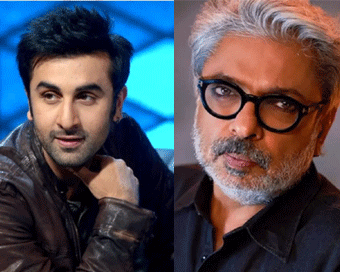खंडित के खिलाफ जातीं कतारें
मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड में मतदान के बाद उत्तर प्रदेश में भी दूसरे चरण का मतदान पूरा हो चुका है.
 |
इन राज्यों की तरह यहां भी अभी तक भारी मतदान हुआ है. वर्ष 2007 में 46 प्रतिशत मतदान की तुलना में पहले चरण के मतदान का प्रतिशत 62 फीसद और दूसरे चरण में 59 फीसद रहा है. सवाल है कि भारी मतदान किसे लाभ पहुंचाएगा? राजनीतिक विश्लेषक इसे बदलाव की बयार की संज्ञा दे रहे हैं. सत्तारूढ़ दल से नाराजगी इस बढ़े मतदान का एक प्रमुख कारण माना जा रहा है.
इस चतुष्कोणीय संघर्ष में बढ़े मतदान प्रतिशत को लेकर हर दल अपने-अपने दावे और तकरे के सहारे भविष्य के राजनीतिक सपने सजाने में लग गया है. ऐसे में नई विधानसभा की तस्वीर को लेकर तरह-तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं. बड़ा सवाल यह है कि क्या 2007 की तरह इस बार भी किसी दल को स्पष्ट बहुमत मिलेगा अथवा खंडित जनादेश होगा?
मोटे तौर पर माना जा रहा है कि दो दौर के मतदान में सत्तारूढ़ बसपा को मतदाताओं की नाराजगी के कारण नुकसान हुआ है. इसका लाभ सपा को मिला है. मुलायम और अखिलेश की सभाओं में जुटी भीड़ को भी पक्ष में वजह बताई जा रही है. कांग्रेस 2009 के लोस चुनाव में अवध और पूर्वाचल में यादगार सफलता हासिल की थी. वह इस बार भी वैसी ही करिश्मा की आस लगाए बैठी है जबकि भाजपा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है. इसलिए किसी के पक्ष में एकतरफा बढ़त की बात करना जल्दबाजी होगी.
वैसे पिछले चुनाव की तुलना में मतदान प्रतिशत में 16 प्रतिशत की वृद्धि को लेकर जिस तरह का राजनीतिक परिदृश्य बनता जा रहा है, वह खंडित जनादेश की ओर ही इशारा कर रहा है. सच है कि यहां बहुसंख्यक आबादी का मतदान धर्म के आधार पर ही नहीं बल्कि जाति, भाषा और क्षेत्रीयता के दबाव में होता है. इस भारी मतदान से यह साफ हो चला है कि आम मतदाता इस मौके को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ज्यादा सक्रिय हुआ है.
ऐसा माना जा रहा है कि बढ़े मतदान में ‘फ्लोटिंग वोट’ का प्रतिशत अधिक है, जिसमें ब्राह्मण, राजपूत जैसी जातियां यादव को छोड़कर दूसरी पिछड़ी जातियां कोइरी, राजभर, निषाद, मल्लाह आदि अति पिछड़ी जातियां और पसमांदा मुसलमान शामिल हैं. इन दोनों दौर में इन जातियों के युवा मतदाताओं की सक्रियता बढ़-चढ़कर थी. उनकी आंखों में बदलाव की ललक दिखी है. ऐसे में अप्रत्याशित परिणाम की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता.
इसलिए मतदाताओं को तंग सवालों में उलझने और किसी राजनीतिक तिलस्म में उलझने की जगह प्रदेश के व्यापक हित को दृष्टिगत रखते हुए मतदान करना चाहिए. उनका मतदान स्पष्ट जनादेश के लिए होना चाहिए. ‘वोट कटवा’ की भूमिका में छोटे दलों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए. साथ ही साथ, अवसर उस दल को ही दिया जाना चाहिए जिसमें सुशासन देने की सामथ्र्य हो. हर वोट बहुमूल्य है. इसलिए उसका परिणामपरक उपयोग होना चाहिए.
वर्ष 1996 और 2002 के चुनावों के परिणाम हमारे सामने हैं. इस बार वैसी चूक नहीं होनी चाहिए. उक्त दोनों चुनावों में ऐसा हो चुका है कि किसी भी दल की सरकार नहीं बन सकी और विधानसभा निलम्बित रखनी पड़ी थी. इसी के बाद, गठजोड़ शुरू हुए थे पर वह कारगर नहीं रहे, जिसका सीधा असर प्रदेश के विकास पर पड़ा और उसका खमियाजा आज भी जनता भुगत रही है. इस दौर में राजनीतिक अस्थिरता के कारण निवेश हुआ ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार बढ़ा. दिलचस्प यह है कि 1995 में मायावती के साथ भाजपा का गठबंधन चार महीने बाद ही टूट गया था.
अगले ही साल यानी 1996 में चुनाव हुए जिसमें किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला. मार्च 1997 में एक बार फिर भाजपा और बसपा साथ-साथ आई थीं. निलम्बित विधानसभा उसी के बाद बहाल हुई थी. बारी-बारी से सत्ता का स्वाद चखने पर सहमति हुई थी. लेकिन छ: माह सत्ता भोगने के बाद जब कल्याण सिंह आए तो दलित एक्ट को लेकर टकराव बढ़ा और मायावती ने आगे समर्थन देने से इनकार कर दिया. ऐसे में भाजपा ने बसपा और कांग्रेस को तोड़कर सरकार बनाई थी. उसी दौर में जगदम्बिका पाल एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने और हटे.
इतना ही नहीं, 2001 में भाजपा ने अजित सिंह से हाथ मिला लिया किंतु अगले साल फरवरी 2002 में विधानसभा चुनाव में भाजपा हार गई तो अपने पुराने जख्मों को भुलाकर एक बार फिर मायावती का साथ दिया. इस बार मायावती अड़ गई कि छह-छह माह के बाद मुख्यमंत्री नहीं बदले जाएंगे. यह गठबंधन मुश्किल से एक साल चल सका. इसी के बाद प्रदेश में सपा की सरकार बनी थी. इन्हीं राजनीतिक झंझावातों को देखते हुए 2007 के चुनाव में जनता ने बसपा को स्पष्ट बहुमत दिया था. यह सच है कि मायावती की बहुमत की सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी. विकास के बजाए घपले, भ्रष्टाचार, मूर्तियां और पार्क बनवाने को लेकर सरकार अपने पूरे कार्यकाल के दौरान सुर्खियों में रही है.
तथ्यों पर आधारित मेरे उक्त विश्लेषण का यह मतलब नहीं होना चाहिए कि स्पष्ट बहुमत वाली कोई भी सरकार वैसी ही निरंकुश हो जाएगी जैसी बसपा सरकार के क्रियाकलापों को देखते हुए उसके बारे में आम धारणा बन गई है. इसका आशय यह है कि परिवर्तन का अधिकार मतदाताओं के ही पास होता है. उनके पास इस ऐतिहासिक अवसर को गंवाने का समय नहीं है.
गठबंधन की राजनीति के बड़े पेच होते हैं. सरकार बनते समय मतदाता के साथ किए गए वादे से कहीं अधिक महत्त्व उन सौदे और समझौतों का हो जाता है, जो बहुमत के अंकगणित की मजबूरी और जरूरी होते हैं. यह नौबत न आने पाए इसीलिए तथा स्थिरता-विकास के लिए खंडित नहीं स्पष्ट जनादेश चाहिए. अभी हाल में आए चुनाव सर्वेक्षणों और नेताओं के बयानों से इस सवाल को बल मिला है. सर्वेक्षणों ने खंडित जनादेश का संकेत दिया है.
कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने किसी भी दल से तालमेल न करने की घोषणा की है तो पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी उनके सुर में सुर मिलाया है जबकि उत्तर प्रदेश के पार्टी के प्रभारी दिग्विजय सिंह ने साफ किया है कि उनका गठबंधन सरकार बनाएगा या राष्ट्रपति शासन लगेगा. उधर, भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी साफ कर चुके हैं कि वह मुलायम और मायावती में से किसी को समर्थन नहीं देंगे. ऐसी स्थिति में अगर दोनों दलों में से किसी ने सपा अथवा बसपा को समर्थन नहीं दिया तो सचमुच ऐसी ही नौबत आ सकती है कि यहां कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना पड़े.
ऐसा हुआ तो फायदा किसको होगा? इसके अलावा एक मजबूत कारण यह भी है कि किसी भी दल के पक्ष में सतह के ऊपर लहर न दिखने का भी है. इसका मतलब है कि कोई एकमुश्त वोट बैंक भी साबुत नहीं बचा है. उनमें बिखराव है. अगर कोई दबी-छुपी लहर है भी तो वह फिलहाल नजर से ओझल है. इन हालात में सवाल यही है कि नतीजे किस करवट बैठेंगे और किसका भाग्योदय होगा.
वैसे मतदान प्रतिशत में बढ़ोत्तरी को लेकर हर दल आशावान हैं और वे अपने जातीय समीकरण को ठीक करने में लगे हैं. कांग्रेस अति दलित और अति पिछड़ों को लेकर काफी मशक्कत कर रही है. बेनी प्रसाद वर्मा और पुनिया को आगे करना उसकी रणनीति का हिस्सा है. उसे लगता है कि मुसलमान और अति दलित-अति पिछड़ा की लामबंदी देखकर ब्राह्मण भी साथ आ जाएंगे.
इसीलिए भारी मतदानों से वह खुश है. सपा अपने पक्ष में अनुकूल माहौल से उत्साहित है. वह बढ़े मतदान प्रतिशत में अपने लिए लहर दिख रही है. वह यादव के अलावा पिछड़ों और मुसलमान के गठजोड़ के सहारे करिश्मा करने की जुगत में है तो बसपा ने कई मंत्रियों और आधे से अधिक विधायकों के टिकट काटकर हर सीट के समीकरण का बारीकी से ध्यान रखा है. उसकी हर कोशिश मतदाताओं की नाराजगी को कम करने की है.
भाजपा बाबू सिंह कुशवाहा को लेकर अति पिछड़ों में घुसपैठ करना चाहती है. अगड़े और बनिया उसके आधार वोट हैं ही. पार्टी नेताओं का दावा है कि बढ़े मतदान का लाभ उन्हें मिल रहा है. फिलहाल, वोटों के इस जोड़-घटाव को अपना दल, पीस पार्टी और कौमी एकता दल सहित अन्य कई छोटे दलों ने और उलझा दिया है. ऐसे में चुनाव के बाद की राजनीति स्थिति को लेकर अटकलबाजी लाजमी है.
| Tweet |