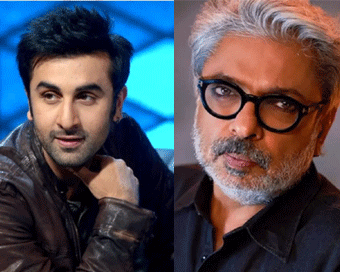बिखरे वोट खिलाएंगे गुल
उत्तर प्रदेश चुनावी रंग में रंग गया है. इस महासमर में चारों बड़े दल अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की जी-तोड़ कोशिश में हैं.
 |
शह-मात का खेल अपने चरम पर है. सत्तारूढ़ बसपा सभी प्रमुख विपक्षी दलों के निशाने पर है. मतदाताओं का विास पाने के लिए हर दल एक दूसरे की कमजोरियों को उजागर करने में लगा है. हर दल की कोशिश अपने को जनता का सबसे हमदर्द साबित करने की है. किंतु मतदाताओं की चुप्पी से प्रदेश की राजनीति अभी अनिश्चितता की तरफ झुकी हुई है क्योंकि तीन बड़े मतदाता समूहों की राजनीतिक वफादारियों के बारे में फिलहाल किसी किस्म का अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं है.
सभी प्रमुख दल (बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा) इन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं किंतु अभी तक किन्हीं को कोई खास सफलता मिलती नहीं दिख रही है. हर कोई सवाल कर रहा है कि ऊंची जातियां किस दल पर मेहरबान होंगी? अति पिछड़े मतदाताओं का बड़ा हिस्सा किसे मिलेगा? मुस्लिम समाज का रुझान इस बार किस पार्टी की चुनावी राह को आसान बनाता है. वोटों के इस जोड़-घटाव के बीच छोटे दल भी इन बड़े दलों के राजनीतिक खेल को बिगाड़ने की कोशिश में हैं. इन अनिश्चितताओं के बीच प्रदेश की राजनीति किस करवट बैठती है, इसी पर सबकी निगाहें टिकी हैं और राजनीतिक विश्लेषक अपने हिसाब से इसके मायने तलाश रहे हैं.
इस बार प्रदेश का चुनावी परिदृश्य बदला हुआ है. वर्ष 2007 के चुनाव में कांग्रेस काफी कमजोर स्थिति में थी और भाजपा अपने अंतर्कलह के चलते पिटी हुई थी. लोगों में मुलायम सिंह सरकार के प्रति गुस्सा था, जिसका सीधा लाभ बसपा को मिला था. किंतु इस बार ऐसा नहीं है. सुश्री मायावती पहली बार अपने पांच साल के काम के आधार पर दुबारा समर्थन पाने के लिए जनता के बीच हैं तो सपा से जनता की पहले जैसी नाराजगी नहीं रही. इस बार कांग्रेस ठोस तैयारी और उत्साह के साथ मैदान में है तो भाजपा अपनी पुरानी राजनीतिक हैसियत पाने के लिए बेताब है. ये दोनों दल इस बार सपा और बसपा के वोट बैंक में ज्यादा से ज्यादा सेंध लगाने की जुगत में हैं. ऐसे में पूरे प्रदेश में चतुष्कोणीय मुकाबले की स्थिति बन गई है तो छोटे दल वोटकटवा की भूमिका में हैं, जो इन बड़े दलों के खेल खराब करने में लगे हैं.
इन सबके बीच प्रदेश की जमीनी राजनीतिक हैसियत समझना जरूरी है. दलित और यादव मतदाताओं की आस्था पहले से तय है. दलित मायावती के साथ हैं तो यादव मतदाताओं की निष्ठा मुलायम सिंह यादव के साथ रही है. किंतु पिछड़ी जातियां जैसे लोधी, कुर्मी, काछी, कुशवाहा आदि अब भी बिखरी हुई हैं. हर दल की निगाहें इन बिखरे वोटों को अपनी झोली में लाने पर टिकी हैं. इतना ही नहीं, अगड़ी जातियों में ब्राह्मण और ठाकुर अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं. 2007 में मायावती को असाधारण बहुमत इनके समर्थन के कारण ही मिला था. वह इस बार मायावती से फिलहाल दूरी बनाए हुए हैं. दूसरे, मुसलमानों की पहली पसंद सपा ही है. 2009 के लोस चुनाव में सपा के बाद कांग्रेस ही उनकी दूसरी पसंद रही है. इसीलिए उसके शानदार प्रदर्शन के पीछे अल्पसंख्यक समर्थन का विशेष हाथ था.
हर दल के अपने मजबूत और कमजोर पहलू हैं. इस महासंग्राम में हर दल अपनी कमजोरी को दूर कर चुनावी वैतरणी पार करने में लग गया है. सत्तारूढ़ बसपा की यह अग्निपरीक्षा है. कांग्रेस और भाजपा की राजनीतिक जमीन उनसे छीनकर उसने अपना मजबूत आधार बनाया था. दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम गठजोड़ की बदौलत ही बसपा ने अपने बलबूते सरकार बनाई थी. उसके इस चुनावी समीकरण के चलते भाजपा और कांग्रेस के जनाधार को बड़ा नुकसान हुआ था. ये दोनों दल अपने खोये इसी राजनीतिक आधार को पाने के लिए बेचैन हैं. ऐसे में मायावती को अपने वोटों के इस गठजोड़ को पकड़कर रखना था. उल्टे वह गैरदलित जातियों को ही नाराज कर बैठी हैं. वह अभी तक इक्कीस मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोपों में बाहर कर चुकी हैं तो बड़ी तादाद में विधायकों के अपने क्षेत्रों में अलोकप्रिय होने के नाम पर टिकट काट चुकी हैं.
मुसलमानों को आरक्षण देने के मामले में जब सभी गैर भाजपा दलों में होड़ मची हुई है तो मायावती ने अपने मंत्रिमंडल से मुसलमान मंत्रियों को भी चलता कर दिया है, जिसका मुस्लिम समुदाय में अच्छा संदेश नहीं गया है. दूसरे दलित, ब्राह्मण और मुसलमान गठबंधन के लिए यह छंटनी पार्टी के लिए कतई हितकारी नहीं है. यह सच है कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी बसपा ऐसा कर जनता को संदेश देना चाहती है कि भ्रष्टाचारियों की उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं है. किंतु जनता सवाल कर रही है कि मंत्रियों का भ्रष्टाचार मायावती को ऐन चुनाव से पहले क्यों दिखा? जब जनता खुलेआम आरोप लगा रही थी तो वह चुप क्यों थीं? इस राजनीतिक चतुराईपूर्ण दांव से वह आम जनता के गुस्से को कम नहीं कर सकतीं. लोगों का मत है कि ऐसा कर मायावती अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकतीं.
इतना ही नहीं उनके द्वारा अगड़ी जातियों के टिकट काटने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि राहुल गांधी के दौरों से कांग्रेस को सीटों का लाभ भले न मिले किंतु ऊंची जातियों के एक बड़े वर्ग का वोट काटने में सफल जरूर होगी. इसलिए बसपा को बड़ी जातियों के वोट बड़े पैमाने पर मिलने की उम्मीद कम है. इसलिए इन पर अपने टिकट व्यर्थ गंवाना उचित नहीं है. उच्च जातियों के समर्थन में मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के ही बीच में है. अब सवाल यह है कि इन राजनीतिक परिस्थितियों के बीच बसपा को सर्वजन की राजनीति का लाभ कैसे मिल पाएगा? यह सवाल उनके रणनीतिकारों को बेचैन कर रहा है. उन्हें पता है कि 2007 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 2009 के लोस चुनाव में लगभग तीन प्रतिशत कम वोट मिलने के कारण ही उसका प्रदर्शन सपा और कांग्रेस के मुकाबले कमजोर रहा है. ऐसे में जातीय गठजोड़ का यह बिखराव उसे डरा रहा है.
इस चुनाव में प्रमुख विपक्षी पार्टी सपा सत्तारूढ़ दल की इन्हीं कमजोरियों का लाभ उठाने में लग गई है क्योंकि सपा और बसपा में मुख्यतौर पर सीधा मुकाबला है. वह अपने ‘माई’ समीकरण को ठीक करने के साथ बसपा की कमजोरियों को उजागर कर अपने पक्ष में माहौल बनाने में लग गई है. डीपी यादव को पार्टी में न लेने के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव के फैसले का भी अच्छा संदेश गया है कि सपा पहले से बदल रही है. इसके अलावा वह अति पिछड़ों के साथ ही साथ व्यापारियों को अपनी ओर खींचने में लग गई है. अभी सांसद नरेश अग्रवाल को अपने साथ लाकर मुलायम सिंह ने अपने इरादे को जता दिया है. सपा अपने इसी चुनावी समीकरण के जरिये माहौल मनाने में लग गई है और काफी उत्साहित है.
लगभग बाइस साल से सत्ता से बाहर रहने वाली कांग्रेस के लिए यह चुनाव खासा अहम है. राहुल गांधी का करिश्माई व्यक्तित्व दांव पर है. प्रदेश की राजनीति में हाशिये पर खड़ी कांग्रेस मुख्यधारा में आने की जद्दोजहद में है. कांग्रेस मानती है कि लोस चुनाव (2009) में मुसलमानों की वापसी के साथ गैर दलित जाटव वोटों के कारण ही उसे सफलता मिली थी. इस बार राष्ट्रीय लोकदल से गठजोड़ कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसने अपनी स्थिति मजबूत की है तो ऊंची जातियों के लिए भाजपा के साथ संघर्ष करती दिख रही है. किंतु कमजोर संगठन उसके लिए परेशानी का सबव बना हुआ है. दूसरे, भाजपा की कोशिश शहरी मध्य वर्ग और अगड़ी जातियों में पहली जैसी पैठ बनाये रखने की है.
बसपा के इनके मोहभंग से भाजपा काफी आशान्वित है. इसके अलावा उसकी नजर अति पिछड़े और गैर यादव पिछड़े वोटों पर है. इसी गठजोड़ की बदौलत उसने नव्वे के दशक में प्रदेश में अपना राजनीतिक रुतबा कायम किया था. किंतु नेतृत्व की गलतियों के कारण यह सामाजिक गठबंधन टूट गया, जिसके कारण वह प्रदेश में इस समय तीसरे नम्बर की हैसियत में आ पहुंची है. अभी बसपा से निकाले गए बाबू सिंह कुशवाहा को पार्टी में शामिल कर उसने चार प्रतिशत कुशवाहा मतों को रिझाने की कोशिश की है, पर उसका यह दांव उसके विपरीत गया है. दूसरे, वह समझ नहीं पा रही है कि पिछड़े वोटों के बीच खोये जनाधार को कैसे वापस लाया जाए? इतना ही नहीं अंतर्विरोध उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है.
कुल मिलाकर जोड़-तोड़ के इस दौर में चुनावी परिदृश्य अभी स्पष्ट नहीं है. दोबारा जनादेश के लिए मायावती उम्मीदवार बदलकर काम चलाना चाहती हैं तो सपा सहित अन्य विपक्षी दल सरकार की असफलताओं व भ्रष्टाचारों को उजागर कर एंटी इन्कन्बन्सी लहर बनाने में लगे हैं. इस दिलचस्प संघर्ष के बीच छोटे दलों को भी अपनी भूमिका नजर आने लगी है. ऐसे में तेरह दलों के गठजोड़ से बना राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई बड़े दलों के उम्मीदवारों की किस्मत छोटी कर सकता है और चुनाव के बाद सरकार बनाने में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता. अब देखना यह है कि नामांकन के बाद क्या चुनावी तस्वीर बनती है?
| Tweet |