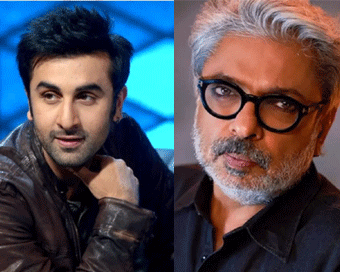कसौटी पर हैं यूपी के मतदाता
उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घमासान तेज हो गया है. हर दल अपने चुनावी अंकगणित को ठीक करने में जुट गया है.
 |
बिहार की तरह उत्तर प्रदेश भी जातीय राजनीति का अखाड़ा बन गया है. वहां जातीय समीकरण के आगे हर मुद्दे दब जाते हैं. पिछले दो दशक के दौरान कभी धार्मिक उन्माद में बहकर तो कभी जातीय गठजोड़ के नये-नये प्रयोगों में फंसकर, यहां के मतदाताओं ने प्रदेश की राजनीतिक तकदीर लिखी है. इसीलिए इस बार भी राजनीतिक पार्टियों ने अपने जातीय समीकरण को ठीक करने की कवायद शुरू कर दी है. उन्हें एकजुट करने के लिए हर दल तरह-तरह के हथकंडे अपना रहा है.
जातीय राजनीति के इस घमासान में विकास का सवाल हर बार गौण हो जाता है. नेताओं ने राजनीति में इतनी उपजातियां खड़ी कर दी हैं कि वे आपस में ही लड़ रही हैं. जिससे सामाजिक समरसता कायम नहीं हो पा रही है. क्या इस बार जातीय राजनीति से ऊपर उठकर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे अथवा जातीय गठजोड़ का आधार ही सत्ता हासिल करने की कुंजी बनेगा? इस चुनावी महासमर में अबूझ पहेली बनकर यह सवाल तैर रहा है.
धर्म और जाति की राजनीति के सहारे सत्ता के शिखर तक पहुंचने वाले दलों का सच जानने और समझने का उचित समय आ गया है. इसलिए इन्हें कसौटी पर कसा जाना जरूरी है क्योंकि इस दौर में राजनीतिक दलों ने आमजन की भावनाओं को उभार कर ही चुनावी वैतरणी पार की है पर हर बार छला मतदाता ही गया है. सभी दलों ने उन्हें अपने मोहरे के तौर पर अपने राजनीतिक हित के लिए उपयोग किया है. बिहार की तरह उत्तर प्रदेश भी गरीबी की मार से कराह रहा है. पूर्वाचल और बुंदेलखण्ड में किसानों की भुखमरी से मौतें हो रही हैं. पूर्वाचल में बाढ़ और बाढ़ के बाद इंसफ्लाइटिस की बीमारी लाइलाज बनी हुई है. रोजगार की तलाश में नौजवानों का पलायन हो रहा है. यहां की युवाशक्ति मुंबई-दिल्ली की फैक्टरियों और सिक्यूरिटी गार्ड कम्पनियों में नौकरी करने को मजबूर है.
योजना आयोग की रिपोर्ट को मानें तो प्रदेश के लोगों का रहन-सहन, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक स्तर ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय औसत का मुकाबला किया जा सके. इतना ही नहीं देश की कुल जीडीपी में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग दस वर्षो में 9.7 प्रतिशत से घटकर 8.1 प्रतिशत रह गई है. हालत यह है कि गांवों में बूढ़े और बच्चों के अलावा नौजवान हैं ही नहीं. मनरेगा भी उनके इस पलायन को नहीं रोक पा रही है. उद्योगों और चीनी मिलों की खस्ताहाल किसी से छुपा नहीं है. कानून व्यवस्था का सवाल यक्ष प्रश्न बनकर खड़ा है. दु:खद यह है कि राजनीतिक दलों के एजेण्डे में ये सवाल हाशिये पर हैं. जातीय राजनीति ही उनकी राजनीति के केन्द्र में है. क्या यह विस चुनाव पड़ोसी राज्य बिहार की तरह जातीय गठजोड़ की राजनीति को तोड़ सकेगा? प्रदेश में विकासोन्मुखी राजनीति के कपाट खुलेंगे?
उत्तर प्रदेश विधानसभा के इस चुनाव पर देश भर की नजरें टिकी हुई हैं. चुनावों के परिणाम सदा की भांति देश की राजनीति के दिशा सूचक होंगे क्योंकि केंद्रीय सत्ता की राह उत्तर प्रदेश से होकर जाती है. वैसे इस चुनावी महासमर में सत्तारूढ़ बहुजन समाज पार्टी के साथ-साथ समाजवादी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है. किंतु मुख्य मुकाबला बसपा और सपा के ही बीच है. भाजपा और कांग्रेस तीसरे और चौथे स्थान के लिए लड़ रही हैं. वर्ष 1993 में मुलायम सिंह यादव के साथ पिछड़ा और दलित गठजोड़ के सहारे सत्ता में आई बसपा इस दौर में सत्ता के खेल में वर्ष 2007 में सर्वजन के नारे के सहारे अपने बलबूते पर सत्ता पर काबिज हो गई है. सुश्री मायावती ने दलित और ब्राह्मण का कार्ड खेला था किंतु इस पांच साल में बहुत पानी बह गया है. यह गठजोड़ आज नाजुक दौर में है. ब्राह्मणों का आकषर्ण बसपा से घटा है. इसीलिए भाजपा और कांग्रेस इस वोट बैंक में सेंध लगाने में जुट गई हैं.
इसके विपरीत दलितों के उत्साह में भी थोड़ी कमी आई है. भ्रष्टाचार और लचर कानून व्यवस्था कोढ़ में खाज की तरह है. इसलिए सुश्री मायावती इस गठजोड़ को इस चुनाव में भी छिटकने न देने में जुट गई हैं. सतीश मिश्र के सहारे वह पुन: ब्राह्मणों को रिझाने की जुगत में हैं. दलित योजनाओं को निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी हैं. सरकार के खिलाफ जनसवालों को लेकर उपजे गुस्से को कम करने के लिए सुश्री मायावती ने प्रदेश को चार भागों में बांटने का राजनीतिक दांव चला है. साथ ही मुसलमानों को रिझाने के लिए उन्हें आरक्षण देने की रणनीति को अंजाम देने जा रही हैं ताकि दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण वोटों के सहारे सत्ता बचाई जा सके. किंतु यह इतना आसान नहीं दिखता है.
भ्रष्टाचार, निरंकुश नौकरशाही, बिगड़ी कानून व्यवस्था आदि के जिन मुद्दों पर जनता ने उन्हें सत्ता सौंपी थी, वे अब भी बने हुए हैं. सपा इन्हीं सवालों को उठाकर बसपा और सरकार को बेनकाब कर रही है. उसके प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने क्रांतिरथ के जरिये चुनावी माहौल बना रहे हैं. वे मिल रहे भारी जनसमर्थन से उत्साहित भी हैं. मुलायम सिंह भी पिछड़ा-मुस्लिम गठजोड़ को बिखरने न देने की जुगत में हैंताकि मायावती की हर राजनीतिक चाल को कुंद किया जा सके.
उधर, भाजपा कलराज मिश्र के सहारे ब्राह्मण मतदाताओं को अपने पाले में लाना चाहती है तो ठाकुरों को रिझाने के लिए राजनाथ सिंह को उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड की चुनावी कमान सौंपी है. किन्तु भाजपा खुद अंतर्कलह की शिकार है. वह शहरी मतदाताओं को अपने पाले में रखने के लिए वह सजग नहीं दिखती है. वहीं कांग्रेस पिछले 25 वर्षो में गैर कांग्रेसी सरकारों के शासनकाल में प्रदेश की हुई बदहाली को मुद्दा बना रही है. राहुल गांधी ने कांग्रेस की सत्ता में वापसी की कमान स्वयं संभाल रखी है. वह दलितों के बीच जा रहे हैं. युवकों से सीधा संवाद करते हैं तो किसानों की हक की लड़ाई लड़कर सबका समर्थन चाहते हैं. कांग्रेस की कोशिश उत्तर प्रदेश में किसी तरह अपने पुराने वोट बैंक दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण को साथ लाने की है, जो अयोध्या की घटना के बाद उससे छिटक गया था. राहुल की यह कोशिश इस चुनाव में क्या रंग लाती है, यह अभी स्पष्ट नहीं है किंतु इतना जरूर है कि उनकी सक्रियता ने बसपा और भाजपा की बेचैनी बढ़ा दी है.
उत्तर प्रदेश का चुनावी राजनीतिक परिदृश्य अभी धुंधला है. जातीय राजनीति अपने चरम पर है. हर जातियों में बिखराव है. न मुसलमान और न ही ब्राह्मण किसी का वोट बैंक बनने को तैयार हैं. दलित मतदाता भी हाथी निशान देखकर बटन दबाने की मानसिकता में पहले जैसे नहीं दिख रहे हैं. ऐसे में वोटों के बिखराव का लाभ किसे मिलेगा? राजनीतिक विश्लेषक इसी राजनीतिक उलझन को सुलझाने की कसरत में लग गए हैं. ऐसे में जातीय राजनीति के इस झंझावात में विकास और कानून व्यवस्था का सवाल चुनावी मुद्दा बन सकेगा. इन सवालों के बीच प्रदेश के मतदाता एक बार फिर कसौटी पर हैं.
| Tweet |