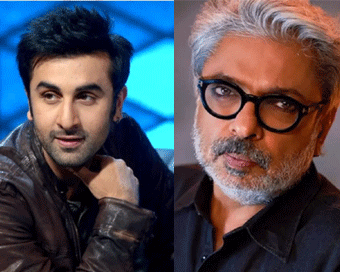यह बांटना नहीं, भटकाना होगा
तेलंगाना और गोरखालैंड राज्यों की मांग के साथ ही अब उत्तर प्रदेश को चार भागों में बांटने की मांग भी तेज हो गई है.
 |
चुनावी लाभ के लिए बसपा सुप्रीमो और प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने इस मांग के साथ एक राजनीतिक दांव चला है. इससे पहले वह मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए भी प्रधानमंत्री को पत्र लिख चुकी हैं. उनके इन सियासी अंदाजों से उनके विरोधी हलकान हो गए हैं. सूबे को बांटने और मुस्लिम आरक्षण जैसी मांगों के राजनीतिक निहितार्थ एकदम स्पष्ट हैं.
पहला मकसद तो अपनी सरकार के खिलाफ जोर पकड़े जनाक्रोश को दूसरी ओर मोड़ना है. ऐसा करके मायावती बिगड़े दिख रहे चुनावी अंकगणित को ठीक करना चाहती हैं. उनका मंसूबा प्रदेश के विभाजन के पैरोकारों की भावनाओं को उभारकर या उनका भरोसा जीत कर उसे वोट बैंक में तब्दील करना है. इसलिए, आगामी 21 नवम्बर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में विभाजन प्रस्ताव पारित कराकर वह मामले को केंद्र के पाले में डालने जा रही हैं. दूसरा आशय चुनाव में कांग्रेस-राष्ट्रीय लोकदल के सम्भावित गठबंधन के राजनीतिक प्रताप को निस्तेज करना या उसकी धार को भोथरा करना है. इस तरह सूबे में शह-मात का राजनीतिक खेल अभी से शुरू हो गया है.
मायावती या बंटवारे के समर्थक सियासी लोग इस सच को नजरअंदाज कर रहे हैं कि छोटे राज्यों से जुड़े अनुभव अभी तक अच्छे नहीं रहे हैं. इनके गठन के बाद समस्याएं और बढ़ी ही हैं. अधिकतर छोटे राज्य राजनीतिक अस्थिरता के शिकार बने हैं. उनका विकास बुरी तरह बाधित हुआ है.
ऐसे में तेलंगाना-गोरखालैंड और अब उत्तर प्रदेश के बंटवारे की मांगें वास्तव में इन क्षेत्रों के लिए तरक्की के रास्ते खोलेंगी अथवा आपसी कलह का सबब बनेंगी; इन मसलों पर उम्मीदें कम और आशंकाएं ज्यादा हैं. एक कहावत आम है कि ‘सियासत में सत्ता के लिए सब कुछ जायज है’. उत्तर प्रदेश विभाजन की मांग इससे मेल खाती है. इस सवाल पर सियासी पार्टियों की समझ को पानी में तेल की तरह तैरते देखा और समझा जा सकता है. केवल मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी ही प्रदेश के विभाजन की मांग का खुलकर विरोध कर रही है जबकि कांग्रेस और भाजपा इस सवाल पर ‘न सांप मरे न लाठी टूटे’ की नीति अपनाए हुई हैं.
कांग्रेस-भाजपा को फिक्र है कि कहीं इस मुद्दे पर बसपा बाजी न मार ले. लिहाजा, दोनों फूंक-फूंक कर कदम रख रही हैं. कांग्रेस वैसे तो द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग की वकालत कर रही है पर जानकारों का यह भी कहना है कि यदि सुश्री मायावती सदन में विभाजन का प्रस्ताव लाती हैं तो कांग्रेस उसका समर्थन कर सकती है.
इसके जरिये जनता में वह यह संदेश देगी कि कांग्रेस के चाहे बगैर प्रस्ताव सदन में पारित ही नहीं हो सकता था क्योंकि इसके लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत उसके व रालोद के समर्थन के वगैर संभव नहीं है. दूसरे, कांग्रेस अपनी नई सियासी दोस्त रालोद और उसके नेता अजित सिंह को भी नाराज नहीं करना चाहती जो काफी लम्बे समय से हरित प्रदेश की मांग उठाते रहे हैं. भाजपा इस मुद्दे पर दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहती है. इसीलिए उसने बंटवारे के मसले पर जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेने की एक आड़ ली है.
इसके विपरीत, सपा विभाजन के साफ खिलाफ है. वह मानती है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में राज्यों को मजबूत होना चाहिए. छोटे राज्य केंद्र पर दबाव बनाने की स्थिति में नहीं होते. अगर बड़े राज्य विघटित कर छोटे राज्य बना दिये जाते हैं तो केंद्र सरकार निरंकुश हो सकती है. छोटे राज्य अपने हितों के लिए आपस में उलझे रह जाएंगे और केंद्र सरकार उन पर मनमाने फैसले लाद सकती है.
आज ज्यादातर छोटे राज्यों की स्थिति खराब है. दस साल पहले बने उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड आज यह प्रमाणित कर रहे हैं कि छोटे राज्य आदर्श राज्य नहीं हो सकते. इसलिए उत्तर प्रदेश की वह दुर्गति नहीं होने दी जाएगी. अन्य सियासी पार्टियों को भी समाजवादी पार्टी की तरह अपने राजनीतिक फलक को बड़ा करना चाहिए और इतिहास से सबक लेना चाहिए.
अब उत्तर प्रदेश पर गौर करें. सूबा कर्ज में डूबा है. इसके पूर्वाचल के कई जिले आज भी उद्योग शून्य हैं तो चीनी मिलें खस्ताहाल हैं. कई सीमेंट और खाद के कारखाने लम्बे समय से बंद पड़े हैं.
अगर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा (प्रस्तावित हरित प्रदेश) अपने मूल से आज अलग हो जाए तो सूबे के अन्य क्षेत्रों की हालत और बदतर हो जाएगी. विभाजन की यह राजनीति प्रदेश के लिए एक बड़ी राजनीतिक त्रासदी हो सकती है. उप्र की आम जनता को प्रदेश के व्यापक हित में खड़ा होना चाहिए क्योंकि बंटने से केंद्र में राजनीतिक सौदेबाजी की उसकी ताकत स्वत: कम हो जाएगी. क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ने के साथ-साथ राज्यों के बीच टकराव बढ़ेगा सो अलग.
इस परिप्रेक्ष्य में छोटे राज्यों की वकालत करने वाली पार्टियों के सामने सचाई रखना जरूरी हो गया है. देश में छोटे राज्यों का बड़ा प्रयोग पूर्वोत्तर से हुआ था. जाति-समूहों, गुटों और कबीलों को ध्यान में रखकर राज्य बनाये गये थे. उस समय यह आम धारणा थी कि स्थानीय लोगों को सत्ता दिये जाने से शांति आएगी. राज्यों का विकास स्थानीय जन-भावनाओं के मुताबिक होगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ. असम की बात फिलहाल जाने दें तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नगालैंड में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है. यहां जातीय संघर्ष वर्षो से चल रहा है. परिणामस्वरूप इन राज्यों में भारी तादाद में उग्रवादी गुट सक्रिय हैं. यहां कबीले और दबावकारी समूह इतने हावी हैं कि वह अपनी मर्जी के मुताबिक सरकारें चलाते हैं.
अरुणाचल में चल रहा राजनीतिक संकट इसका ताजा प्रमाण है. पश्चिम में गोवा भी इसी अस्थिरता का शिकार है. यहां छोटे-छोटे दलों द्वारा आये दिन सरकार को ब्लैकमेल किया जाता है. छत्तीसगढ़ के दो-तिहाई जिलों पर नक्सलियों का राज कायम है. वे उद्योगपतियों और व्यापारिक घरानों से खुलेआम वसूली कर रहे हैं. क्या इसी के लिए राज्य बनाया गया था? इसके अलावा झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, जिसके कारण विकास ही नहीं हो पा रहा और भ्रष्टाचार तो चरम पर है ही. केवल केरल, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा अपवाद माने जा सकते हैं.
इस तथ्यों की रोशनी में मेरा विचार है कि देश की एक बड़ी आबादी जब तक गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण और बेरोजगारी की मार झेल रही है; उसके असंतोष को डायवर्ट करने के लिए अलग राज्यों की मांग होती रहेगी. अत: इन मांगों से बचने के लिए जरूरत उन समस्याओं को प्राथमिकता से खत्म करने की है. इनकी जवाबदेही सियासी दलों की है. इन्हें पूरा करने की बजाय उन्हें क्षेत्रीय भावनाओं को उभारने का राजनीतिक खेल नहीं खेलना चाहिए और सूबे को चार हिस्सों में बांटने की मांग से तौबा करनी चाहिए.
| Tweet |