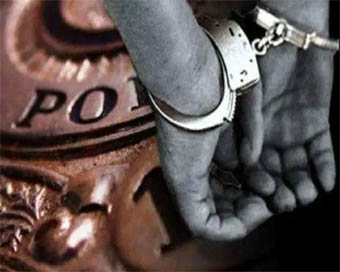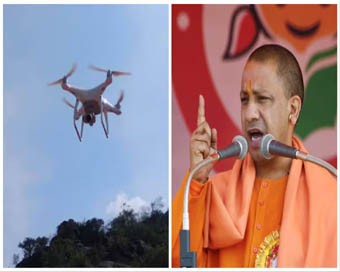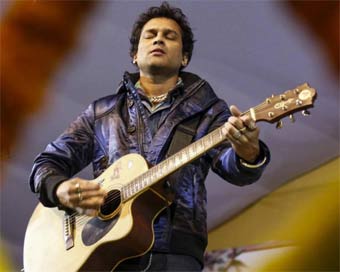विकास : उचित मूल्यों से ही संभव है बेहतर दुनिया
प्राय: विकास का मुख्य द्योतक यह माना जाता है कि भौतिक वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धि कितनी बढ़ रही है पर इस संकीर्ण सोच पर आधारित विकास तब तक सार्थक नहीं माना जा सकता जब तक उससे सभी मनुष्यों और जीवन रूपों की भलाई से जुड़े जीवन मूल्यों का समावेश न हो और ऐसे जीवन मूल्यों के प्रति आस्था मजबूत न बने।
 विकास : उचित मूल्यों से ही संभव है बेहतर दुनिया |
ऐसे जीवन मूल्यों के बिना मात्र भौतिक वस्तु-सेवाओं की बढ़ती उपलब्धि पर आधारित विकास से तमाम समस्याएं आ सकती हैं।
सार्थक जीवन-मूल्य क्या हैं, इस पर विद्वान और दार्शनिक बहुत कुछ कह चुके हैं पर यहां हम इसे सबसे सरल और संक्षिप्त रूप में ही रखते हैं-मनुष्य यथासंभव सदा इस बारे में ध्यान रखे कि उसके किसी कार्य और वचन से किसी दूसरे व्यक्ति या जीव-जंतु को दुख और कष्ट न हो। यह इतनी सरल बात है कि अधिकांश लोग कहेंगे कि इसमें नया क्या है, यह तो बहुत बार सुन चुके हैं। पर जरा सोच कर तो देखिए-इस बहुत से सरल जीवन सिद्धांत का दैनिक जीवन में ही क्या बार-बार उल्लंघन नहीं होता है। दूसरी ओर यदि हम इसके प्रति बहुत सचेत और सावधान हो जाएं तो क्या हमारे जीवन में, आपके जीवन में केवल इस आधार पर बहुत से सार्थक बदलाव नहीं जुड़ जाएंगे और क्या अनेक व्यक्तियों के इस तरह के बदलाव का व्यापक असर यह नहीं होगा कि हमारे आसपास का दुख-दर्द बहुत कम हो जाएगा। मान लीजिए कि मनुष्य आदिम अवस्था में है, कंद-मूल एकत्र कर बस पेट भरना जानता है पर उसने यह जीवन मूल्य अपना लिया है कि यथासंभव किसी को दुख नहीं पहुंचाना है तो वह आदिम समाज, जहां विज्ञान एवं तकनीकी अभी निम्नतम स्तर पर है और सभी अनपढ़ हैं, भी एक सुखी समाज होगा, वहां दुख-दर्द बहुत कम होगा। अब एक आधुनिक समाज लीजिए जहां विज्ञान, तकनीकी के बल पर सुख-सुविधा, विलासिता की तमाम सामग्री मौजूद हैं पर इस सरल सिद्धांत की कोई मान्यता नहीं है, इसका व्यापक उल्लंघन होता है। इस दूसरे समाज में पहले समाज यानी आदिम समाज की अपेक्षा अधिक दुख-दर्द, बैचेनी, असंतोष, तनाव आपको मिलेंगे। यह संभव है कि जीवन मूल्य उचित हैं तो सौ प्रतिशत अनपढ़ आदिम समाज भी अमन-शांति और सुख का समाज होगा। दूसरी ओर जीवन-मूल्य प्रतिकूल हैं तो सौ प्रतिशत शिक्षित विज्ञान और तकनीकी की प्रगति वाले समाज में भी दुख-दर्द, तनाव अधिक हो सकते हैं।
जीवन-मूल्य पहले व्यापक स्तर पर सही बन जाएं तो विज्ञान एवं तकनीकी का सही उपयोग भी दुख-दर्द कम करने में ही होने की संभावना है पर जीवन मूल्य प्रतिकूल हैं तो विज्ञान एवं तकनीकी के आगे तेजी से बढ़ने से अनुचित प्रवृत्तियां भी तेजी से बढ़ सकती हैं। अत: जो सबसे बुनियादी चुनौती है, वह यह है कि मौजूदा दुनिया में ऐसे जीवन-मूल्यों का मजबूत आधार तैयार हो जो सभी मनुष्यों और जीवन रूपों का दुख-दर्द न्यूनतम करने के अनुकूल हों।
पृथ्वी पर जीवन के लाखों रूप हैं पर केवल मनुष्य में यह क्षमता है कि वह नियोजित ढंग से पृथ्वी के लाखों विविध तरह के जीवन-रूपों की रक्षा के लिए प्रयास कर सके, उनके पनपने और फलने-फूलने के अनुकूल पर्यावरण की रक्षा कर सके। मनुष्य की विशिष्ट क्षमताओं का मूल औचित्य इसी में है कि वह जीवन के विभिन्न रूपों की रक्षा करे। यही मानवता का मुख्य उद्देश्य है। जब मनुष्य अपने इस मूल उद्देश्य और औचित्य के अनुरूप जीते हैं, तभी इंसानियत की कसौटी पर खरा उतरते हैं, तभी सही अथरे में इंसान कहलाते हैं। जितनी बढ़ती संख्या में मनुष्य इंसानियत को प्राप्त करेंगे या इसके अनुरूप जीवन जिएंगे, उतनी ही पृथ्वी पर जीवन के विविध रूपों की रक्षा होगी, उनके जीवन के पनपने के अनुकूल पर्यावरण की रक्षा होगी और धरती पर विभिन्न तरह के जीवन के फलने-फूलने की स्थितियां बनी रहेंगी, बेहतर होंगी।
इस बारे में व्यापक सहमति है कि मनुष्यों को एक-दूसरे की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। यह इंसानियत के लिए जरूरी तो है पर पर्याप्त नहीं है। जिस तरह मनुष्य दुख-दर्द अनुभव करते हैं उसी तरह जीवन के अधिकांश अन्य रूप भी दुख-दर्द अनुभव करते हैं। पृथ्वी केवल मनुष्य की नहीं बल्कि जीवन के अन्य रूपों की भी है। अत: सभी मनुष्यों की समता-भलाई के बारे में सोचना तो बहुत जरूरी है ही, पर साथ ही जीवन के अन्य रूपों की चिंता करना भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है। मनुष्यों सहित विभिन्न अन्य जीवन-रूपों की रक्षा के लिए उन समुद्रों, नदियों, वनों, मिट्टी, वायुमंडल को बचाना जरूरी है जहां से यह जीवन प्राप्त होता है। पर्यावरण बचेगा तभी जीवन के विविध रूपों की रक्षा होगी-आज भी और कल भी। आगामी पीढ़ियों की चिंता करना उतना ही जरूरी है, जितना वर्तमान की चिंता करना। सार्थक सामाजिक बदलाव की राह यही होनी चाहिए कि बढ़ती संख्या में मनुष्य अपने मूल उद्देश्य को पहचाने और विभिन्न जीवन रूपों के रक्षक के रूप में मनुष्य की मूल भूमिका को व्यापक पहचान मिले। जब इस तरह इंसानियत का प्रसार तेजी से होगा तो पृथ्वी पर मनुष्य सहित सभी जीवन रूपों के दुख-दर्द भी तेजी से कम होंगे। क्या ही अच्छी बात होती, कितनी सुंदर वह दुनिया होती, यदि पृथ्वी पर मनुष्य का जो कल्याणकारी उद्देश्य है उसके अनुकूल ही सब मनुष्यों को स्वभाव सदा के लिए मिला होता। तब सभी मनुष्य अपना जीवन एक-दूसरे की और जीवन के अन्य रूपों की भलाई के लिए जीते और दुनिया सभी के लिए बहुत कल्याणकारी होती। किंतु अफसोस ऐसा नहीं है। अपने मूल कर्त्तव्य और औचित्य के अनुरूप जीवन जीने के गुण ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाते हैं अपितु उन्हें विकसित करने के लिए काफी प्रयास करना पड़ता है। सभी मनुष्य ऐसे ही इंसान नहीं बन जाते, काफी प्रयास करने के बाद इंसान बन सकते हैं। हां, यदि समाज में अनुकूल माहौल हो तो मनुष्यों के इंसान बनने की संभावना बढ़ जाती है, यह कार्य सहज हो जाता है और अधिक संख्या में मनुष्य इंसान बनने लगते हैं।
एक बड़ा सवाल यह है कि ऐसा अनुकूल माहौल कैसे बने। सही प्रगति और विकास वह है जो ऐसा अनुकूल माहौल बनाने में सहायक हो। मनुष्य में जो प्रवृत्तियां हैं, वे इंसानियत के अनुकूल भी हो सकती हैं और प्रतिकूल भी। पर यदि उन्हें उचित सामाजिक परिवेश मिलेगा, अनुकूल सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था मिलेगी, तो इंसानियत के अनुकूल प्रवृत्तियों को खिलने का भरपूर अवसर मिलेगा और जो इंसानियत के प्रतिकूल प्रवृत्तियां है, उन पर रोक लगेगी। अत: जो एक बड़ी खोज है वह ऐसी सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था की खोज है जो मनुष्य को इंसानियत की राह पर चलने के लिए प्रोत्साहन देती है, और जब वह उससे भटकता है तो उसे राह सुधारने में मदद करती है और फिर भी न माने तो उसे रोकती है। यह खोज मोहल्ले और गांव स्तर पर भी है, देश और दुनिया स्तर पर है। यह खोज बड़े विद्वानों की भी है, बड़े नेताओं की भी है पर आम लोगों की भी है। ऐसी सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक व्यवस्था हम कायम कर सकें तो यह हमारा हमारे बच्चों, भावी पीढ़ियों के लिए सवरेत्तम उपहार होगा। अत: विभिन्न तरह की संकीर्ण बहसों के स्थान पर ऐसी व्यवस्था की स्थापना पर अधिक ध्यान देना चाहिए।
| Tweet |