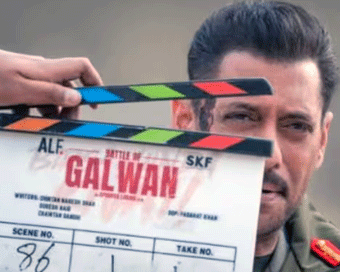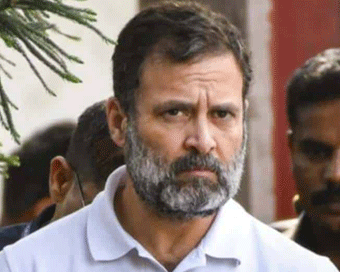हर मसला अदालत पर नहीं छोड़ा जा सकता
न्यायपालिका (Judiciary) देश की रीढ़ है। इसके मजबूत कंधों पर लोकहित के कई महती कार्य हैं, लेकिन हास्यास्पद है कि उन मसलों में इसे अपना कीमती वक्त जाया करना पड़ रहा है जो खालिस रूप से केंद्र या राज्यों की जिम्मेदारी है।
 हर मसला अदालत पर नहीं छोड़ा जा सकता |
दरअसल, हाल ही में सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने केंद्र सरकार को मेंस्ट्रुअल हाइजीन (menstrual hygiene) पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चार हफ्ते के अंदर एक समान नीति बनाकर रिपोर्ट पेश करने का आदेश पारित किया है। साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से स्कूलों में लड़कियों के टॉयलेट की उपलब्धता और सेनेटरी पैड (sanitary pad) की आपूर्ति को लेकर जानकारी भी मांगी है।
हैरानी की बात है कि आजादी के इतने सालों बाद भी महिलाओं की सेहत और स्वास्थ्य से जुड़े इस सबसे संवेदनशील मुद्दे पर आज भी न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ा रहा है। इस सबसे अहम और सबसे गंभीर विषय को न तो कभी सार्वजनिक चर्चा का विषय बनाया गया न ही इसे किसी व्यापक नीति का हिस्सा बनने दिया गया।
वैसे भी महिलाओं के जीवन से जुड़ी इस मामूली सी जरूरत को किसी बड़े बजट या किसी बड़े ताम-झाम की जरूरत नहीं। इससे जुड़े आंकड़े चिंता पैदा करते हैं। उत्तर भारत के राज्यों मसलन-उत्तर प्रदेश में 69.9, बिहार में 67.5 और उत्तराखंड में 55 प्रतिशत वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों यथा-असम में 69.1 और सिक्किम में 85 प्रतिशत तथा छत्तीसगढ़ में 68.6 प्रतिशत लड़कियां आज भी पैड के अभाव में कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, जो स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद असुरक्षित है।
हालांकि दक्षिण भारत के राज्य सुरक्षित माहवारी उपायों के मामले में थोड़े बेहतर हैं। तमिलनाडु 91 तो केरल 92 प्रतिशत वहीं गोवा 89 प्रतिशत के साथ राज्यों में सबसे अव्वल हैं, जहां सैनेटरी नैपकिन इस्तेमाल करने वाली महिलाओं का प्रतिशत सबसे अधिक है।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family Health Survey) की हालिया रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती है कि देश में कुल 82 प्रतिशत महिलाएं महावारी के दौरान रक्तस्राव (bleeding during menstruation) को रोकने के लिए घरेलू कपड़े का उपयोग करती हैं और केवल 42 प्रतिशत महिलाएं नियमित रूप से सैनेटरी नैपकिन के इस्तेमाल से खुद को सुरक्षित रखती हैं। इसमें भी ग्रामीण और शहरी महिलाओं के आंकड़ों में भारी अंतर है।
सैनेटरी पैड इस्तेमाल करने वाली ग्रामीण महिलाओं का प्रतिशत जहां केवल 48 है तो वहीं 78 प्रतिशत शहरी महिलाएं नैपकिन का नियमित इस्तेमाल कर पाती हैं। क्या इसके पीछे जागरूकता की कमी और वर्जनाओं को जिम्मेदार ठहरा कर पल्ला झाड़ा जा सकता है। एक कल्याणकारी राज्य अपने नागरिकों की स्वास्थ्य और शिक्षा कि महती जिम्मेदारियों से कब तक भाग सकता है। इस अतिसंवेदनशील मसले पर न केवल बजट में अलग से चर्चा हो अपितु सरकारी नीतियों में भी इसे प्रमुखता से स्थान दिया जाए।
आखिर आधी आबादी के बेहतर स्वास्थ्य के बूते ही देश में एक सेहतमंद पौध तैयार की जा सकती है। जन स्वास्थ्य का मुद्दा अनावश्यक चिक्तिसीय भार से भी जुड़ा है। यदि इस पर त्वरित काम न किया गया तो देश की चिकित्सा सेवा पर भार और दायित्व दोनों का बोझ बढ़ेगा, जिससे अर्थव्वयस्था चरमराएगी। जनजागरूकता, सैनिटरी नैपकिन के इस्तेमाल से जुड़ी ग्रामीण कार्यशालाएं, स्कूलों में मुफ्त नैपकिन वेंडिग मशीनों की स्थापना और इसे वस्तु कर से मुक्त कर इस दिशा में सकारात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं।
| Tweet |