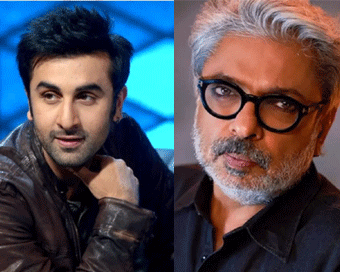मुद्दा : प्लास्टिक का विकल्प क्या
प्लास्टिक के विकल्प ने हमारी जिंदगी को आसान किया है.
 मुद्दा : प्लास्टिक का विकल्प क्या |
पॉलीथिन की थैलियां और प्लास्टिक की चीजें (रंग-बिरंगे पेन-पेंसिल से लेकर डिजाइनर लंच बॉक्स और पानी की बोतलें तक) हमारे जीवन में अनायास नहीं आई. साइंस की तरक्की और उससे मिलने वाली सुविधा ने उन्हें जीवन में शामिल कराया है. निश्चय ही प्लास्टिक ने काफी सुविधाएं दीं, लेकिन समस्या यह है कि इसका 70 फीसद हिस्सा अब कबाड़ (प्रदूषित-जहरीले कचरे) के रूप में धरती पर मौजूद है. आज हर कोई प्लास्टिक से पर्यावरण और हमारे जीवन पर पड़ने वाले खराब असर की बात करता है, पर मजबूरी यह है कि किसी को इसका ठोस विकल्प नहीं सूझ रहा.
प्लास्टिक का सबसे खराब पहलू यह है कि जितनी देर इससे बनी चीजें इस्तेमाल में लाई जाती हैं, उसके मुकाबले सैकड़ों गुना ज्यादा वक्त इनके नष्ट होने में लगता है. पिछले वर्ष अगस्त में प्रश्नकाल के दौरान संसद में तत्कालीन पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी दी थी कि देश के 60 बड़े शहर रोजाना 3500 टन से अधिक प्लास्टिक-पॉलीथिन कचरा निकाल रहे हैं. वर्ष 2013-14 के दौरान देश में 1.1 करोड़ टन प्लास्टिक की खपत हुई जिसके आधार पर जानकारी मिली कि दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद जैसे बड़े शहर सर्वाधिक प्लास्टिक कचरा निकाल रहे हैं. प्लास्टिक-पॉलीथिन से बनी दूध व पानी की बोतलों, लंच बॉक्स या डिब्बाबंद खाद्य पदाथरे का सेवन मनुष्य स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है क्योंकि गर्मी, धूप आदि कारणों से रासायनिक क्रियाएं प्लास्टिक के विषैले प्रभाव उत्पन्न करती हैं, जो कैंसर आदि तमाम बीमारियां पैदा कर सकती हैं. जिन डिस्पोजल बर्तनों, कप-प्लेटों में खाने और चाय-कोल्ड ड्रिंक आदि पेय पदार्थ मिलते हैं, कुछ समय तक उनमें रखे रहने के कारण रासायनिक क्रियाएं होने से वह खानपान विषैला हो जाता है.
प्लास्टिक में अस्थिर प्रकृति का जैविक काबर्निक एस्सटर (अम्ल और अल्कोहल से बना घोल) होता है, जो कैंसर पैदा करने में सक्षम है. सामान्य रूप से प्लास्टिक को रंग प्रदान करने के लिए उसमें कैडमियम और जस्ता जैसी विषैली धातुओं के अंश मिलाए जाते हैं. जब ऐसे रंगीन प्लास्टिक से बनी थैलियों, डिब्बों या अन्य पैकिंग में खाने-पीने के सामान रखे जाते हैं, तो ये जहरीले तत्व धीरे-धीरे उनमें प्रवेश कर जाते हैं. उल्लेखनीय है कि कैडमियम की अल्प मात्रा शरीर-पेट में जाने से उल्टियां हो सकती हैं, हृदय का आकार बढ़ सकता है. इसी प्रकार यदि जस्ता नियमित रूप से शरीर में पहुंचता रहे, तो इंसानी मस्तिष्क के ऊत्तकों का क्षरण होने लगता है, जिससे अल्झाइमर जैसी बीमारियां होती हैं. जहां तक प्लास्टिक की रोकथाम और इसे चलन से बाहर करने का प्रश्न है, तो पिछले सितम्बर में केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके दवाओं को प्लास्टिक से बनी शीशियों व बोतलों में पैक करने पर रोक लगाने का इरादा जाहिर किया था. दवाओं की प्लास्टिक शीशियां और बोतलें मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण, दोनों के लिए हानिकारक हैं. हालांकि दवा उद्योग इसके लिए राजी नहीं है क्योंकि इससे उसके कारोबार पर असर पड़ सकता है. पिछले एक दशक में कई तरह के सीरप, टॉनिक और दवाएं प्लास्टिक पैकिंग में बेची जाने लगी हैं. वजह यह है कि ये शीशियां और बोतलें सस्ती पड़ती हैं. इनके टूटने का खतरा भी नहीं होता. वैज्ञानिकों का दावा है कि प्लास्टिक बोतलों में पाए जाने वाले खास तत्व-थैलेट्स-सेहत पर प्रतिकूल असर डालते हैं. इनकी वजह से हॉर्मोनों का रिसाव करने वाली ग्रंथियों का क्रियाकलाप बिगड़ जाता है.
अब यह सवाल असल में साइंस और इंजीनियरिंग के लिए ज्यादा जरूरी है कि क्या प्लास्टिक का उससे बेहतर नहीं तो क्या एक समकक्ष समाधान सुझाया जा सकता है. ध्यान रहे कि सिर्फ पाबंदियों और सरकारी आह्वानों के बल पर ही विकल्पों की राह नहीं रोकी जा सकती. इसके लिए जरूरी है कि दुनिया प्लास्टिक-पॉलीथिन का और भी बेहतर विकल्प सुझाए. इस बारे में अमेरिकी साइंटिस्ट डॉ. रोलैंड गेयेर कहते हैं कि यह दुनिया बहुत तेजी से ‘प्लास्टिक प्लैनेट’ बनने की ओर अग्रसर है. ऐसे में बेहतर विकल्प यह ही है कि लोग प्लास्टिक के बजाय प्राकृतिक चीजों, जैसे जूट, पत्तलों आदि से बनी चीजों का इस्तेमाल करें. बेशक पाबंदी एक इलाज है, लेकिन सुविधाजनक प्लास्टिक के आगे कोई रोक टिक नहीं पाती. ऐसे में उपाय यही बच रहता है कि लोग खुद ही प्लास्टिक से इतर विकल्पों को आजमाएं.
| Tweet |