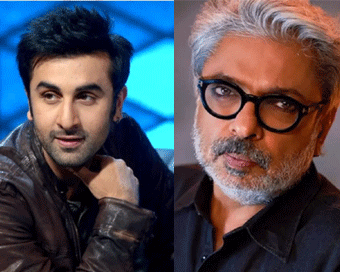प्रणब मुखर्जी : बहुलतावाद के पक्ष में
जिस दिन प्रणब मुखर्जी सेवानिवृत्त हो रहे थे, राष्ट्रपति भवन में उन्हें एक पत्र मिला. पत्र नरेन्द्र मोदी का था.
 प्रणब मुखर्जी |
प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा था, ‘प्रणब दा, आप हमेशा मेरे लिए पिता समान और मार्गदशर्क रहे.’ इस देश का दुर्भाग्य ही है कि जिसे मोदी सरीखे तेज-तर्रार प्रधानमंत्री ने अपना मार्गदर्शक माना, उससे देश के ही कुछ अति उत्साही नागरिक कुछ भी नहीं सीख पाए. पांच साल का राष्ट्रपति का अपना कार्यकाल निर्विघ्न पूरा करने से एक दिन पहले प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दिया था. उसे सिर्फ रस्मी भाषण नहीं समझा जाना चाहिए. उन्होंने कहा था, ‘भारत की आत्मा इसकी सहिष्णुता में निवास करती है.’ यह ध्यान देने की बात है कि सेवानिवृत्त हो रहे राष्ट्रपति ने विदाई के समय अपने देश के लोगों से कहने के लिए यही विषय क्यों चुना?
मुखर्जी राष्ट्रपति चुने जाने से पहले कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक थे. कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुने गए थे. लेकिन कांग्रेस की धुर विरोधी बीजेपी जब सत्ता में आई तो राष्ट्रपति भवन से पार्टी को कभी कोई असुविधा नहीं हुई. नीलम संजीव रेड्डी की तरह कोई विवाद नहीं हुआ. राजेन्द्र प्रसाद या ज्ञानी जैल सिंह की तरह केंद्र सरकार से किसी मुद़्दे पर असहमति नहीं हुई. प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुखर्जी, दो अलग-अलग पार्टयिों से आये थे. दोनों की विचारधाराएं अलग-अलग थीं. लेकिन इस बिंदु पर दोनों समान रूप से सहमत थे कि हमारे लोकतंत्र में अलग-अलग दृष्टिकोण रखने के बावजूद अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह गरिमापूर्ण और प्रभावी ढंग से किया जा सकता है. दोनों ने अपने इस मर्यादापूर्ण आचरण का आदर्श उदाहरण पेश किया.
उसी राष्ट्रपति ने जाते समय जब देशवासियों को भारत की सांस्कृतिक बहुलता की याद दिलाई, तो कोई बड़ा कारण ही रहा होगा. उन्होंने कहा कि अनेक भाषाओं और संस्कृतियों का यह संगम सदियों के सहजीवन से विकसित हुआ है. सबको अपने में समाहित कर लेने और साथ ले कर चल सकने की वजह से ही आज हम दूसरों से अलग पहचान कायम कर सके हैं. इसके बाद उन्होंने इस तथ्य की ओर संकेत किया कि आज किस तरह वैचारिक असहिष्णुता और हिंसा बढ़ रही है. और हम चाहे सहमत हों या असहमत, हमें अपने लोकतंत्र में विचारों की विविधता को जगह देनी ही होगी. जिस रोज देश के तत्कालीन राष्ट्रपति अपनी चिंता देश के साथ साझा करने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय एक टीवी चैनल पर कुछ एंकर अपनी व्यथा सुना रहे थे कि डिबेट में जब भी वे किसी पार्टी के नेता से कोई तीखा सवाल करते हैं, तो सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, और उन्हें ‘मां-बहन की गालियां’ सुनाई जाती हैं. इस तरह की शिकायतें अखबारों के कई संपादकों और सभा-सेमिनारों में विचार व्यक्त करने वाले बुद्धजीवी भी करते हैं. सोशल मीडिया पर अपने विरोधियों या असहमति रखने वाले लोगों को इस तरह गालियां सुनाने वाले लोग कौन होते हैं? सभाओं में किसी वक्ता के विचारों से असहमत होने पर उससे मारपीट करने वाले लोग आखिर कहां से आते हैं? क्या वे उसी देश के नागरिक नहीं हैं, जिस देश के राष्ट्रपति उन तक अपनी वह चिंता पहुंचाना चाहते थे?
जिस समय तत्कालीन राष्ट्रपति अपनी चिंता देश के साथ साझा कर रहे थे, उसी समय देश में एक और बहस चल रही थी, भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा को ले कर, मॉब लिंचिंग की बढ़ती प्रवृत्ति को लेकर. इस मुद्दे को ले कर कई जगह प्रदर्शन हो चुके हैं, और अब तो लगता है कि संसद भी उस असहिष्णु आक्रामकता की गर्मी से बच नहीं पा रही है. राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है. तो सोचने की बात है कि देश के प्रथम नागरिक और नागरिकों के ऐसे समूहों के सोचने के ढंग में इतना अंतर क्यों है? क्या अन्य नागरिकों को प्रथम नागरिक की चिंता पर विचार करना चाहिए, क्या उसके बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए, क्या कोई बाहरी कारण दोनों की सोच के बीच इतनी बड़ी खाई पैदा कर रहा है? राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक मानने से हमारा क्या आशय है? क्या वह उसकी महिमा का बखान करने के लिए गढ़ा गया आडंबरपूर्ण शब्द है? क्या वोटर लिस्ट में लिखा हुआ पहला नाम है? या इसका कोई नैतिक पक्ष भी है? यदि प्रथम नागरिक देश के आदर्श नागरिक की तरह आचरण करता है, देश के हित के बारे में सबसे पहले सोचता है, नागरिक के रूप में देश के हित में पहला कदम उठाने का अधिकारी है, तो अन्य नागरिकों से भी अपेक्षा की जाती है कि उसका अनुसरण करें. ऐसे में विदाई संदेश को क्या चुनावी भाषणों की तरह सुनने के बाद बिसरा देना उचित होगा?
जो कल देश का प्रथम नागरिक था, वह आज नहीं है. आज एक सामान्य नागरिक है. तो सामान्य नागरिक होते ही क्या उसके सोचने का ढंग बदल जाएगा? क्या वह भी देश के उस आक्रामक नागरिक समूह की तरह भाषायी हिंसा पर उतारू हो जाएगा? यदि ऐसा नहीं होगा, तो देश में दो तरह के विचार रखने वाले बने रहेंगे. एक वे जो देश को बहुलतावादी समझते हैं. दूसरे वे जो अपनी सोच से अलग सोच रखने वालों को कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहते. ऐसे नागरिक, जो अपने विचारों से असहमत होने वालों को गाली दे रहे हैं, या उस असहमति को दबाने के लिए शारीरिक हिंसा का सहारा ले रहे हैं, वे प्रथम नागरिक की बातों को (और संवैधानिक मूल्यों को) अपनी इच्छा और सुविधा से आदर दे सकते हैं, या अपमानित कर सकते हैं. यह भी कह सकते हैं कि तो कांग्रेसी एजेंट था, जाते-जाते पिन चुभो गया. लेकिन तब उन्हें नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कोविंद का भाषण भी सुनना चाहिए.
आश्चर्य है कि वे भी उसी ‘बहुलता’ की बात कर रहे हैं. कह रहे हैं कि ‘भारत की सफलता का मंत्र उसकी विविधता है, और यह विविधता ही हमारा वह आधार है, जो हमें अद्वितीय बनाता है.’ जाहिर है, प्रथम नागरिक के पद की ऊंचाई तक पहुंचने वाले लोग तो इस राष्ट्र की आत्मा को पहचान रहे हैं, पर असहमति का उपचार हिंसा से करने वाले इस महान राष्ट्र की नागरिकता का दर्जा पाने लायक परिपक्वता अभी हासिल नहीं कर पाए हैं.
| Tweet |