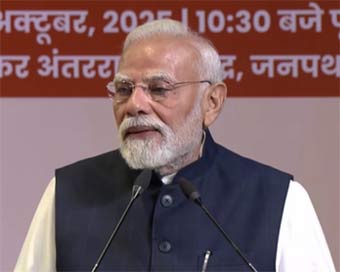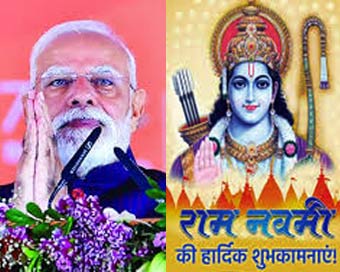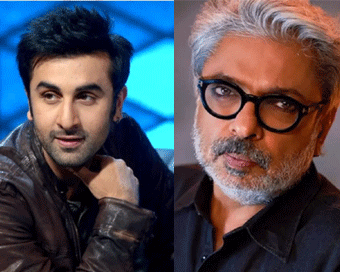निजता : एकल व्यवस्था की अपेक्षा
सरकार द्वारा अपने नागरिकों के बारे में उनकी व्यक्तिगत सूचनाओं को सहेजने का स्तर और मात्रा अपरिमित हैं.
 निजता : एकल व्यवस्था की अपेक्षा |
मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि वह डीएनए प्रोफाइलिंग बिल पेश करने वाली है. सरकार के प्रभावी कामकाज और सामाजिक कल्याण योजनाओं के कारगर कार्यान्वयन के लिए जहां संवेदनशील व्यक्तिगत सूचनाओं को सहेजना और उनका इस्तेमाल जरूरी है, वहीं सभी सरकारी एजेंसियों का भी दायित्व है कि निजता के अधिकार का उल्लंघन न होने पाए. इतनी बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत सूचनाएं एकत्रित करने से पूर्व हमारे लिए सूचनाओं के संरक्षण संबंधी कानून बनाया जाना आवश्यक है.
सूचना प्राप्त करने की आजादी में किसी की निजता संबंधी चिंता भी निहित है यानी सूचना का अधिकार कानून में व्यक्तिगत सूचना न बताने से छूट है. सूचना और संपर्क के हासिल में मानवाधिकार को प्रोत्साहन, बुनियादी स्वतंत्रताओं और मानवीय गरिमा भी शामिल हैं. जब निजता के रूप में मौजूद गरिमा का हनन होता है, और सूचना जबरिया या गुपचुप तरीके से हासिल की जाती है, तो वैयक्तिक निजता पर हमला है. कहने का तात्पर्य यह कि किसी के आशियाने को अलंघनीय माना जाए या जैसा कि एडर्वड कोक काफी पहले कह चुके हैं, ‘किसी का घर उसका महल होता है.’
आधार को अनिवार्य बनाने की संवैधानिकता पर सुनवाई में विलंब का मानवाधिकार के पैरवीकारों में अच्छा संकेत नहीं गया है. पूर्व एटॉर्नी जनरल और केके वेणुगोपाल, देश की बार के नवनियुक्त नेता, द्वारा व्यक्त विचारों से मानवाधिकारों के अलम्बरदारों को झटका लगा है. क्या निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वंत्रता के अधिकार में निहित किया जाए? इस मुद्दे पर अब नौ जजों की पीठ सुनवाई कर रही है. बीते जून माह में शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए निराशाजनक आदेश के आलोक में मानवाधिकार कार्यकर्ता नौ न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए जाने वाले फैसले को लेकर चिंतित हैं. जब कभी लोकतांत्रिक सरकार ने अपनी शक्तियों से बाहर जाकर संविधान में संशोधन करने का प्रयास किया तो सुप्रीम कोर्ट ने नागरिक अधिकारों के संरक्षक और गारंटर के रूप में मजबूती से उस सरकार को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग से रोका. जहां तक निजता के अधिकार का प्रश्न है, तो यह अनुसुलझा मुद्दा नहीं है.
निजता के अधिकार का पहला मामला सतीश चंद्रा (1954) का था जिसमें तलाशी और जब्ती संबंधी सरकार के अधिकार पर सवाल था. अदालत ने निजता के अधिकार संबंधी विशेष प्रावधानों के मामले में अमेरिकी संविधान के चौथे संशोधन सरीखे प्रावधान की भारतीय संविधान में कमी की ओर इंगित किया. उसने स्पष्ट कहा, ‘हम भारत में निजता का अधिकार आयात नहीं कर सकते.’ तदोपरांत खड़क सिंह (1963) का मामला आया. इस मामले डकैती और हिंसा के अभियुक्त को रिहा किया गया था, लेकिन उस पर निगरानी रखी जा रही थी.
गांव का चौकीदार और पुलिस के सिपाही रात में चिल्लाते हुए उसका दरवाजा खटखटा कर उसे जगा देते थे. उससे उसकी नींद में खलल होता था. उसे कई बार थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जाना पड़ता था. ऐसे में उप्र पुलिस नियमन के अध्याय 20 को चुनौती दी गई. अपील-दलील सुनने के पश्चात छह जजों ने फैसला सुनाया कि ‘प्रत्येक व्यक्ति का घर उसका अपना महल होता है’ लेकिन कहा कि भारत में निजता का अधिकार बुनियादी अधिकार नहीं है. उसके बाद जस्टिस सुब्बा राव का फैसला आया जिसमें कहा गया कि बेशक, निजता के अधिकार का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, तो भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है. फिर गोबिंद (1975) मामले में खड़क सिंह मामले में व्यक्त की गई अल्पसंख्यक राय ने बहुमत की राय की शक्ल अख्तियार कर ली. जस्टिस मैथ्यू, जस्टिस कृष्णा अय्यर और जस्टिस गोस्वामी ने इस विचार को स्वीकार किया कि भारत में निजता का अधिकार है.
तदोपरांत मलक सिंह (1981) मामले में अदालत एक कदम और बढ़ी. इस फैसले में अदालत ने कहा कि निगरानी अनुच्छेद 21 तथा 19(1)(डी) के तहत प्रदत्त निजता के अधिकार का अतिक्रमण करती है. निजता के अधिकार की स्वीकार्यता का उस समय और भी विस्तार हुआ जब अदालत ने एक फैसले में कहा कि महिलाओं की अपनी निजता होती है, और किसी को उनकी निजता को भंग करने का अधिकार नहीं है. नीरा (1992) मामले में जब भारतीय जीवन बीमा निगम की एक परिवीक्षा अधिकारी ने चिकित्सा जांच के दौरान पिछली माहवारी के बारे में जानकारी दी तो अदालत ने माहवारी चक्र की नियमितता आदि संबंधी अनुच्छेदों को निजता के अधिकार का उल्लंघन करार देते हुए आदेश दिया कि ऐसे कॉलम को तत्काल हटाया जाए.
राजा गोपाल (1995) मामले में शीर्ष अदालत ने कहा कि मौत की सजा पाए व्यक्ति को भी निजता का अधिकार मिला है. टेलीफोन टेप करने को भी अदालत ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करने वाला बल्कि अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ भी बताया. हिंसा विरोधक संघ (2008) मामले में व्यवस्था दी कि शाकाहार या मांसाहार का मामला भी निजता के अधिकार में निहित है. 2016 में तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीफ खाने को प्रतिबंधित करने वाले कानूनी प्रावधान को भी खारिज कर दिया था. यह कहते हुए कि कट्टीघर पर प्रतिबंध नहीं है, तो खाने पर क्यों. आइए, उम्मीद करें कि नौ जजों की पीठ ठोस कानूनी व्याख्यों के आधार पर व्यवस्था देगी.
(लेखक नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद के उपकुलपति हैं. लेख में व्यक्त विचार निजी हैं)
| Tweet |