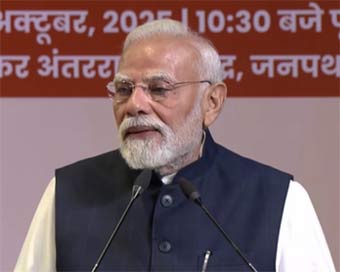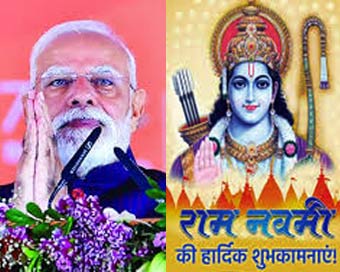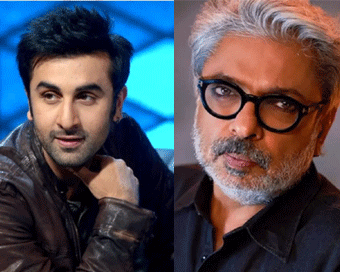बाढ़ : बर्बाद होती असम की आर्थिकी
यह तो मॉनसून की शुरुआत ही है और असम के कई जिलों में आई बाढ़ से 95 हजार से अधिक लोग प्रभावित हैं.
 बाढ़ : बर्बाद होती असम की आर्थिकी |
बुरी तरह पीड़ित दारंग जिले में लगभग 37 हजार लोग बाढ़ की चपेट में हैं. कई इलाकों में कटान से समस्याएं बढ़ी हैं. पूर्वोत्तर के असम राज्य के 14 जिले आने वाले तीन महीने पूरी तरह बाढ़ की चपेट में रहेंगे और कमोबेश यही स्थिति वहां हर साल होती रहती है. हर साल नदियों में आने वाली बाढ़ की विभीषिका की वजह से राज्य का लगभग 40 फीसद हिस्सा पस्त-सा रहता है.
एक अनुमान के अनुसार इससे हर साल जान-माल की लगभग 200 करोड़ रु पये की क्षति होती है. राज्य में एक साल के नुकसान के बाद सिर्फ मूलभूत सुविधाएं खड़ी करने में ही दस साल से ज्यादा का समय लग जाता है जबकि नुकसान का सिलसिला हर साल जारी रहता है. केंद्र और राज्य की सरकारें बाढ़ के बाद मुआवजा बांटने में तत्परता दिखाती है. यह दुखद ही है कि आजादी के लगभग 70 साल बाद भी हम राज्य के लिए बाढ़ नियंत्रण की कोई मुकम्मल योजना नहीं दे पाए हैं. यदि इस अवधि में राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान व बांटी गई राहत राशि को जोड़ें तो पाएंगे कि इतनी धनराशि में एक नया और सुरक्षित असम खड़ा किया जा सकता था.
नीतियां ऐसी बनें कि बाढ़ और असम में हर साल तबाही मचाने वाली ब्रह्मपुत्र और बराक नदियां और उनकी लगभग 48 सहायक नदियां और उनसे जुड़ी असंख्य सरिताओं पर सिंचाई व बिजली उत्पादन परियोजनाओं के अलावा इनके जल प्रवाह को आबादी में घुसने से रोकने की योजनाएं बने. जिसकी मांग लंबे समय से उठती रही है. असम की अर्थव्यवस्था का मूलाधार खेती-किसानी ही है, और बाढ़ का पानी हर साल लाखों हेक्टेयर में खड़ी फसल को नष्ट कर देता है. ऐसे में यहां का किसान कभी भी कर्ज से उबर ही नहीं पाता है.
एक बात और यह कि ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह का अनुमान लगाना भी बेहद कठिन है. इसकी धारा लगातार और तेजी से बदलती रहती है. परिणामस्वरूप भूमि का कटाव, उपजाऊ जमीन के क्षरण से नुकसान बड़े पैमाने पर होता रहता है. यह क्षेत्र भूकंपग्रस्त है और यहां हल्के-फुल्के झटके अक्सर महसूस किए जाते हैं. भूकंप की वजह से जमीन खिसकने की घटनाएं भी यहां की खेती-किसानी को प्रभावित करती है. इस क्षेत्र की मुख्य फसलें धान, जूट, सरसो, दालें व गन्ना हैं. धान व जूट की खेती का समय ठीक बाढ़ के दिनों का ही होता है. यहां धान की खेती का 92 प्रतिशत आहू, साली बाओ और बोडो किस्म की धान का है और इनका बड़ा हिस्सा हर साल बाढ़ में धुल जाता है. असम में मई से लेकर सितम्बर तक बाढ़ रहती है और इसकी चपेट में तीन से पांच लाख हेक्टेयर खेत आते हैं. हालांकि, खेती के तरीकों में बदलाव और जंगलों का बेतरतीब दोहन जैसी मानव-निर्मिंत दुर्घटनाओं ने जमीन के नुकसान के खतरे का दोगुना कर दिया है. दुनिया में नदियों पर बने सबसे बड़े द्वीप माजुली पर नदी के बहाव के कारण जमीन कटान का सबसे अधिक असर पड़ा है. बाढ़ का असर यहां के वनों व वन्य जीवों पर भी पड़ता है. हर साल कांजीरंगा व अन्य संरक्षित वनों में गैंडा जैसे संरक्षित जानवर भी मारे जाते हैं. वहीं दूसरी ओर, इससे पेड़-पौधों को बड़े पैमाने पर नुकसान होता है. राज्य में नदी पर बनाए गए अधिकांश तटबंध व बांध 60 के दशक में बनाए गए थे.
अब वे बढ़ते पानी को रोक पाने में असमर्थ हैं. उनमें गाद भी जमा हो गई है, जिसकी नियमित सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है. पिछले साल पहली बारिश के दबाव में 50 से अधिक स्थानों पर ये बांध टूटे थे. इस साल पहले ही महीने में 27 जगहों पर मेड़ टूटने से जलनिधि के गांव में फैलने की खबर है. ब्रह्मपुत्र घाटी में तट-कटाव और बाढ़ प्रबंध के उपायों की योजना बनाने और उसे लागू करने के लिए दिसम्बर 1981 में ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थापना की गई थी. बोर्ड ने ब्रह्मपुत्र व बराक की सहायक नदियों से संबंधित योजना कई साल पहले तैयार भी कर ली थी. केंद्र सरकार के अधीन एक बाढ़ नियंत्रण महकमा कई सालों से काम कर रहा है और उसके रिकार्ड में ब्रह्मपुत्र घाटी देश के सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में से हैं. इन महकमों ने इस दिशा में अभी तक क्या कुछ किया? असम को सालाना बाढ़ के प्रकोप से बचाने के लिए ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियों की गाद सफाई, पुराने बांध व तटबंधों की सफाई, नये बांधों का निर्माण जरूरी है. लेकिन सियासी खींचतान के चलते जहां जनता ब्रह्मपुत्र के कहर को अपनी नियति मान बैठी है, वहीं नेता एक-दूसरे पर आरोप मंढ़ रहे हैं.
| Tweet |