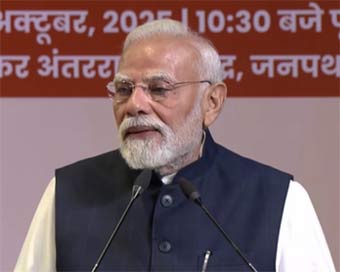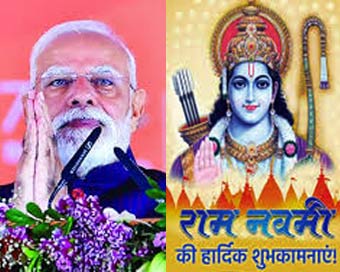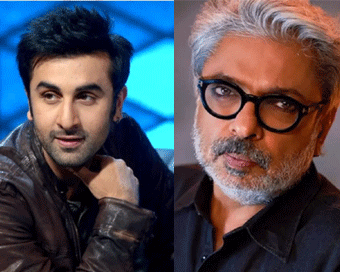प्रसंगवश : हिंदी पट्टी में हिंदी की चिंता
हिंदी को हाशिये से उठा कर मुख्य धारा के लायक बनाये रखने की सरकारी कवायद बदस्तूर है. उसकी व्यवस्था पुख्ता बनी हुई है.
 प्रसंगवश : हिंदी पट्टी में हिंदी की चिंता |
राजभाषा विभाग, संसदीय राजभाषा समिति, केन्द्रीय हिंदी निदेशालय, तकनीकी शब्दावली आयोग, केन्द्रीय हिंदी संस्थान निदेशालय तथा अनुवाद ब्यूरो जैसी संस्थाएं और हिंदी अधिकारियों का उनका अमला चार-पांच दशकों से हिंदी के संवर्धन की दिशा में निरंतर कार्यरत है. व्यवस्था के मुताबिक़ उनकी अधिकांश शक्ति मूल अंग्रेजी सूचनाओं और निर्देशों के अनुवाद में खप जाती है और शेष बची-खुची शक्ति हिंदी विकास की जानकारी देने वाली भारी-भरकम प्रश्नावली को पूरा करने में व्यय होती है.
ये सभी संस्थाएं और उनके प्रयास सरकारी तंत्र की व्यवस्था के अनुरूप हिंदी के प्रचार-प्रसार को लेकर अपने दायित्वों का निर्वाह कर रही हैं. पर यदि थोड़े-बहुत अपवादों को छोड़ दिया जाय तो सरकारी काम-काज में हिंदी के उपयोग को लेकर यथास्थिति-सी ही बनी प्रतीत होती है. बदलाव कम आया है. अपने बूते राजभाषा का अमली जामा पहनने के लिए हिंदी काबिल नहीं हो पाई है. अंग्रेजी की ठसक पूर्ववत है. शायद कुछ और करने की जरूरत भी है. पर यहां प्रश्न यह भी उठता है कि हिंदी समाज स्वयं हिंदी को कितनी गंभीरता से लेता है ? भाषा को लेकर उसकी क्या मनस्थिति है?
इस बात से शायद ही किसी को गुरेज हो कि भाषा समाज की संपत्ति होती है और भाषा का व्यवहार कैसे, कितना और किस प्रयोजन के लिए किया जाय, यह अंततोगत्वा एक सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दा है और ऐसा होना भी चाहिए. मीडिया और मनोरंजन की दुनिया में हिंदी की सफलता को लेकर हिंदी वाले मन में खुश हो लेते हैं पर भाषा की शक्ति को ज्ञान-विज्ञान और विचार-विमर्श की भाषा के रूप में प्रयोग की स्थिति को लेकर जब विचार करते हैं तो असंतोषजनक स्थिति ही नजर आती है. हिंदी भाषा की ऐसी स्थिति के लिए अधिक भयावह बात यह है हिंदी भाषी समाज कदाचित स्वयं हिंदी के प्रति उदासीन है. वह इसके लिए किसी प्रकार का उत्साह तो नहीं ही दिखा रहा है, अब तो नकारात्मक दृष्टि रखने लगा है.
हिंदी पट्टी अर्थात सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र कभी ‘बीमारू’ नाम से जाना जाता था. आज के जमाने में आगे बढ़ने के लिए शैक्षिक योग्यता हेतु शिक्षा की सुविधाएं भी कम हैं और जो हैं, उनका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है. यह स्थिति किस क़दर बिगड़ रही है, इसका अंदाज़ा हिंदी विषय में उत्तर प्रदेश के बोर्ड की परीक्षा का ताजा परिणाम है. जिसमें बड़ी संख्या में छात्र असफल हुए हैं, जिनकी हिंदी मातृभाषा है. अत: अनुमान किया जाता है कि हिंदी का उपयोग और अभ्यास करने के अवसर उन्हें अधिक मिलता रहा होगा. पर उनका भाषा-परिवेश जरूर समृद्ध न रहा होगा. यदि भाषा-प्रयोग की मूल योग्यता उनमें नहीं आ पाएगी तो यह उनके भविष्य को बाधित-कुंठित करने वाली बात है.
भाषा पर अच्छा अधिकार होने पर अभिव्यक्ति प्रभावपूर्ण हो जाती है, संचार शक्तिशाली हो उठता है और व्यक्ति स्वयं को प्रमाणित कर पाता है. हिंदी माध्यम के छात्रों के साक्षात्कार में ऐसा अनुभव मिलता है कि इन प्रत्याशियों का सम्प्रेषण दुर्बल है. ऐसा मान लिया लिया जाता है कि हिंदी सीखने की जरूरत नहीं है. अंग्रेजी सीखने की दूकानें खूब चलती हैं.
चूंकि भाषा का प्रयोग तरह-तरह के औपचारिक और अनौपचारिक अवसरों और सन्दर्भों में होता है उसका अध्ययन और भाषा के उपयोग की योग्यता सिर्फ कक्षा में होने वाले अध्ययन तक ही सीमित नहीं होता. उसका वातावरण व्यापक सामाजिक परिवेश में रचता-बनता है. मीडिया में बहस, साक्षात्कार, सीरियल, फिल्म, टीवी और रेडियो पर समाचार आदि सबमें भाषा का जीता-जागता प्रयोग मिलता है और उन लोगों का ज्यादा प्रभाव पड़ता है जो जीवन में सफल है और ‘सेलिबट्री’ की औकात रखते हैं.
उनकी प्रतिष्ठा उनके भाषा-प्रयोग और आचरण पर मुहर लगाती है. ये नेता, अभिनेता और अधिकारी जिस तरह की भाषा, लहजा, हाव-भाव का उपयोग करते हैं, वह सब अनजाने ही भाषा-प्रयोग के मानकों का भी निर्माण करता चलता है और लोगों के मन पर अचेतन रूप से छाने लगते हैं. हिंदी सीखने-सिखाने को लेकर सामाजिक स्तर पर कोई सजग प्रयास नहीं दिखता. विद्यालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग और हिंदी शिक्षण के प्रति कोई आदर भाव नहीं होता है. जब तक यह मनोभाव नहीं बदलेगा, हिंदी ठहरी रहेगी.
| Tweet |