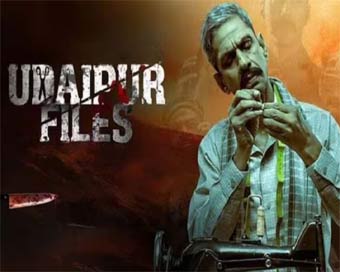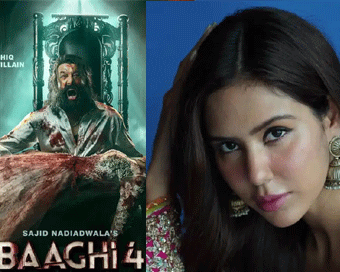कम्युनिस्ट डेमोक्रेट होने में शरम कैसी!
भारत के समाजवाद की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह गांधी जी की छाया में विकसित हुआ.
 राजकिशोर (फाइल फोटो) |
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पहले कांग्रेस में ही थी और गांधी जी के उसूलों में उसकी श्रद्धा थी. यही वजह है कि समाजवादी नेता डॉ. राममनोहर लोहिया ने सोशलिस्टों की पहली सरकार से, जो केरल में बनी थी, इस्तीफा मांगने में एक क्षण का भी विलंब नहीं किया, जब उसने निहत्थे नागरिकों पर गोली चलाई. भारत में साम्यवाद की धारा ज्यादा मजबूत रही है, पर उसका अंत सिंगुर और नंदीग्राम में हुआ, जहां पार्टी और सरकार दोनों ने हिंसा की. यह एक ऐसे रास्ते पर चलने से ही संभव हुआ, जिसका लक्ष्य क्रांति न हो कर सत्ता सुख भोगना था.
डॉ. राममनोहर लोहिया द्वारा समाजवाद की नूतन व्याख्या करने के पहले भारत का समाजवाद मार्क्सवाद का ही एक संस्करण था. आचार्य नरेन्द्र देव और जयप्रकाश नारायण, दोनों को समाजवादी माना जाता है, वास्तव में ये थे मार्क्सवादी, जो वर्ग संघर्ष की अवधारणा से आगे न जा सके. डॉ. लोहिया ने मार्क्सवाद में अहिंसा, लोकतंत्र, विकेंद्रीकरण और मानव अधिकार जोड़ा नहीं, बल्कि एक ऐसी विचारधारा विकसित की, जिसमें ये चीजें सहज और स्वाभाविक जान पड़ती हैं. भारतीय समाजवाद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह अंग्रेजी के विध्वंसक आभिजात्य से मुक्त रहकर जमीन से जुड़ा रहा. यही कारण है कि जाति की असलियत और स्त्री की हीन स्थिति को पहचानने का एकमात्र श्रेय उसे ही है.
जो लोग आरोप लगाते हैं कि डॉ. लोहिया की राजनीति में जातिवाद के बीज छिपे हुए थे, वे न लोहिया को जानते हैं, न जातिवाद को. उनके पहले सिर्फ डॉ. अम्बेडकर थे, जिन्होंने जाति प्रथा को समाप्त करने की बात की थी. लेकिन वे सिर्फ दलितों की ओर से बोल रहे थे. लोहिया का योगदान यह है कि उन्होंने इसमें पिछड़ी जातियों, स्त्रियों, मुसलमानों और आदिवासियों को जोड़ा. साठ प्रतिशत आरक्षण का विचार उन्हीं का दिया हुआ है, लेकिन उनकी विचारधारा में केंद्रीय स्थान एक ऐसे समाज का था, जिसमें किसी को आरक्षण की जरूरत ही न पड़े. अगर लोहिया की सिर्फ एक ही बात-अंग्रेजी हटाओ-मान ली जाती, तो आज देश का वातावरण कुछ और ही होता. हमारे यहां सत्ता का चरित्र कुछ ऐसा है कि एक समय में \'हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान\' का प्रतीक भारतीय जनता पार्टी ने भी हिंदी को छोड़ दिया है.
डॉ. राममनोहर लोहिया ने समाजवाद को दो शब्दों से परिभाषित किया था-समता और समृद्धि. न गरीबी रहे, न विषमता. यह कविता नहीं है, ठोस गद्य है. यह सच है कि भारत में विषमता दूर किए बिना गरीबी को विदा नहीं किया जा सकता. चूंकि विषमता की संस्कृति को प्रोत्साहन है, इसलिए गरीबी भी अंगद के पांव की तरह अटल है. इससे बचने के लिए लोहिया का मंत्र यह है कि भारत का आर्थिक विकास लघु और कुटीर उद्योग-धंधों से ही संभव है. पश्चिम में भारी पूंजी की अर्थव्यवस्था एक विशेष ऐतिहासिक परिस्थिति में बनी है, जिसे पाना भारत के लिए संभव नहीं है और संभव हो भी, तो वांछनीय नहीं है, क्योंकि भारी पूंजी और उपभोक्तावाद ने मिल कर जिस संस्कृति की रचना की है, वह व्यक्तिपरकता, विघटन, क्षणवाद, अपराध, आत्महत्या, स्त्री के अवमूल्यन और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से लबालब भरी हुई है. पर्यावरण का विनाश इस सबका बाई-प्रोडक्ट है.
यह अकारण नहीं है कि पश्चिमी मुल्कों में ग्रीन आंदोलन मजबूत हो रहा है. वाल स्ट्रीट पर कब्जे का स्वप्न है. स्त्रियां एक नई संस्कृति की मांग कर रही हैं, जो शोषण से मुक्त और अहिंसा पर आधारित हो. समाजवाद फिर एक संभावना बन रहा है, जिसकी एक झलक अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में बर्नी सैंडर्स की गरजती हुई आवाज में दिखाई दी थी. इसके साथ इस तथ्य को जोड़ दें कि जो कल तक वैीकरण के प्रबल समर्थक थे, वे ही आज उसका विरोध कर रहे हैं, तो तस्वीर मुकम्मल हो जाती है.
इस संदर्भ में लोहिया की \'सप्त क्रांति\' की अवधारणा बहुत ही प्रासंगिक है. उन्होंने इन सात क्रांतियों का आह्वान किया था-1. नर-नारी की समानता के लिए, 2. चमड़ी के रंग पर रची राजकीय, आर्थिक और दिमागी असमानता के विरुद्ध, 3. संस्कारगत, जन्मजात जाति प्रथा के खिलाफ और पिछड़ों को विशेष अवसर के लिए, 4. परदेसी गुलामी के खिलाफ और स्वतंत्रता तथा वि लोक-राज के लिए, 5. निजी पूंजी की विषमताओं के खिलाफ और आर्थिक समानता के लिए तथा योजना द्वारा पैदावार बढ़ाने के लिए, 6. निजी जीवन में अन्यायी हस्तक्षेप के खिलाफ और लोकतांत्रिक पद्धति के लिए, और 7. अस्त्र-शस्त्र के खिलाफ और सत्याग्रह के लिए. लोहिया कहते हैं, \'मोटे तौर से ये हैं सात क्रांतियां. सातों क्रांतियां संसार में एक साथ चल रही हैं.
अपने देश में भी उनको एक साथ चलाने की कोशिश करनी चाहिए. जितने लोगों को भी क्रांति पकड़ में आई हो उसके पीछे पड़ जाना चाहिए और बढ़ाना चाहिए. बढ़ाते-बढ़ाते शायद ऐसा संयोग हो जाए कि आज का इंसान सब नाइंसाफियों के खिलाफ लड़ता-जूझता ऐसे समाज और ऐसी दुनिया को बना पाए जिसमें आंतरिक शांति और बाहरी या भौतिक भरा-पूरा समाज बन पाए.\' क्या इस उम्मीद को हम कभी छोड़ सकते हैं? या, इसके लिए काम करना कभी स्थगित किया जा सकता है?
| Tweet |