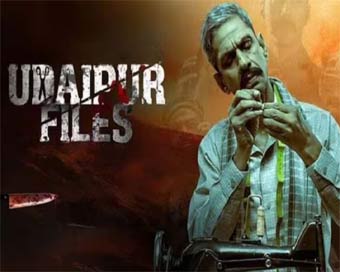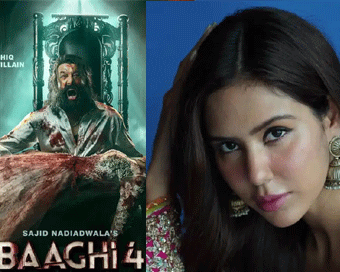तीन तलाक : अदालत और सरकार
करीब एक साल से चल रही तीन तलाक पर कानूनी पाबंदी की मुहिम में कई महत्त्वपूर्ण पड़ाव आए हैं.
 तीन तलाक : अदालत और सरकार |
सर्वोच्च न्यायालय में बृहस्पतिवार को हुई गतिविधियां ऐसा ही महत्त्व रखतीं हैं. इस लेख काल में हुई कार्रवाई के कुछ पहलुओं का जायजा लेने की कोशिश करते हैं. वैसे तो तीन तलाक के मुद्दे का राजनीतिकरण करने की भरपूर साजिश चल रही है, जिसमें राजकीय पक्ष, रूढ़िवादी इदारे और कुछ अवसरवादी नेता शामिल हैं.
कई स्थापित हितों को इसमें अपना उल्लू सीधा करने का अवसर दिख रहा है. लेकिन असल में बात जेंडर जस्टिस और स्त्री समानता की है, न कि स्थापित हितों के बढ़ावे की. खुशी की बात है कि यह साजिशें नाकामयाब होती नजर आ रही हैं. सर्वोच्च न्यायालय से निष्पक्ष एवं सटीक तरीके से न्याय की सबको उम्मीद है. इस मुहिम को यहां तक पहुंचाने का श्रेय पूरी तरह से साधारण मुस्लिम स्त्रियों को जाता है. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा की वे सिर्फ तीन तलाक पर कानूनी पाबंदी की तहकीकात करेगा सामान नागरिक संहिता की नहीं. यह पूरी तरह से सटीक है; क्योंकि तीन तलाक और समान नागरिक संहिता दो अतिमहत्त्वपूर्ण किंतु अलग अलग मुद्दे हैं.
सामान नागरिक संहिता पर तमाम भारतीय समाज को यानी कि सभी नागरिकों को गौर करना होगा. जबकि तीन तलाक, निकाह हलाला और बहुपत्नीत्व मुस्लिम महिला नागरिक के मानव अधिकार एवं धार्मिंक अधिकार से जुड़े मुद्दे हैं. इन कुप्रथाओं की इजाजत न धर्म में है, न ही संविधान में. और फिर कानून बनाने का काम संसद का है न कि कोर्ट का. इन दोनों मुद्दों को जोड़कर राजनीति करने की कोशिशें चल रही हैं. ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्टीकरण एक अहम कदम है. यही वजह है कि आम मुस्लिम औरतों ने इसका भरपूर स्वागत किया है.
यहां दोहराना जरूरी है कि इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान में तीन तलाक का जिक्र नहीं है. लेकिन पितृसत्ता के चलते भारतीय समाज में यह कुरीति प्रचलित है. फिर संविधान के आर्टकिल 14 और 15 के तहत किसी भी नागरिक से लिंग आधारित भेदभाव और असमानता अवैध है. आर्टकिल 25 जो कि धर्म स्वतंत्र के अधिकार के बारे में है, वहां भी धर्म स्वंत्रता का अधिकार महिला और पुरुष दोनों ही नागरिक के व्यक्तिगत अधिकार की बात है. साथ ही यहां ये ही लागू है कि यह अधिकार के अंतर्गत जन व्यवस्था एवं नैतिकता को हानि नहीं पहुंचाई जा सकती. सरल भाषा में कहें तो धर्म की आड़ में किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन अवैध है.
साथ ही तीन तलाक जैसी कुरीति एसेंसियल प्रैक्टिस या बुनियादी उसूल की परिभाषा में नहीं आतीं. अगर ऐसा होता तो फिर हमारे देश में शिया समुदाय में तीन तलाक को अवैध नहीं माना जाता. बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सामने वैधता जांचने कि गुजारिश के साथ चार प्रश्न रखे. केंद्र ने निवेदन किया कि सर्वोच्च न्यायालय तीन तलाक, निकाह हलाला एवं बहुपत्नीत्व की संविधानिक वैधता इस नजरिये से आंके. पहला सवाल यह कि, क्या इन रीतियों को संविधान के आर्टकिल 251 के तहत वैधता दी जा सकती है? क्या आर्टकिल 25 का संबंध आर्टकिल 14 एवं 21 से नहीं है? क्या पसर्नल लॉ या पारिवारिक कानून को आर्टकिल 13 के चलते कानून माना जा सकता है?
क्या ये रीतियां भारत के संयुक्त राष्ट्र इत्यादि अन्य अंतरराष्ट्रीय दायित्व के चलते लागू रह सकतीं हैं? यह चारों ही गहरे सवाल हैं और इनका औचित्य जांचना जरूरी है. यह काम सर्वोच्च न्यायालय पांच जज की संवैधानिक बेंच बनाकर करेगा. इसका नतीजा जरूर ऐतिहासिक होगा और सामाजिक बदलाव के लिए सकारात्मक भी. धार्मिंक और संवैधानिक सिद्धांत दोनों ही पूरी तरेह से स्पष्ट हैं. लेकिन पितृसत्ता और राजनीति की मिलीभगत के चलते 1947 से अब तक इस पूरे मामले को पेचीदा बनाने की या दबा देने की पूरी कोशिश की गई है. मगर आज हवा का रु ख बदल चुका है. आम मुस्लिम महिलाओं ने सर्वोच्च न्यायालय में इंसाफ की गुहार लगाकर पुरुष प्रधानता पर सीधे रूप से प्रहार कर दिया है.
केंद्र में बीजेपी की सरकार होने का डर जताकर आम लोगों को गुमराह करने का प्रयास हो रहा है. पांच राज्यों में चुनाव के चलते इस मुद्दे पर राजनीति गरमाई हुई है. लेकिन हकीकत यह है कि जेंडर जस्टिस सरकार का संवैधानिक दायित्व है और यदि सरकार इससे पीछे हटती तो वह सरकार की भारी विफलता होती. देश भर की महिलाएं, फिर वे हिन्दू हो चाहे मुस्लिम; इस विफलता को कभी माफ नहीं करती. साथ ही, लोकतंत्र और लिंग समानता में विश्वास करने वाला हर भारतीय नागरिक भी नाखुश होता. मौजूदा सरकार की अन्य क्षेत्रों में कमियों एवं त्रुटियों का ताल्लुक इस मामले से नहीं है. इस कसौटी पर सरकार खरी उतरी है. कुछ महीने पहले सरकार ने जो हलफनामा दायर किया था वे भी मुस्लिम महिलाओं के इस संघर्ष की ताईद में था.
हमारे देश में आज भी पुरुष प्रधान सोच के चलते महिलाओं का उत्पीड़न आम है. लेकिन पर्सनल लॉ या पारिवारिक कानून के मामले में हिन्दू एवं ख्रिस्ती धर्म मानने वाली महिलाओं को कानूनी सुरक्षा मिली हुई है. पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे रूढ़िवादी मुस्लिम गुटों के वर्चस्व के चलते मुस्लिम महिलाओं को अपनी अन्य बहनों की तरह कानूनी विकल्प नहीं मिल पाया है. यही वजह है कि आज भी तीन तलाक, निकाह हलाला एवं बहुपत्नीत्व जैसी कुप्रथाएं लागू हैं. इसको खत्म करना जरूरी है. साथ ही मुस्लिम पारिवारिक कानून में व्यापक सुधार की जरूरत है. तीन तलाक पर पाबंदी इस सुधार की दिशा में एक तरह से पहला कदम है. चुने हुए लोक प्रतिनिधि, संसद, न्यायालय, मीडिया एवं अन्य सारे ही लोकतांत्रिक संस्थानों को इस मुहिम में अपनी भूमिका निभानी होगी. इसी उम्मीद के साथ आम मुस्लिम महिलाओं ने सर्वोच्च न्यायालय में इंसाफ की गुहार लगाई है.
(जकिया सोमन भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की सह संस्थापक हैं और सर्वोच्च न्यायलय में तीन तलाक मामले में याचिकाकर्ता हैं)
| Tweet |