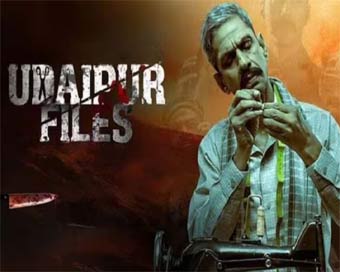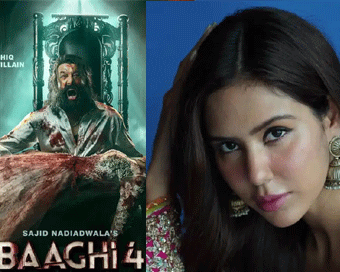कृषि-कर्ज : कैसे उबरेंगे किसान?
सर्वोच्च न्यायालय ने किसानों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों पर एक बड़ा आदेश दिया.
 कृषि-कर्ज : कैसे उबरेंगे किसान? |
कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ शासित प्रदेश और आरबीआई को किसानों की खुदकुशी की वजह जानने के निर्देश दिए. प्रधान चीफ जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस एनवी रमन की बैंच ने चार हफ्तों में जवाब मांगा है. गैर सरकारी संगठन सिटीजंस रिसोर्सेज एंड एक्शन एंड इनीशिएटिव (क्रांटि) की याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने टिप्पणी की कि यह देशभर के किसानों से जुड़े व्यापक जनहित का बहुत ही ‘संवेदनशील मामला’ है.
कोर्ट ने पूछा है कि फसल की बर्बादी, कर्ज और प्राकृतिक आपदा से किसानों की रक्षा करने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारें एक समग्र नीति क्यों नहीं ला रहीं? एनजीओ ने पहले गुजरात हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी. उसे हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि वह नीतिगत मामलों में दखल नहीं दे सकता. इसके बाद क्रांटि ने सुप्रीम कोर्ट का रु ख किया. सुप्रीम कोर्ट ने अब इसका दायरा गुजरात से बढ़ाकर पूरे देश के किसानों के लिए कर दिया है.
गौरतलब है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ताजा रिपोर्ट मुताबिक, किसानों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ी है. साल 2014 में 5650 किसानों ने मौत को गले लगाया था, जबकि ताजा आंकड़ों में यह संख्या बढ़कर 8007 हो गई है. यह 2014 में किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं से 42 प्रतिशत अधिक हैं. चिंता इसलिए बढ़ जाती है कि आंकड़े घटने के बजाय निरंतर बढ़ रहे हैं. रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई कि आत्महत्या करने वाले किसानों की लगभग 72 फीसदी तादाद छोटे व गरीब किसानों की रही जिनके पास दो हेक्टेयर से भी कम जमीन थी.
आंकड़े इस ओर भी इशारा करते हैं कि आत्महत्या करने वाले किसानों का लगभग 80 फीसदी हिस्सा बैंक कर्ज के बोझ से दबा था, न कि महाजनों के कर्ज से. ऐसे में कृषि आर्थिकी और ग्रामीण सामाजिकता की जटिलताओं के साथ उनकी विडंबनाओं पर बहुत ईमानदारी के साथ पारदर्शी ढंग से सोचने और कार्ययोजनाएं बनाने की जरूरत है, ताकि किसान आत्महत्याओं को न्यूनतम किया जा सके. भले ही हम दावा करें कि हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में आने वाला है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग खेती-किसानी का काम कर्ज की मदद से ही कर रहे हैं. किसानों के लिए खेती जीवन-मरण का प्रश्न है. इसके बावजूद सरकार को जितना कृषि पर ध्यान देना चाहिए उतना नहीं दिया गया.
हालत यह है कि किसानों को उनकी लागत ही नहीं मिलती. ज्यादातर किसानों की आय राष्ट्रीय औसत से कम है. उपज का सही मूल्य मिल पाता और न ही कृषि को लेकर मौजूदा सरकारी नीतियों से उन्हें लाभ पहुंचता है. वे कम उत्पादन करने पर भी मरते हैं, और अधिक उत्पादन करने पर भी. अक्सर मानसून को दोष देकर हम अपनी कमियां छुपाते रहे हैं.
हालांकि भाजपा के चुनाव घोषणा-पत्र में और खुद नरेन्द्र मोदी ने वादा किया था कि भाजपा की सरकार किसानों के ‘अच्छे दिन’ लाएगी और किसानों की आत्महत्याएं खत्म कराएगी. लेकिन बीते 30 माह में अब तक किसानों व खेतीबाड़ी के लिए हुआ क्या..इससे हम सभी वाकिब हैं.
खैर, हमारे यहां राजनीतिक पार्टयिों को अपने इन ‘अन्नदाताओं’ की याद तभी आती है, जब चुनाव सिर पर आते हैं, क्योंकि देश का सबसे बड़ा वोट बैंक भी यही हैं. लेकिन सत्ता की चाभी हाथों तक पहुंचते ही देश की इस सबसे बड़ी साधनहीन आबादी को उसकी तकदीर पर छोड़ दिया जाता है. जाहिर है, घटती आमदनी के चलते किसान निराश हैं. एक अध्ययन के अनुसार 40 प्रतिशत किसान विकल्पहीनता की स्थिति में खेती कर रहे हैं. नया युवक इस खेती के धंधे में आना नहीं चाहता. वह शहरों की चकाचौंध देख शहरों की ओर भाग रहा है.
आजादी के बाद सारी विकास की योजनाएं शहरों को केंद्र में रखकर तैयार की गई. किसान तथा कृषि प्रधान देश का नारा संसद तक सीमित रहा. कृषि अर्थव्यवस्था तो अब सारी बाजार और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास चली गई है. देखते-देखते सारे किसान अपनी भूमि पर गुलाम हो गए. आखिर, क्या कारण हैं जो किसान खेती से बाहर आना चाहते हैं? बहरहाल, अगर 130 करोड़ जनता को अन्न चाहिए तो अन्नदाता को गांव में रोकना होगा, उसे बेहतर जीने का अवसर देना होगा, जैसी दुनिया के विकसित राष्ट्र अपने किसानों को देते हैं, वैसी व्यवस्था लानी ही होगी.
| Tweet |