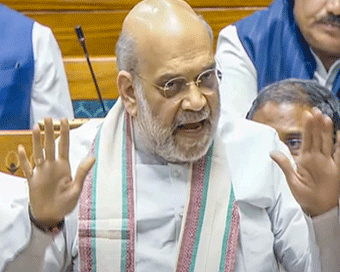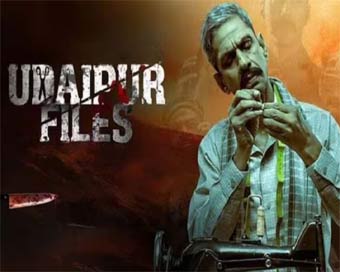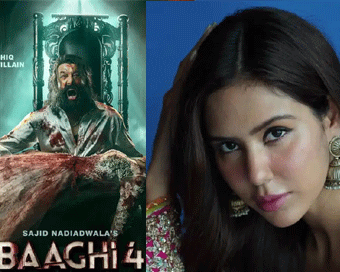गणतंत्र दिवस : संबोधन के मायने
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का राष्ट्र के नाम संदेश गणतंत्र दिवस पूर्व संध्या पर दिया जाने वाला आखिरी संदेश है. वे जुलाई 2012 में प्रतिभा पाटिल के बाद पांच वर्षों के लिए राष्ट्रपति चुने गए थे.
 गणतंत्र दिवस : संबोधन के मायने |
राष्ट्रपति के संदेश की समीक्षा की एक परंपरा है; क्योंकि इस संदेश में समय के अंतर्विरोधों , बहसों के स्पष्ट संकेत होते हैं और उनमें आगे निकलने के सुझाव होते हैं.
राष्ट्रपति का संदेश इसीलिए भी महत्त्वपूर्ण होता है; क्योंकि उनसे पार्टीगत राजनीति से अलग भूमिका में होने की अपेक्षा की जाती है. संविधान को सर्वोपरि मानकर उसके प्रमुख के तौर पर उनका संदेश हमें अपनी राजनीतिक विरासत की याद दिलाता है. इस बार का राष्ट्रपति संदेश स्वतंत्रता हासिल करने, उसे बनाए रखने के लिए संविधान बनाने और संविधान में लिये गए देशवासियों के शपथ की याद दिलाने की जरूरत महसूस करता है. ‘जब भारतीय जनता ने इसके सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और लैंगिक और आर्थिक समता के लिए स्वयं को एक संविधान सौंपा. हमने भाईचारे, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रोत्साहित करने का वचन दिया.’ राष्ट्रपति जोर देकर कहते हैं कि इसी जनता के शपथ और नागरिक के उद्देश्य ने ही हमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का दावेदार कहलाने की ताकत देता है. जनता और नागरिक के बीच की इस यात्रा को समझना, आज सबसे बड़ी जरूरत लगती है.
दरअसल, जिन राजनीतिक अंतर्विरोधों से हमारा समाज और देश गुजर रहा है वहां अपनी विरासत की याद भी कराना एक महत्त्वपूर्ण राजनैतिक काम की तरह है. यह नागरिक-देश की वास्तविकता को हासिल नहीं कर पाने की विफलता की तरफ संकेत है. वे अपने पूरे संदेश में उस पृष्ठभूमि को दोहरा रहे हैं, जहां से हमें ब्रिटिश साम्राज्य के सीधे नियंत्रण से मुक्ति मिली और जहां तक की यात्रा इस देश ने पूरी की है उसे सुरक्षित रखने की जद्दोजहद पर वे जोर दे रहे हैं. यह एक गंभीर राजनीतिक संकेत है. राष्ट्रपति के असंतोष की भी अपनी शैली होती है; क्योंकि उन्हें देश के नागरिकों के सामने एक स्वर्णिम तस्वीर पेश करनी होती है और नागरिकों के भीतर उत्साह पैदा करने की कोशिश होती है. वे कहते हैं कि ‘जैसे हम यहां तक पहुंचे हैं वैसे ही और आगे भी पहुंचेंगे. परंतु हमें बदलती हवाओं के साथ तेजी से और दक्षतापूर्वक अपने रु ख में परिवर्तन करना सीखना होगा.’
राष्ट्रपति के भाषण का एक हिस्सा नागरिकों के नाम संदेश है तो दूसरी हिस्सा राजकीय कामकाज की एक मोटी समीक्षा भी होती है. यह समीक्षा कई स्तरों पर होती है. इनमें तात्कालिक विषयों पर राष्ट्रपति के संकेतों को उनकी एक टिप्पणी के रूप में देखा जाता है. वे देश में सबसे ज्यादा असर डालने वाले विमुद्रीकरण के फैसले पर अपनी टिप्पणी इस रूप में दर्ज कराते हैं. ‘काले धन को बेकार करते हुए और भ्रष्टाचार से लड़ते हुए, विमुद्रीकरण से आर्थिक गतिविधि में, कुछ समय के लिए मंदी आ सकती है.’
मौजूदा राजनीतिक हालात पर अपने तरीके से राष्ट्रपति ने कटाक्ष किया है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. वे जब कहते हैं कि जो कुछ हमने उपलब्धियां हासिल की है वह इसीलिए कि ‘स्वतंत्र भारत में जन्मी, नागरिकों की तीन पीढ़ियां औपनिवेशिक इतिहास के बुरे अनुभवों को साथ लेकर नहीं चलती हैं. ‘वे बुरे अनुभव क्या है. वे अनुभव देश का साम्प्रदायिकता के आधार पर विभाजन है. यह विभाजन महज जमीन का बंटवारा नहीं था बल्कि वह समाज में मिल-जुलकर सोचने और आगे बढ़ने और साम्राज्यवाद यानी वर्चस्व के खिलाफ लड़ने की एकजुट ताकत का बिखराव था. सामूहिक चेतना का आधुनिक निर्माण मानव सभ्यता की लंबी यात्रा के बाद ही संपन्न होता है. भारत और पाकिस्तान के बनने का अंत नहीं है. पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश बना है और ये भी अभी दावा से नहीं कहा जा सकता है कि भविष्य कितने ऐसे टुकड़ों में बंट सकता है. इसीलिए वे जोर देते हैं कि ‘भारत का बहुलवाद और उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषायी और धार्मिंक अनेकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है. हमारी परंपरा ने सदैव ‘असहिष्णु’ भारतीय नहीं बल्कि ‘तर्कवादी’ भारतीय की सराहना की है.’
दरअसल, मौजूदा राजनीति पर इसे एक टिप्पणी के रूप में दर्ज किया जा सकता है और यह पहली बार नहीं है कि आजादी के संघर्ष की छाया में अपना राजनीतिक जीवन जीने वाले प्रणव मुखर्जी ने बतौर राष्ट्रपति सबसे ज्यादा बार सार्वजनिक तौर पर बहुलतावाद और विविधता पर जोर दिया है; क्योंकि उन्हें इस दौर में सबसे ज्यादा इन पर हमले के अनुभवों से गुजरना पड़ा है. राष्ट्रपति सरकार के कार्यक्रमों की सफलता की तस्वीर तो पेश करने की सीमाओं से बंधे होते हैं, लेकिन उनके संदेशों का जो राजनीतिक पक्ष है वह नागरिकों के लिए महत्त्वपूर्ण संदेश होता है. वह राजनीतिक तौर पर नागरिकों को सचेत करता है.
प्रथम नागरिक की भूमिका नागरिकों को सचेत करने के साथ समाज पर टिप्पणीकार की भी होती है. उनकी यह टिप्पणी गौरतलब है कि ‘कभी-कभी स्वतंत्रता को हल्के में लेना; असाधारण पुरुषों और महिलाओं द्वारा इस स्वतंत्रता के लिए चुकाए गए मूल्यों को भूल जाना; और स्वतंत्रता के पेड़ की निरंतर देखभाल और पोषण की आवश्यकता को विस्मृत कर देना आसान हो जाता है.’ राजनीतिक तौर पर एक गंभीरता की जरूरत पूरे देश में वे महसूस करते हैं और युवाओं की मौजूदा स्थिति को लेकर संदेश में अपने तीक्ष्ण नजर को प्रस्तुत कर रहे हैं. ‘वे रोजमर्रा की भावनाओं के उतार-चढ़ाव में, और अपने लिए निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति में प्रसन्नता खोजते हैं. अवसरों की कमी से उन्हें निराशा और दुख होता है, जिससे उनके व्यवहार में क्रोध, चिंता, तनाव और असामान्यता पैदा होती है. लाभकारी रोजगार, समुदाय के साथ सक्रिय जुड़ाव, माता-पिता के मार्गदशर्न, और एक जिम्मेवार समाज की सहानुभूति के जरिए उनमें समाज अनुकूल आचरण पैदा कर इससे निपटा जा सकता है. ‘राष्ट्रपति का आखिरी गणतंत्र दिवस संदेश राजनीतिक दृष्टि से अहम है और देश के अंदरूनी हालात की तरफ स्पष्ट संकेत है.
| Tweet |