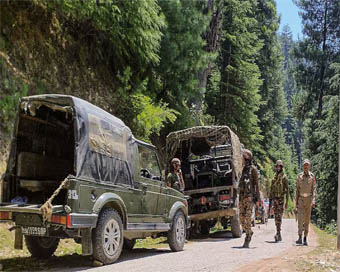वित्तीय पूंजी को समझने की एक कोशिश
वित्तीय पूँजी पर बहुत कुछ लिखा गया होगा और लिखा जा रहा है. मेरा अनुमान है कि आज वित्तीय पूंजी की मात्रा औद्योगिक पूंजी की मात्रा से अधिक हो गई है.
 राजकिशोर, लेखक |
अगर ऐसा नहीं है तब भी उसकी मात्रा इतनी तो है ही कि उसकी भूमिका पर विचार करना जरूरी लगता है. वित्तीय पूंजी का आविर्भाव वहीं से होता है जहां से औद्योगिक पूंजी का. जब पूंजीवाद का विकास नहीं हुआ था, उसके सौ-डेढ़ सौ वर्षो में एकल पूंजी ने उसका रास्ता प्रशस्त किया. जिसके पास पैसा होता था, वह कारखाना डाल लेता था और मजदूरों का खून-पसीना एक कर देता था. यह वही दौर था जब पुरु षों और स्त्रियों से बारह से सोलह घंटे तक काम कराया जाता था. वे फटेहाल रहते थे और उनका हर अगला दिन कुपोषण का होता था. कह सकते हैं, यह पूंजीवाद का पाषाण युग था.
लेकिन पाषाण युग कहीं भी ज्यादा चलता नहीं है. अगर पूंजीवाद का वही निर्दय युग जारी रहता, तो निसंदेह मार्क्स की परिकल्पना के अनुसार सर्वहारा वर्ग विद्रोह कर देता और अपने को भी और अपने मालिक को भी मुक्त कराता. ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पूंजीवाद साल-दर-साल सामथ्र्यवान होने लगा, उसकी उत्पादकता बढ़ती गई और उपनिवेशों को लूट कर वह अपने मजदूरों को ज्यादा पगार तथा अन्य सुविधाएं देने लगा. बाद में यह संघर्ष भी सफल रहा कि किसी से भी दिन भर में आठ घंटे से ज्यादा काम न कराया जाए.
पूंजीवाद का विकास जितनी तीव्र गति से हुआ, वह एक लंबी कहानी है. लेकिन पूंजीवाद ने जो कुछ हासिल किया, उसका श्रेय औद्योगिक पूंजी को है न कि वित्तीय पूंजी को. मिल-कारखाने बढ़ते गए, नए उत्पाद सामने आते गए और बाजार का विस्तार होता रहा. यह एक ठोस प्रगति थी, जिससे आम आदमी का शोषण तो बहुत हुआ और आज भी हो रहा है, पर उसके साथ-साथ वस्तुएं बनीं, सड़कें बनीं, रेलगाड़ियां दौड़ीं और विमान उड़े. वस्तुत: सभ्यता के नाम पर आज हम अपने आसपास जो कुछ देखते हैं, वह सब औद्योगिक पूंजी का कमाल है.
पूंजी कहते ही उस धनराशि को हैं जिसका निवेश माल या सेवा के उत्पादन में किया जाए. यह काम समाजवादी तरीके से किया जाए तो वस्तुएं और सेवाएं ज्यादा पैदा होंगी और पैदा करने वालों के रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठेगा. समाजवादी रास्ता मानवीय समस्याओं के समाधान का है, जबकि पूंजीवादी रास्ता यह करते हुए अधिक से अधिक मुनाफा कमाने का है. जिस रास्ते पर मुनाफे का बुलडोजर चल रहा हो, वहां लागत और कीमत के बीच कोई विवेकसंगत संबंध नहीं रह जाता. इससे कई नई समस्याएं पैदा होती हैं.
ऐसी व्यवस्था में ही अमीरों के पास समाज के धन का संकेंदण्रहोता जाता है और श्रमिक वर्ग के हाथ में इतना पैसा नहीं आता कि वह कोई उद्योग शुरू करने की सोच सके. एक इलाके के सारे मजदूर मिल कर भी यह सपना नहीं देख सकते. करोड़पति का घोड़ा चारों ओर दौड़ता है और गरीब सिर्फ गृहपति बन कर रह जाता है. बहरहाल, इससे भी प्रगति होती है. समाज को नई-नई चीजें मिलती हैं और मुनाफे में श्रमिक का हिस्सा बढ़ता जाता है. अमेरिका में तो यह हिस्सा इतना बढ़ गया है कि वहां के उद्योगपति अपना माल दूसरे देशों के मजदूरों से बनवाने लगे हैं, जिनकी प्रति घंटा कीमत उनके देश से बहुत कम है. भाग्य ही मनुष्य को जहां-तहां नहीं ले जाता, उद्योग भी ले जाता है.
कह सकते हैं कि आज के जमाने में उद्योग ही भाग्य है और श्रमिक होना दुर्भाग्य. इस संदर्भ में सवाल करता हूं : वित्तीय पूंजी क्या करती है? क्या वह किसी वस्तु का उत्पादन करती है? क्या वह कोई सेवा प्रदान करती है? क्या वह समाज की उत्पादकता को बढ़ाती है? वह इनमें से कुछ भी नहीं करती. वह सिर्फ रुपए से रुपया पैदा करती है. रुपए से रुपया तो उद्योगपति भी पैदा करता है, पर वह इसके लिए कारखाना और दुकान खोलता है, माल बनाता और बेचता है. इससे समाज की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है. इस प्रकार उत्पादन एक सामाजिक कर्म है. उससे समाज को कुछ मिलता है.
वित्तीय पूंजी असामाजिक घटना है, क्योंकि वह कुछ पैदा नहीं करती, बस रुपए से रुपया बनाती है. यही काम गांव का सूदखोर करता था और बदले में समाज की घृणा प्राप्त करता था. अब तो इस धंधे पर रोक लग चुकी है. लेकिन वित्तीय पूंजी के खेल का दायरा बढ़ता जा रहा है. वह सस्ते दाम पर शेयर और प्रभूतियां खरीदती है और महंगे दाम पर बेच देती है. वह बैंकों को उधार देती है और उनसे ब्याज लेती है. उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई है कि वह किसी भी देश के शेयर बाजार में हस्तक्षेप कर वहां की अर्थव्यवस्था में हड़कंप मचा सकती है.
संक्षेप में, वित्तीय पूंजी वह है जो किसी उद्योग-धंधे में नहीं लगाई जाती, बल्कि या तो सूदखोरी में लगाई जाती है या शेयरों की खरीद-बिक्री में. कारखाना किसी एक जगह स्थापित होता है. दुकान भी एक जगह लगाई जाती है. इनमें लगी हुई पूंजी आवारा पूंजी नहीं हो सकती, क्योंकि पूंजी यहां स्थान विशेष से बंधी होती है. लेकिन सूदखोरी और शेयरों की खरीद-बिक्री का काम किसी भी जगह से हो सकता है. चूंकि ये सौदे अंतरराष्ट्रीय होते हैं, इसलिए वित्तीय पूंजी यहां से वहां फुदकती रहती है. वह हरजाई है- किसी एक देश या क्षेत्र से उसे कुछ भी लेना-देना नहीं है. क्या इस हरजाई को नाथा जा सकता है? क्या इससे सामाजिक पूंजी का निर्माण किया जा सकता है? इस पर योजनाकारों को विचार करना चाहिए. लोगों के पास अतिरिक्त धन है और उसे आप किसी उत्पादक काम में नहीं लगाएंगे, तो वह कहीं न कहीं गोलमाल करेगा ही.
Tweet |