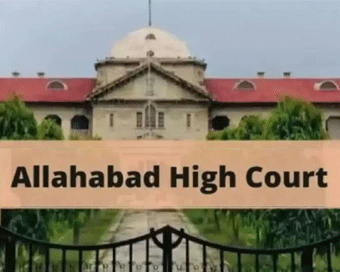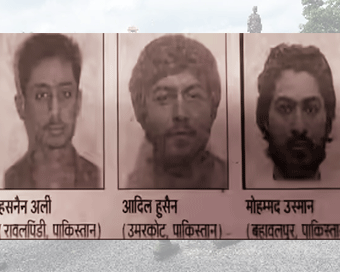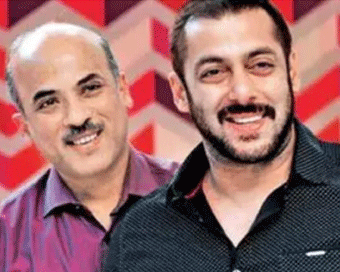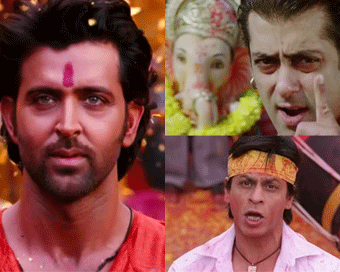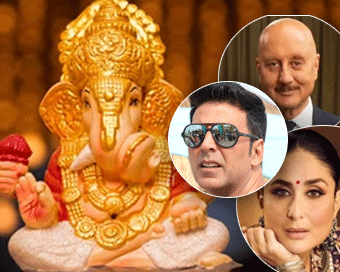सूखे इलाके : उम्मीद के अलाव
देश के करीब 624 सूखे इलाकों में से सवा सौ हर साल सूखे की चपेट में आते हैं।
 सूखे इलाके : उम्मीद के अलाव |
राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक सहित नौ राज्य हैं, जहां सूखा पड़ता है, पलायन होता है, दम तोड़ते हौसले के बीच किसानों के मन में मौत को गले लगाने का खयाल भी आता है। सरकारी योजनाओं के सिरे कभी पकड़ में आते हैं, कभी नहीं।
सूखे इलाकों के लिए जीने लायक इंतजाम को ही हमने सबसे बड़ा सवाल बना दिया है। ऐसे में यहां के किसानों के लिए खेती कभी फायदे का सौदा बन ही नहीं पाई। बिना पानी के क्या खेती, क्या अन्न, क्या घर और क्या सुकून। फिर भी हकीकत है कि देश को पैदावार देने वाली जमीन में 68 फीसद हिस्सेदारी सूखे इलाकों की ही है। इसलिए यहां हर एक बूंद को संभालना, हर किसान का हाल लेना, देश की आर्थिक सेहत के लिए बेहद जरूरी फिक्र है। डिजिटल दौर में तेजी से तैरकर आती जानकारियों ने सूखे इलाकों के किसानों में जीवन की बेहतरी के लिए बेचैनी पैदा की है। खेती की समझ उन्हें भरपूर है, मालूम है कि टिकाऊ खेती के लिए कौन सी खाद, मिट्टी, बीज माफिक हैं, और मौसम का बदलता-बिगड़ता मिजाज कैसे सहना है। रासायनिक खेती के नुकसान से वाकिफ किसानों का मन मुनाफे के लिए भी कसा हुआ है। लेकिन पानी के परंपरागत स्रोतों की अनदेखी से कई इलाकों के तले खाली हो चुके हैं। इन्हीं सूखे इलाकों में पीने का पानी तक खरीदने की नौबत है।
सूखे और पलायन की वजह से सुर्खियों में रहने वाले इलाकों में महाराष्ट्र का सोलापुर भी है। इस पहचान का दाग मिटाने के लिए यहां के माढ़ा तालुक के युवाओं ने जमीन में दबे हुए बेंद नाम के ओढ़ा यानी छोटी नदी के निशान तलाशने शुरू किए थे कुछ साल पहले। साल भर में बरसने वाले 400-500 मिमी. पानी को सहेजने में हमेशा नाकाम रहे माढ़ा के दर्जन भर गांवों ने जिस नामुमकिन से काम को कामयाब किया उसे देखकर लगता है कि ऐसी कहानियां ही आज सूखे इलाकों के लिए तसल्ली का रास्ता खोल रही हैं। किसानों को मजदूर बना देने वाले इस देश में सूखे इलाकों का सबसे बड़ा दर्द पलायन ही रहा है। माढ़ा तालुक के कुरूड़ गांव की सुमन गावली सहित गांव के तमाम किसान जब करीब ले जाकर 12 गांवों और 2 नगर पंचायतों से गुजरने वाला 37 किमी. लंबा बेंद नाला दिखाते हैं, तो इस गांव के करीब पांच सौ और आस-पास के गांवों के हजारों परिवारों की बदली तकदीर की कलकल भी सुनाई देती है। जहां खेती की जमीनों पर कारोबारियों और नेताओं की खराब होती नीयत की हकीकत हो गई है, उस दौर में सुमन जैसे सैंकड़ों परिवारों ने अपने नदी-नालों को जीवित करने के लिए उसके रास्ते में आई अपनी कीमती जमीनें दिल खोल कर दे दीं। बिना किसी शर्त, बिना मुआवजे के, बिना फिक्र। तंगदिली न होना और समझदार-ईमानदार युवाओं का गांव की ओर मुड़ना इस दौर की सबसे खास खबर है।
मेहनतकश किसानों को पढ़े-लिखे युवाओं का साथ मिल जाए तो वो वैज्ञानिकता और आधुनिकता के पाठ को कितनी आसानी से अपना लेंगे, और आपके इस अहसान के बदले अपने प्राण तक देने को तैयार रहेंगे, यह बात स्वामी विवेकानन्द ने राजस्थान के अलवर में अपने प्रवास के दौरान युवाओं के साथ संवाद में कही थी। मिट्टी में दबे बेंद नाले की मरम्मत, खुदाई और छोटे बांध बना कर पानी रोकने का खर्च सरकारी रास्ते से करीब नौ करोड़ का बना। पानी को गांव-गांव बांधने, खेतों के लिए नमी का बंदोबस्त करने और परंपरागत तरीकों को तरजीह देकर अपनी कीमत खुद तय करने का पूरा खाका दिमाग में तैयार था। इस शिद्दत ने नदियों को जीवित करने में जुटी ‘नाम’ फाउंडेशन के गणोश और मल्हार का साथ हासिल किया और संगठन और समुदाय की भागीदारी से बेंद का जीवन लौटाने का काम 10-12 लाख में दो साल में ही हो गया। अन्न की संभाल में जुटे समाज के बहाव का यह एक तट था, जिसने मिलजुल कर तटबंध तैयार कर लिए। कुरूड़ के बगल के ही गांव भोसरे में कई किसान आज एक सुर में बात करते हैं कि जो पानी अब तक 600 फीट की गहराई पर पकड़ में आता था, बेंद नाले के जीवंत होने से अब 5-7 फीट तक आ पहुंचा है, इससे बेहतर और क्या। कमाई पहले के मुकाबले 5-6 गुना होने से काम की तलाश में घर से दूर जाना खत्म हुआ। मवेशियों की आबादी हर गांव में इंसानी आबादी की करीब तीन गुना है। सूखा पड़ने पर दूध की कमाई से ही गुजारा होता था, मगर हरा चारा भी नसीब नहीं था। अब सब भरपूर है, और भरे-पूरे मन वाले यहां के डेढ़ हजार से ज्यादा परिवारों वाला यह गांव खुद तो तर है ही मगर चाहता है कि आगे के और चार गांव जरूरतमंद हैं, इसलिए खुदाई और आगे तक हो, इस बार बाढ़ में टूटे बांधों की मरम्मत भी हो। किसान मन ही इस अहसास के साथ जीता है कि धरती में हम सब साथ पिरोए हुए हैं।
देश के कई इलाके हैं, जहां किसान संगठित होकर उपज बढ़ा रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। मगर माढ़ा के करीब चार हजार किसानों के इस संगठन की असल कहानी भगीरथी कोशिशों और कामयाबी की ही है। पानी की फिक्र से बरी होकर, फसलों के नवाचार में लगे इस इलाके के किसान दो साल पहले तक एक फसल भी बमुश्किल ले पाते थे। आज परंपरागत ज्वार, गेहूं, मक्का, तुहर, प्याज के अलावा कई नई किस्मों की पैदावार हो रही है। खुद की हिस्सेदारी है, तो अनार, अंगूर सहित देश-विदेश की मांग को ध्यान में रखकर अच्छी कमाई वाली फसलें भी उगा रहे हैं। इस संगठन के खड़े किए आकुंठ फॉर्म में किसान शेयर धारक हैं। कई कंपनियों से करार हैं। मिट्टी की जांच, खेत की सेहत, खाद की जरूरत सहित कमाई का लेखा जोखा सब संगठन से जुड़े किसानों को स्मार्ट कार्ड के जरिए हासिल हो जाता है। कैसे दुनिया की बेहतरीन समझ को अपने गांव-खेड़े तक लाने के लिए युवा पूरे जोश से जुटे हैं। खरी समझ वाले ये किसान ही आने वाले दौर के असल नुमाइंदे हैं, जिनकी रफ्तार और पानीदार काम कायम रहे, यह उम्मीद के अलाव में बैठे चेतन समाज का ही जिम्मा है।
| Tweet |