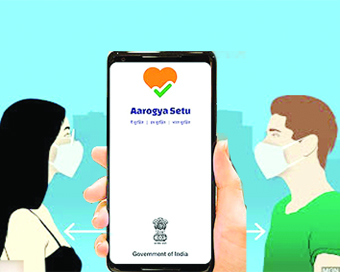आर्थिक नियोजन : व्यापक बदलाव की जरूरत
कभी कभी गहरे राज का पर्दाफाश अनायास ही हो जाता है। घटनाक्रम कुछ और होता है, और उसकी छानबीन के दरम्यान अलग तरह का सच सामने आ जाता है।
 आर्थिक नियोजन : व्यापक बदलाव की जरूरत |
यह क्षण अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, निर्बल को सबल बनने के लिए प्रेरित करता है, सत्य-असत्य को परिभाषित कर देता है।
इसी पृष्ठभूमि में गौर करें। विश्वव्यापी महामारी ‘कोरोना’ के बढ़ते दुष्प्रभाव और उससे बचाव के उपाय के दौरान तरह-तरह के चेहरे और दिल दहला देने वाले अतीत के सरकारी दावों की पोल खुली है। कोरोना के चलते जो पोल खुले हैं, उसमें बेरोजगारों, श्रमिकों और उनके परिवारों के हालात पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के दिल दहलाने वाले बर्ताव भी शामिल है। कोरोना की वजह से लागू आवास निवास बंधन (लॉकडाउन) से यह पता चला है कि देश में बेरोजगारी विष वृक्ष ने नौनिहालों को जकड़ रखा है। वहीं लालफीताशाही और सफेदपोश संस्कृति निश्चिंत होकर अमरबेल के पथ पर अट्टहास कर रही है। श्रमिकों और गरीबों को मदद देने का वादा कर बेशर्मी का ढोल बजाया जा रहा है मानों ‘अहो रूपम अहो ध्वनि’ का नाद हो रहा है। खैर! कोरोना से संघर्ष कर रहे लोगों को गुमराह कर संघर्ष की रूपरेखा के पीठ में खंजर भोंकने के भी संकेत मिले हैं।
अपने गृह प्रदेश में जाने के लिए आतुर मजदूरों को पल्रोभन दिखाकर पीछे हटने की अमानवीय रणनीति का भी पर्दाफाश हुआ है। अपने ही देश के लोगों ने देशवासियों को ‘प्रवासी मजदूर’ कहकर मजदूरों और गरीबों के धैर्य को तोड़ा है। प्रतिक्रिया में जानकार यही प्रतिपादित कर रहे हैं कि देश बंटवारे ने लाखों का कत्ल कराया, लाखों की इज्जत और संपत्ति लूटी गई। सुरक्षा का वचन देकर विश्वासघात हुआ। वहां रह गए 20 फीसद अल्पसंख्यक हिंदू घट कर गिनती के बचे हैं और जिल्लत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। बहरहाल, देश में कोरोना से प्रभावित मजदूरों की हरसंभव मदद करने के लिए सशक्त केंद्र सरकार और ज्यादातर राज्य सरकारें योजनाबद्ध तरीके से सक्रिय हैं। इस वजह से ‘सेक्युलर छाप’ रोटी सेंकने वाले मदारी और जमूरे काफी परेशान हैं। अस्तु यक्ष प्रश्न यह कि, 70 साल पहले अंग्रेजों की दासता से मुक्त भारत का आर्थिक ढांचा दयनीय दशा में क्यों है? इतना लंबा काल खंड बीत जाने के बावजूद देश का किसान, शोषित-पीड़ित, आदिवासी-वनवासी और मजदूर ‘मजे से दूर’ (आर्थिक सबल होने से) क्यों हैं? क्या तत्कालीन सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया? क्या सरकारें दूरदृष्टिविहीन थीं? नहीं। सरकार चलाने वालों ने विदेशों में पढ़ाई की थी, प्रगतिशील थे, योजनाकार थे लेकिन लोमड़ी की तरह चालाक थे। गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन और अशिक्षा उन्मूलन के लिए असंख्य योजनाएं बनाई। पर बजट की रकम नौकरशाहों, दलालों और सफेदपोशों की थैली में गई। असल में भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गरीबी को एक सापेक्ष अवधारणा माना गया है। हालांकि यह अवधारणा अलग अलग देशों में अलग अलग है।
भारत में यह अवधारणा अलग-अलग भौगोलिक परिस्थितियों, सामाजिक-धार्मिंक सोच,भाग्य-प्रारब्ध और पारंपरिक कौशल पर निर्भर है, जबकि सत्ता के सूत्रधारों ने नई सोच और नये परिवेश पर बल दिया। नतीजतन देश के कोने-कोने से निकलकर लोग रोजगार के लिए शहरों में भटकने लगे। फुटपाथ उनके लिए रैन बसेरा बनने लगे। देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था तार- तार हो गई। यह हालात अब भी बदस्तूर जारी है। गरीबी उन्मूलन के नाम पर गरीबों को ही निपटाने की कहावत प्रचलित हो गई। गरीबों का मसीहा साबित होने के लिए तत्कालीन सरकार के दो बड़े फैसलों पर गौर करें। पहला फैसला देश के पूर्व राजाओं को दिए जाने वाले प्रिवी पर्स (पॉकेट खर्च) को खत्म करने से संबंधित था। देश के राजाओं ने अपने राज्य का विलय भारत संघ राज्य में कर दिया। किसी राज्य की भूमि और अन्य संपत्तियों का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था। फिर भी छोटे राजा बड़े राजा के अनुसार पांच-दस रुपये से लेकर लाख रुपये पाकेट खर्च देने का वादा हुआ था। यह वादा पीढ़ी दर पीढ़ी देने के लिए नहीं था। केवल संबंधित पीढ़ी के लिए था। गरीबों के हक का हवाला देकर इसे खत्म कर दिया गया। प्रश्न यह है कि, इस फैसले से बची रकम को आवंटित करने के लिए प्रचलित गरीबों को नहीं बल्कि सरकार ने विधायक-सांसद जैसे नये गरीब ढूंढ़ लिये। तत्कालीन सरकार ने दूसरा फैसला बैंकों के राष्ट्रीयकरण के संबंध में किया। गरीबों के नाम पर बैंको पर सरकार ने कब्जा कर लिया।
यह विडंबना ही है कि, भारत में प्रचलित कुटीर उद्योग और पारंपरिक रोजगार से विरत करने की नीति अंग्रेजों के शासनकाल में ही शुरू हो गई थी। इसका सबसे सजीव उदाहरण नमक कानून है। आजाद भारत में दोहरी नीति अपनाई गई। एक ओर पारंपरिक और कुटीर उद्योग वाले उत्पाद को बनाने के लिए बड़े कारखाने और मिल खोलने के लिए लाइसेंस दिए जाने लगे तो दूसरी ओर घरेलू उत्पादकों को संरक्षण देने के नाम पर बजटीय झुंझुना दिया जाने लगा। हद तो यह है कि शराब का कारखाना खोलने के लिए लाइसेंस दिया जाता है तो दूसरी ओर इससे परहेज करने का संदेश देने के लिए दारूबंदी विभाग का गठन होता है। आशय यह कि, बीते सौ साल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तहस- नहस करने का क्रम जारी रहा है। अब सवाल है कि इस देश में गरीब कौन है? इसका पता लगाने के लिए भोजन को पैमाना बनाया गया है। इसी के आधार पर यह तय होता है कि कौन गरीबी रेखा के नीचे और कौन ऊपर? फिलहाल जो 2400 कैलोरी तक उपभोग करता है वह गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करता है। दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रश्न बेरोजगारी और रोजगार की तलाश से जुड़ा है।
यह तो स्पष्ट है कि अनेक राज्य अन्य राज्य के लोगों को रोजगार देने में सक्षम हैं, तो कई राज्य बेरोजगारों की फौज बनाने में सक्षम हैं। यह असंतुलन कब खत्म होगा। कोरोना महामारी के कहर ने जाने-अनजाने में भारत में व्याप्त आर्थिक विषमता को उजागर कर दिया है। इसे मोहक चित्र नहीं बल्कि एक्स-रे या एमआरआई फिल्म के रूप में देख कर आत्ममंथन की जरूरत है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने लिए कई सकारात्मक पहल की है। फिर भी देश की जटिल परिस्थितियों को देखते हुए आर्थिक नियोजन में व्यापक बदलाव की जरूरत है।
(लेखक एस्ट्रोलॉजी टुडे के संपादक हैं)
| Tweet |