मनरेगा : सब कुछ उजला नहीं है
लॉकडाउन के हालात में जिन कुछ सरकारी योजनाओं ने देश को राहत दी है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एंप्लाइमेंट गारंटी एक्ट (मनरेगा) उनमें से एक है।
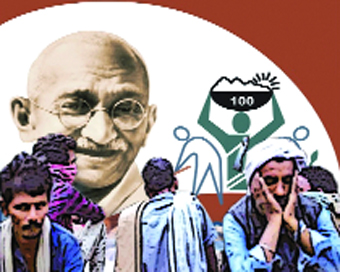 मनरेगा : सब कुछ उजला नहीं है |
इधर बड़े पैमाने पर मजदूर शहरों को छोड़कर अपने गांवों में पहुंचे हैं, वहां उन्हें मनरेगा के तहत काम भी मिल रहा है और पहले के मुकाबले इसमें तय से ज्यादा मजदूरी (एक दिन के काम के लिए 182 रुपये की जगह 202 रुपये) भी मिल रही है। मजदूरी की इस दर में इजाफा हाल में ही केंद्र सरकार ने किया है। दावा है कि एकाध राज्यों ने मनरेगा के तहत काम देने में यह शर्त भी खत्म कर दी है कि मजदूर कौन-से राज्य से आए हैं; जैसे झारखंड के पालकोट में मुंबई, बेंगलुरू, गोवा, दिल्ली यहां तक कि पड़ोसी देश भूटान तक से आए 2500 मजदूरों को इसमें काम दिया गया है। लेकिन मनरेगा में सब कुछ उजला नहीं है।
कुछ कस्बाई और शहरी तबकों को छोड़कर देश के जमीनी हालत का अंदाजा लेने निकलेंगे तो पता चलेगा कि चाहे कोरोना हो या नहीं, वहां हमेशा एक लॉक-डाउन सी स्थिति बनी रहती है। वहां आज भी 50 फीसद से ज्यादा आबादी ऐसी है, जिसके पास साल के कुछ ही महीने काम रहता है। बाकी दिन कटते हैं ग्राम प्रधानों, ठेकेदारों- सरकारी बाबुओं की चिरौरी करते कि वे किसी तरह मनरेगा के तहत उनका जॉब कार्ड बनवा दें। साल में सौ दिन की रोजी पक्की करने वाली इस योजना-मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी कई बार महंगाई दर के सामने ‘ऊंट के मुंह में जीरे’ वाले हालात पैदा करती है, लेकिन इसकी विडंबनाएं कुछ और भी हैं। जैसे कि यह इसकी गाइडलाइन के बावजूद ज्यादातर राज्य इस योजना में मजदूरों को अलग-अलग रकम देते हैं। जो सरकार पूरे देश में वस्तुओं की कीमतें एक समान रखने के लिए ‘वन नेशन-वन टैक्स’ के तहत जीएसटी के प्रावधान लागू करवा सकती है, हास्यास्पद है कि मनरेगा में उसे राज्यों के विभेदकारी रवैए से कोई परेशानी नहीं होती।
सरकार के एजेंडे में मजदूरों का अच्छा जीवन क्यों नहीं है-यह इस योजना से जुड़ी सबसे अजब पहेली है। यूपीए-1 शासनकाल में वर्ष 2005 में संसद से पारित कर 2 फरवरी 2006 को देशभर के 200 जिलों में लागू की गई राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) योजना (जिसका नाम 2009 में बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मनरेगा किया गया) में तय किया गया था कि गांव-कस्बों में स्थानीय विकास के तमाम सरकारी कार्यों के तहत अकुशल, अर्ध कुशल और कुशल मजदूरों को सौ दिन काम दिया जाएगा, ताकि उनका शहरों की तरफ पलायन रु के। साथ ही, अशिक्षित बेरोजगारी से कुछ राहत मिल सके। इस योजना में फिलहाल 13.62 करोड़ जॉब कार्डधारक हैं, जिनमें से 8.17 करोड़ जॉब कार्डधारक सक्रिय हैं। यूं इस योजना की चाहे जितनी आलोचना की जाए, इसमें तमाम नुक्स निकाले जाएं, लेकिन एक दौर में इसकी विरोधी रही भाजपा भी जब सत्ता में आई, तो उसे भी इसका महत्त्व समझ में आ गया। केंद्र में आई बीजेपी सरकार भले ही मनरेगा के रोल को लेकर सहज हो गई, लेकिन कई राज्य सरकारों को लगता है कि मनरेगा से लाभान्वित होने वाले मजदूरों के मन में राज्य सरकार की बजाय केंद्र सरकार के प्रति झुकाव बन जाता है। इसलिए वे इसमें हुई बढ़ोत्तरी मजदूरों को देने में आनाकानी करती हैं। इस योजना के नियम, मापदंड और उद्देश्य पूरे देश के लिए एक समान हैं, लेकिन इन सारी गाइडलाइंस की अवहेलना कर राज्य सरकारें श्रमिकों की मजदूरी दर समान रखने की शर्त से मुकर जाती हैं।
सवाल यह उठता है कि जब मनरेगा का उद्देश्य एक है, क्रियान्वयन के मापदंड आदि नियम एक जैसे हैं, तो राज्यों में मजदूरी की दरों में यह भिन्नता क्यों। राज्यवार देखें तो देश के 17 राज्यों में मनरेगा के अकुशल श्रमिकों को 200 रुपये से कम राशि की ही दिहाड़ी दी जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे राज्यों की संख्या 34 है, जहां मनरेगा के अकुशल श्रमिकों की मजदूरी 200 रु पये से भी कम है। अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल आदि विभाजन पर दरों में अंतर स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन समान श्रेणी के मजदूरों के पारिश्रमिक में राज्यों की ओर से किए गए मनमाने बदलाव इस योजना के उचित क्रियान्वयन पर सवाल खड़े करते हैं। हालांकि एक विरोधाभास यह भी है कि जो मजदूरी मनरेगा में मिलती है, उसके एवज में कोई श्रमिक काम नहीं करना चाहता, लेकिन लॉकडाउन जैसे हालात में ऐसी ही योजनाओं के तहत मिलने वाले मानदेय से जिंदगी की गाड़ी खिंचती है- इसे अवश्य ध्यान में रखना होगा।
| Tweet |





















