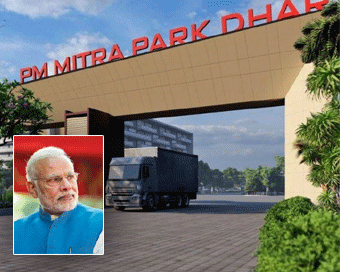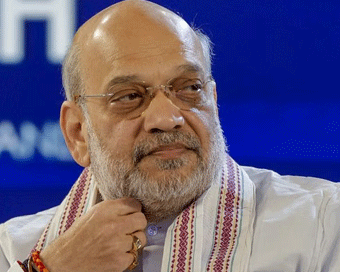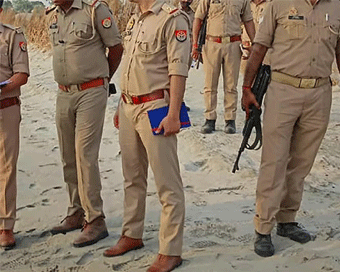मुद्दा : नेटबंदी के दुख-दर्द
देश हर मामले में डिजिटल हो जाए-इसकी एक कल्पना सरकारी अभियान-डिजिटल इंडिया के तहत की गई है।
 मुद्दा : नेटबंदी के दुख-दर्द |
हमारे देश में भी अब 65 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़े हैं, उसके फायदे ले रहे हैं-यह दावा भी किया जाता है। लेकिन सवाल है कि शिक्षा, वित्तीय सेवाओं, राजनीतिक संवाद, अभिव्यक्ति की आजादी जैसे कई अधिकारों और रेल-विमान आरक्षण, ऐप आधारित कैब सर्विस, बैंकिंग आदि अनगिनत सेवाओं का लाभ बरास्ता इंटरनेट उठाने वाले लोगों को अगर किसी रोज नेट सेवाओं से महरूम कर दिया जाए, तो क्या होगा।
धारा 307 के तहत मिले विशेष दरजे को हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में पिछले साल अगस्त से इंटरनेट पर पाबंदी है। सरकार नहीं चाहती कि वहां इंटरनेट के जरिए किसी भी तरह से लोगों को बहकाने या भड़काने का कोई काम न हो सके। लेकिन इससे लोगों के छोटे-मोटे काम भी रुक गए हैं। हालात इतने विकट हैं कि पिछले दिनों (10 जनवरी, 2020 को) सुप्रीम कोर्ट को यह व्यवस्था देनी पड़ी कि इंटरनेट का इस्तेमाल संविधान के अनुच्छेद-19 के तहत मौलिक अधिकार है। इसलिए वहां हफ्ते भर में इस पाबंदी की समीक्षा की जाए और इसे हटाया जाए।
उल्लेखनीय है कि भारत समेत दुनिया के कई देशों में यह मांग भी उठती रही है कि इंटरनेट को मानवाधिकार माना जाए और सरकारें चाहें किसी भी कारण से मजबूर क्यों न हों, वे इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी न लगा सकें। लेकिन सवाल है कि सोशल मीडिया (इंटरनेट) से फैलने वाली अफवाहों से प्रेरित हिंसा और अराजकता को थामने के लिए अगर सरकार-प्रशासन इंटरनेट को बैन न करे तो क्या करे। प्रतिप्रश्न यह भी है कि किसी भी विरोध को दबाने के लिए इंटरनेट को रोकना एक दमनकारी उपाय है, लिहाजा, सरकारों को इससे परहेज करना चाहिए। यही नहीं, आज के साइबर कर्फ्यू सबसे ज्यादा नुकसान हर तरह के कारोबार को भी पहुंचा रहे हैं। बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक आज भारत इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने में दुनिया में सबसे आगे है, जहां बीते कुछ अरसे से सालाना सौ से ज्यादा डिजिटल किल स्विच दबाने की नौबत आने लगी है। इस मामले में बाकी मुल्क तो मीलों पीछे हैं। जैसे पड़ोसी पाकिस्तान (12 बार), इराक और यमन (7-7 बार), इथियोपिया (6 बार), बांग्लादेश (5 बार) और रूस में इस साल सिर्फ दो बार इसकी नौबत आई है। यूनेस्को और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स की ओर से जारी ‘साउथ एशिया प्रेस फीडम रिपोर्ट 2017-18’ पर नजर दौड़ाने से पता चलता है कि मई, 2017 से अप्रैल, 2018 के बीच की अवधि में पूरे दक्षिण एशिया में इंटरनेट शटडाउन की 97 घटनाएं रिकॉर्ड की गई, जिनमें 82 घटनाएं अकेले भारत में हुई। मई, 2018 में इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ने एक आकलन कर बताया है कि 2012 से 2017 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को इससे 3.04 अरब डॉलर की चपत लगी थी। नेटबंदी के दूरसंचार कंपनियों को ही हर घंटे तकरीबन 18 हजार डॉलर की आर्थिक नुकसान हो रहा है। एक आकलन वेबसाइट इंडियास्पेंड का भी है, जिसके अनुसार 2011 से 2017 तक भारत में तकरीबन 16,000 घंटों तक इंटरनेट शटडाउन रहा। बताया गया कि इस पाबंदी से देश को करीब 213.36 अरब रु पये का नुकसान हुआ।
जहां तक बात सोशल मीडिया के जरिए आतंकी घटनाओं और अफवाहों के प्रचार-प्रसार के पहलू की है, तो हर कोई इसका पक्ष लेना चाहेगा कि इन्हें किसी भी कीमत पर रोका जाए। लेकिन क्या यह मुमकिन नहीं है कि नेट-बंदी से बाहर जाकर किसी और तरीके से यह रोकथाम हो। असल में इसके कुछ उपाय तकनीक में ही नजर आते हैं। चेहरा पहचानने वाली अत्याधुनिक तकनीक-फेस रिक्गनाइजेशन ने यह सहूलियत अब पुलिस-प्रशासन को दे दी है कि उससे भीड़ में संदिग्धों की मौजूदगी को पहचाना जा सके। आईपी एड्रेस को डिकोड करके सोशल मीडिया से अफवाह फैलाने वालों की सीधी धरपकड़ हो सकती है। पुलिस इस उपाय को आजमाती भी रही है। लेकिन अपना काम हल्का करने के लिए पुलिस प्रशासन ये उपाय न आजमा कर सीधे इंटरनेट शटडाउन का सहारा लेता है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। इसके अलावा, सरकार-प्रशासन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर 1973 (सीआरपीसी), इंडियन टेलिग्राफ एक्ट 1885 और टेंपररी सस्पेंशन ऑफ टेलिकॉम सर्विसेज (पब्लिक इमज्रेसी या पब्लिक सेफ्टी) रूल्स, 2017 जैसे कानूनी प्रावधानों के तहत अफवाहों के प्रसार को रोकने की जो कोशिश करते हैं, उनका नकारात्मक पहलू यही है कि इससे सरकार के साथ समाज के रूप में हमारी परिपक्वता पर भी सवाल उठाने लगा है।
कहना न होगा कि हमारा समाज सूचनाओं, खबर के तथ्यों और अफवाहों में फर्क नहीं कर पाता है, लेकिन यह समझ विकसित करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। अगर एक आम नागरिक खुद के बल पर ऐसा नहीं कर पा रहा है, तो इसका जिम्मा सरकार को उठाना चाहिए।
| Tweet |