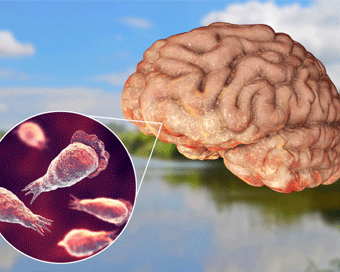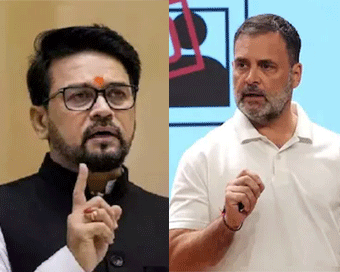नल से जल का पक्ष-विपक्ष
पाइप से पानी मिलने लगता है, तो लोग पानी की स्वावलंबी व्यवस्था के बारे में सोचना और करना..दोनों बंद कर देते हैं।
 नल से जल का पक्ष-विपक्ष |
पानी चाहे पाइप से पहुंचाया जाए अथवा नहरों से, जलापूर्ति के इस तंत्र की एक कमजोरी यह भी है कि जितना पानी उपयोग में नहीं आता, उससे ज्यादा बर्बाद हो जाता है। भारत की नहरी सिंचाई व्यवस्था के प्रभावी उपयोग का आंकड़ा मात्र 15 से 16 फीसद का है। पाइप के जरिए, मूल स्रोत से नल तक पानी पहुंचाने के रास्ते में 40 फीसद तक पानी रिसकर बह जाने का आंकड़ा है।
ऐसे में पूछा जा सकता है कि हर घर को नल से जल की राह में इतनी विषमताएं हैं तो क्या जरूरी है कि हम इस राह चलें? कम से कम मैदानी गांवों के मामलों में क्या यह उचित नहीं कि ग्राम्य पेयजल स्वावलंबन की दृष्टि को लक्ष्य बनाएं? भारत के सबसे कम वष्रा वाले जिले जैसलमेर की रामगढ़ तहसील के पानी इंतजाम को सामने रखकर दावा किया जा सकता है कि हर इलाके के सिर पर पर्याप्त पानी बरसता है; यदि हर इलाका अपने सिर पर बरसे पानी को संजो ले, तो ही उसके पीने के पानी का इंतजाम हो जाएगा। यह एक ऐसा बिंदु है, जिस पर आकर पाइप से पानी पहुंचाने के पक्ष और प्रतिपक्ष की बीच समझौता संभव है बशर्ते एक शर्त मान ली जाए।
तय हो कि अपने नल में अपना पानी ही आएगा अर्थात नल भी अपना, पाइप भी अपनी, आपूर्ति का मूल स्रोत भी अपना तथा प्रबंधन का दायित्व भी अपना ही हो। स्रोत दूसरे का, नल अपना; यह नहीं चलेगा। स्रोत का प्रबंधन उसी के हाथ हो, जिसे उस नल से पानी दिया जाता है। दूसरे इलाके के स्रोत से पानी खींचकर लाने पर पूर्ण प्रतिबंध हो। आप पूछ सकते हैं कि क्या यह व्यावहारिक है? हां, यह व्यावहारिक भी है, लीकप्रूफ भी और संभव भी; क्योंकि भारत का पेयजल-संकट पर्यावरणीय कम, गवन्रेस से जुड़ा संकट ज्यादा है।
भारत के ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में पेयजल का मुख्य स्रोत अभी भी भूजल है। ‘जिसकी भूमि, उसका जल’-भारत में भूजल की मलकियत की वर्तमान कानूनी स्थिति यही है। स्थानीय सतही जल-स्रोत सामान्यतया निजी, सामुदायिक या पंचायती होते हैं। शेष स्रोतों के मामलों में सरकारें ट्रस्टी भर हैं, मालिक नहीं। इस जलाधिकार व दायित्व के मद्देनजर गवन्रेस का तकाजा है कि क्यों नहीं कम से कम स्थानीय भूजल प्रबंधन के दायित्व व अधिकार उसे सौंप दिए जाएं, स्थानीय जल-संचयन स्रोत जिनके नाम से दर्ज हैं। लाइसेंसिंग, प्रतिबंध अथवा पानी को समवर्ती सूची में लाने से भूजल का दुरु पयोग रु केगा नहीं; बल्कि पानी प्रबंधन में गिरावट और भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। अत: भूजल का दुरु पयोग रोकने के लिए क्यों न उपभोक्ता भू-स्वामियों को बाध्य किया जाए कि वे जितना पानी धरती से निकालें, कम से कम उतना और वैसी गुणवत्ता का पानी धरती को वापस लौटाएं? कृषि और उद्योग, पानी के दो सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। क्यों नहीं सर्वप्रथम इन्हीं से शुरुआत हो? इनमें भी सर्वप्रथम रेल नीर जैसे पानी से पैसा कमाने वाले उद्योगों से? रेलवे, स्कूल, सरकारी इमारतों तथा चारदीवारी वाले घरेलू-व्यावसायिक परिसरों के पास भी काफी भूमि है। दूसरों के हिस्से का पानी खींचकर पीने वाले नगर भी कम नहीं। पानी के लेन-देन में संतुलन का कायदा इन पर भी लागू हो। सतही तथा भू-जल स्रोत का दुरुपयोग नियंत्रित होगा, तभी हर घर को नल से जल सुनिश्चित हो पाएगा।
| Tweet |