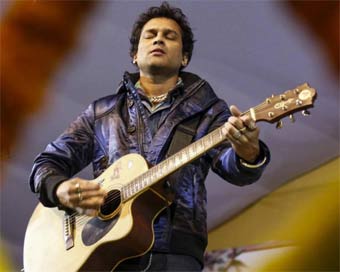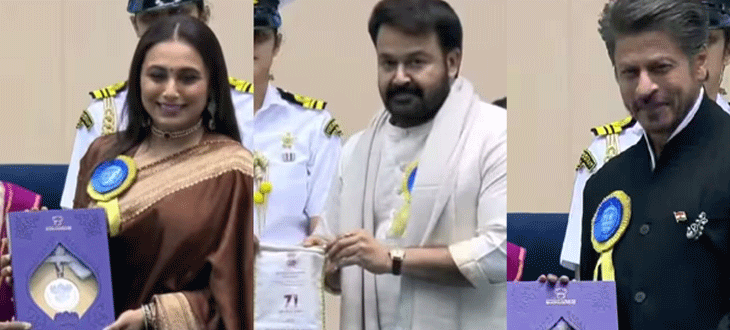भारत-जापान : बड़े फलक के साझीदार
भारत और जापान इतिहास और संस्कृति के जीवंत रिश्तों, विश्वासों और जरूरतों की अन्योन्याश्रिताओं को पोषित करते हुए अब वैश्विक विकास तथा सामरिक-रणनीतिक साझेदारी की ओर बढ़ते दिख रहे हैं।
 भारत-जापान : बड़े फलक के साझीदार |
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्ट्रांग इंडिया-स्ट्रांग जापान के जरिए आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो शिंजो आबे मोदी के भरोसे के सहारे भारत के साथ ताल-कदम मिलाने की। लेकिन क्या इस दोस्ती से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत-जापान मिलकर केप ऑफ गुड होप से लेकर भारत-प्रशांत की व्यापक परिधियों तक कॉम्प्रीहेंसिव साझेदारी का निर्माण करने में सफल हो पाएंगे? सवाल यह भी है कि क्या भारत-जापान वैिक फलक पर ऐसे प्रतियोगी विकास की बुनियाद रख पाएंगे जो चीन की वैिक इंफ्रा-इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी (विशेषकर वन बेल्ट वन रूट) को चुनौती दे सके?
कभी-कभी लगता है कि जापान चीन के विरुद्ध नई रणनीति पर आगे बढ़ने में भारत पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रहा है, क्या अब आगे वह ऐसा करने में समर्थ होगा? जब एशिया रणनीतिक पुनर्रचना (स्ट्रैटेजिक रिशेपिंग) से गुजर रहा हो और चीन इसमें ऐसे स्थायी खांचों का निर्माण करने के लिए हर संभव यत्न कर रहा हो जिनमें वह अपने आप को एक ग्लोबल लीडर के रूप में फिट कर सके, क्या जापान और भारत मिलकर उसे पीछे धकेल पाएंगे? भारत-जापान-अमेरिका त्रिभुज या भारत-जापान-अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया चतुभरुज (या रणनीति की तकनीकी शब्दावली में कहें तो नई दिल्ली-टोक्यो-वाशिंगटन धुरी या नई दिल्ली-टोक्यो-वाशिंगटन-कैनबरा धुरी) की जो कवायदें चल रही हैं, वे उन स्थितियों में सफल हो पाएंगी जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक अनिश्चित, असंभ्रांत एवं प्रतिक्रियावादी विदेश नीति को प्रश्रय दे रहे हों?
मोदी 29 अक्टूबर को टोक्यो में शिंजो आबे से 12वीं बार और शिखर सम्मेलन में 5वीं बार मिले। टोक्यो में मोदी ने अपने संबोधन के जरिए दुनिया को बताने का प्रयास किया कि भारत-जापान अफ्रीका और दुनिया के अन्य हिस्सों में ठोस विकास के प्रयास में संयुक्त तौर पर निवेश करना चाहते हैं। हालांकि इस सम्बंध में ¨शजो आबे 2016 में ही घोषणा कर चुके हैं। जहां तक द्विपक्षीय संबंधों की बात है तो भारत के लिए जापान इस समय काफी अहम दिखाई दे रहा है। इसके कई कारण हैं। एक तो यह कि जापान तकनीक के क्षेत्र में एशिया का सबसे एडवांस देश है, और भारत को तकनीकी उन्नयन एवं विकास की जरूरत है। दूसरा यह कि भारत-प्रशांत क्षेत्र में जो समीकरण बन रहे हैं, उनमें भारत को अपने पक्ष में संतुलन बनाए रखना है, तो जापान के साथ समग्र एवं अन्योन्याश्रितता की साझेदारी करनी होगी। फिर इसे थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस आदि तक विस्तार देना होगा। कारण यह है कि इस क्षेत्र में अब अनिश्चितता और गैर-संभ्रांतता वाली प्रतियोगिता अधिक दिखने लगी है। उदाहरण के तौर पर चीन अपने आर्थिक आकार के कारण अपनी सैन्य क्षमता का विस्तार कर रहा है।
दूसरी तरफ रूस इस समय ‘पीवोट टू एशिया’ पर काम कर रहा है। उसका मुख्य फोकस है पूर्वी एशिया में रक्षा सहयोग के जरिए स्थायी पैठ सुनिश्चित करना। ऐसे में रूस और चीन बेहतर साझेदारी निर्मित कर ले जाते हैं, जो अभी संभव नहीं दिखाई देती, तो फिर उसकी काट ढूंढ़ना मुश्किल हो जाएगी। तीसरा पक्ष ऑस्ट्रेलिया है, जिसकी दिशा अभी स्पष्ट नहीं है क्योंकि वह चीन के खिलाफ जाने का निर्णायक मनोविज्ञान विकसित नहीं कर पाया है। अंतिम और सबसे निर्णायक पक्ष अमेरिका है, जिसकी विदेश नीति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की असंभ्रांत, अनिश्चित और दिशाहीन सक्रियता का शिकार है, इसलिए उससे स्थायी भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि भारत से पहले ही अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक रणनीतिक चतुभरुज का निर्माण कर चुका है, जिसका मुक्त उद्देश्य तो कनेक्टिविटी एवं मैरीटाइम सिक्योरिटी है, लेकिन इसके पीछे अमेरिका और जापान का एक छुपा हुआ उद्देश्य चीनी विस्तार को रोकना भी है, लेकिन ट्रंपियन युग में इस पर किसी निष्कर्ष तक पहुंचाना मुश्किल होगा। लेकिन भारत के लिए जरूरी है कि हिन्द महासागर में अपनी स्थिति का आकलन कर जापानी सहयोग से सॉफ्ट और स्ट्रैटेजिक पॉवर का विस्तार करे। अनमेन्ड एरियल विहीकल्स, रोबोटिक्स आदि क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाओं को व्यावहारिक आकार दे।
रही बात जापान की तो चीन दक्षिण चीन सागर में एकाधिकार चाहता है। जापान की खिल्ली उड़ाने के अंदाज में वह उसे एक स्खलित राष्ट्र की संज्ञा तक दे जाता है। ध्यान रहे कि उसने नये हवाई क्षेत्र प्रतिबंध को लागू करने का निर्णय लिया है, जिसके दायरे में सेनकाकू (जापानी नाम) भी आता है, या कहें तो वह स्प्राटली द्वीप का विवाद (वियतनाम, ताइवान के साथ) पैदा कर रहा है। चीन का यह मनोविज्ञान आबे को ‘पोस्ट-वार पेसिफिस्ट संविधान’ में संशोधन कर नई रक्षा नीति बनाने की जरूरत भी महसूस करा रहा है। संभव है कि जापान अमेरिकी छतरी से बाहर आकर अपना सुरक्षा कवच स्वयं तैयार करना चाहे। ऐसे में उसे भारत की और अधिक जरूरत होगी। यह भी देखना होगा कि चीन के एक महाशक्ति के रूप सामने आते ही शक्ति संतुलन का केंद्र वाशिंगटन से बीजिंग कैसे खिसकता है, या शी जिनपिंग इस तरह का प्रयास किस प्रकार करते हैं। इन्हीं रणनीतियों, सक्रियताओं एवं संयोजनों के अनुसार नई दिल्ली-टोक्यो के बीच भी नये संयोजनों की जरूरत होगी। संभवत: दोनों देशों के बीच ‘टू प्लस टू डायलॉग’ पर सहमति इन्हीं उद्विकासों का परिणाम है। भारत और जापान सुरक्षा सहयोग में ‘टू प्लस टू डायलॉग’, द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय मैरीटाइम एक्सरसाइज तथा हथियारों की बिक्री शामिल होगी।
उल्लेखनीय है कि सब-कैबिनेट/सीनियर ऑफिसियल्स के स्तर पर ‘टू प्लस टू डायलॉग’ के लिए नई दिल्ली और टोक्यो के बीच सहमति बनाने का प्रयास 2009 में ही शुरू हो गया था लेकिन अंतिम निष्कर्ष तक अब पहुंच पाए। इस देरी के लिए संभवत: जापान के कुछ संकोच और हिचकिचाहटें जिम्मेदार रहीं। फिलहाल, दोनों देशों की जियो-पॉलिटिकल रणनीति में काफी समानता है। मोदी की ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ और आबे की ‘फ्रीएंड ओपन इंडो पैसिफिक पॉलिसी’ निर्णायक बॉण्ड बनाती नजर आ रही है। देखना है कि मोदी की स्मार्ट डिप्लोमेसी और शिंजो का मोदी फेथ दोनों देशों के रिश्तों को किन सिरों तक विस्तार दे पाता है।
| Tweet |