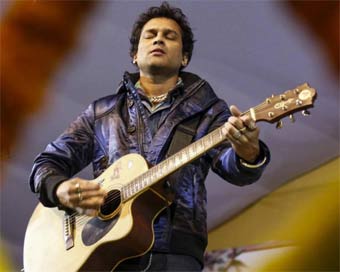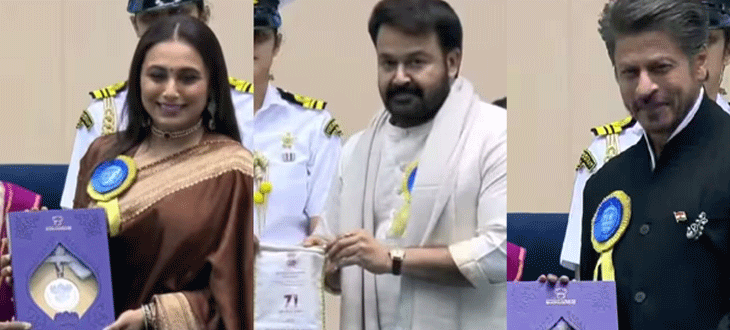अर्थव्यवस्था : संभालने के कठोर उपाय
जब बीमारी इलाज के बावजूद लगातार बढ़ती जाए तो इसके दो ही कारण हो सकते हैं. एक तो यह कि बीमारी बहुत गंभीर है अथवा इलाज गंभीरता से नहीं हो रहा.
 अर्थव्यवस्था : संभालने के कठोर उपाय |
.jpg) दुर्भाग्य से भारत में सरकारी बैंकों के संदर्भ में ये दोनों बात लागू होती हैं. इलाज मर्ज को गहराई से पहचान लेने की अपेक्षा लक्षणों पर आधारित है. रिजर्व बैंक वह विशेषज्ञ है, जिसकी जिम्मेदारी है और वही संपूर्ण रूप से फेल नजर आ रहा है.
दुर्भाग्य से भारत में सरकारी बैंकों के संदर्भ में ये दोनों बात लागू होती हैं. इलाज मर्ज को गहराई से पहचान लेने की अपेक्षा लक्षणों पर आधारित है. रिजर्व बैंक वह विशेषज्ञ है, जिसकी जिम्मेदारी है और वही संपूर्ण रूप से फेल नजर आ रहा है.
वर्तमान बैंकिंग परिदृश्य बहुत धूमिल है और अभी तक सरकार ने केंद्रीय बैंक की कोई खबर ही नहीं ली है. बैंकों के खातों की जांच पर करोड़ों रुपये किस बात के खर्च होते हैं? कोई पूछ ही नहीं रहा है. केंद्रीय बैंक पहले एनपीए मामले में अपनी जवाबदेही के प्रति लापरवाह रहा फिर नोटबंदी के दौरान घोर अव्यवस्था से मानों उसे कोई लेना-देना नहीं हो और अब फ्रॉड के प्रति सतर्कता किसका दायित्व है? इसका आम जनता को सही-सही पता नहीं. प्रथमदृष्टया केंद्रीय बैंक की समस्त जिम्मेदारी है. मगर सुख-सुविधाओं से संपन्न महाराज स्टाइल की अच्छी साहब बहादुर वाली नौकरी करते नौकरशाह मस्त हैं. आज सरकारी बैंकों की दुर्गति के लिए रिजर्व बैंक के दायित्व को समझना होगा और अवश्य ही शीर्ष पद पर आसीन अधिकारियों को कुछ-न-कुछ ऐसा करना चाहिए, जिसे लगे कि वह अपने कर्तव्यों के प्रति संवेदनशील हैं. मगर इधर एक-दूसरे पर आरोप मढ़ने से अधिक कुछ नहीं हो रहा.
हमारी अर्थव्यवस्था पिछले दो-तीन साल से लगातार मथी जा रही है. इससे अभी तक विष ही विष उत्पन्न हुआ है. लगता है धन-संपदा के अमृत का पान बहुत पहले ही हो चुका है. इस विष का भान लगातर बढ़ते जा रहे एनपीए में तो नजर आ ही रहा था, जो कि किसी प्रकार भी काबू में आने का नाम ही नहीं ले रहा था. मगर पीएनबी में एकदम से इतने बड़े घोटाले के उजागर होने से सरकार अत्यधिक सशंकित हो गई. कुछ विशेषज्ञों ने तो सरकारी बैंकों को प्राईवेट किए जाने की वकालत भी करनी शुरू कर दी. जब हर तरह से सरकारी बैंकों को मर्ज पकड़ में नहीं आ पाया तो सरकार ने अपने तुरूप के पत्ते को यानी सीबीआई को प्रयोग में लाने का मन बनाया है.
इससे पूर्व सीमित दायरे में ही यह कार्य सीबीआई के द्वारा किया जाता था. मगर अब उसका रोल अधिक होने वाला है. इधर, सीबीआई स्टाफ एवं विशेषज्ञता की कमी से पहले ही त्रस्त है और अब मानो उसे एनपीए से निबटने के एक रामबाण के रूप में सरकार देख रही है. इस तथ्य में तनिक भी संदेह नहीं कि सीबीआई एक बेहतरीन संस्था है और उसकी सहायता से काफी कुछ समस्या का समाधान अवश्य हो जाएगा. सरकार के सब्र की परीक्षा का यह आखिरी इम्तहान है. उम्मीद है इस परीक्षा में सरकार खरी उतरेगी. परंतु दूसरी तरफ इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ऋण देने में अब बैंक अधिकारियों के मन में एक भय व्याप्त होगा. बैंक ऋणों की मांग में कमी लगातार बनी हुई है और सरकार के इस कदम से उसमें और अधिक उदासीनता का खतरा है. इसका एक मात्र उपाय वैकल्पिक वित्त को उपलब्ध कराना ही नजर आ रहा है. यह दो तरह से उपलब्ध की जा सकती है.
एक तो कॉर्पोरेट बांड मार्केट द्वारा और दूसरा इक्विटी मार्केट में निर्गम द्वारा. यह तरीका बैंकों को प्राइवेट सेक्टर में देने की अपेक्षा उनके बिजनेस को प्राइवेट हाथों में देने जैसा है. यही एकमात्र रास्ता नजर आ रहा है, जो भविष्य में वित्तीय व्यवस्था को एक नया रास्ता दिखा सकता है. दूसरी तरफ, आर्थिक अपराधों के मामलों में अभियुक्तों के ऊपर शिंकजा कसने के लिए कैबिनेट ने ‘भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल 2018’ को मंजूरी दे दी है. इस बिल की सारी बातों को अभी सार्वजानिक नहीं किया गया है, मगर इतना इंगित किया गया है कि आर्थिक अपराध कर के विदेश भागने वालों को अदालत में दोषी ठहराए बिना भी उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान बिल में है.
इस बिल के साथ ही लापरवाह और धोखाधड़ी में लिप्त पाए जाने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर नकेल कसने के लिए ‘राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिग प्राधिकरण’ को भी मंजूरी दी गई है. विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश था, जहां ऑडिटर्स को कंट्रोल करने के लिए ‘सेल्फ रेगुलेटरी’ व्यवस्था थी. 2013 के ‘कंपनी लॉ’ में प्रस्तावित एक प्राधिकरण की व्यवस्था को भी लगभग पांच साल बाद दिन की रोशनी दिखी. यह सब प्रतिक्रियाएं पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले से तेज हुई. खराब घटनाएं अच्छे कानूनों को जन्म देती ही हैं. कुछ-न-कुछ सकारात्मक असर तो इस घोटाले का भी होगा. अब सरकार को मजबूती दिखने का एक मौका मिला है. अब कोई उस पर कठोर होने का आरोप नहीं लगा सकता. इस बात की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि सीबीआई को बैंकों के फ्रॉड की जांच में सक्रियता से सहभागिता होने से ऋण उपलब्धता में कोई कमी आएगी.
इक्कीस में से ग्यारह बैंक पहले से ही एक अलग सूची में चल रहे हैं और पूरी तरह से ऋण देने के पात्र नहीं हैं. मजेदार बात है कि इस सूची में पीएनबी नहीं था. सरकारी बैंकों के शेयर मूल्यों में लगातार गिरावट की वजह से निवेशकों का भारी नुकसान हुआ है. उसकी भरपाई तभी हो सकेगी जब कुछ ठोस एवं कठोर निर्णय लिए जाएं ताकि विदेशी संस्थागत निवेशकों का विश्वास लौटे. अभी इसकी कोई सम्भावना नजर नहीं आ रही है. विदेशी बाजारों में घबराहट का माहौल इस आग में घी का काम कर रहा है.
यह एक मुश्किल भरा समय है परन्तु एक आशा की किरण जीडीपी ग्रोथ में नजर आई है और एक दिन पहले अमेरिका द्वारा स्टील एवं एल्युमीनियम के आयात पर ड्यूटी लगाए जाने का निर्णय एक ट्रेड वार को जन्म देता प्रतीत हो रहा है. देखना होगा कि भारत अपने वर्तमान बैंकिंग संकट के साथ-साथ इस विश्व व्यापार संबंधी उथल-पुथल को किस प्रकार अपने पक्ष में कर सकता है? घरेलू और वैश्विक मोर्चे पर ही नई चुनौतियां नये अवसरों को जन्म देंगी और यह संतोष की बात है कि राष्ट्र दो झटकों-एक नोटबंदी और दूसरा जीएसटी-के ऑपरेशनल अवरोधों से सही समय पर उबर रहा है. भविष्य बड़ा अनिश्चित है, किंतु हमारे पास अब खोने के लिए कुछ अधिक नहीं है. शायद ये सब हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा ही साबित होगा क्योंकि स्थापित मूल्यों के ध्वस्त होने से विकासशील देशों को गति ही मिलती है.
| Tweet |