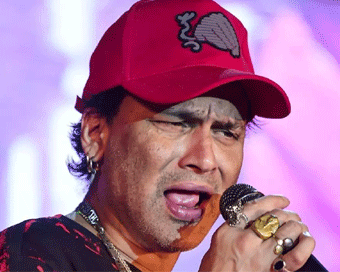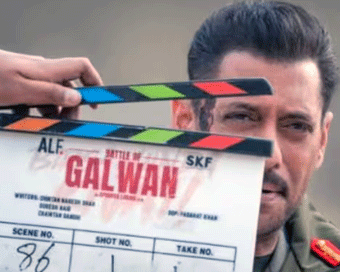मानसिक शांति भी चाहिए
महंगाई के दौर में अर्थोपार्जन के लिए दिन-प्रतिदिन बढ़ते दबाव और बेलगाम (और कभी-कभी आधारहीन! ) होती महत्त्वाकांक्षाओं को अंजाम देने की कोशिशों के चलते हम सभी बिना विचार किए अधिकाधिक संग्रह के मुरीद बनते जा रहे हैं.
 मानसिक शांति भी चाहिए |
.jpg) आवश्यकताओं की जगह अब इच्छाओं का ज़ोर है जिनमें बहुत सारी ऐसी भी होती हैं, जिनका व्यक्ति के वास्तविक जीवन में खास महत्त्व भी नहीं होता. हां, प्रतिस्पर्धा के युग में दूसरों के तुलना में हेठे न दिखने की चिंता जानी अनजानी-दिशाओं में मन को भटकाती रहती है ताकि हम ‘पोसेस’ करने या अपना अधिकार जमाने की क्षमता का प्रदर्शन कर सकें. इस माहौल में तनाव या स्ट्रेस सबकी मुसीबत का कारण बन रहा है और कई मानसिक और शारीरिक बीमारियों को पैदा कर रहा है. तनाव पैदा करने वाली परिस्थितियां व्यक्ति सापेक्ष होती है और इस कारण उनमें काफ़ी अंतरवैयक्तिक अन्तर भी पाया जाता है परंतु उनका केंद्र प्राय: व्यक्ति की खुद की अपनी समझ ही हुआ करती है, जो परिस्थिति विशेष को चुनौती, अवसर या खतरा किसी भी रूप में निरूपित करती है.
आवश्यकताओं की जगह अब इच्छाओं का ज़ोर है जिनमें बहुत सारी ऐसी भी होती हैं, जिनका व्यक्ति के वास्तविक जीवन में खास महत्त्व भी नहीं होता. हां, प्रतिस्पर्धा के युग में दूसरों के तुलना में हेठे न दिखने की चिंता जानी अनजानी-दिशाओं में मन को भटकाती रहती है ताकि हम ‘पोसेस’ करने या अपना अधिकार जमाने की क्षमता का प्रदर्शन कर सकें. इस माहौल में तनाव या स्ट्रेस सबकी मुसीबत का कारण बन रहा है और कई मानसिक और शारीरिक बीमारियों को पैदा कर रहा है. तनाव पैदा करने वाली परिस्थितियां व्यक्ति सापेक्ष होती है और इस कारण उनमें काफ़ी अंतरवैयक्तिक अन्तर भी पाया जाता है परंतु उनका केंद्र प्राय: व्यक्ति की खुद की अपनी समझ ही हुआ करती है, जो परिस्थिति विशेष को चुनौती, अवसर या खतरा किसी भी रूप में निरूपित करती है.
मानसिक तौर पर हम अपने साथ अपना निजी इतिहास भी लिए चलते हैं और हमारा वर्तमान अपने अतीत और भविष्य के बीच की खींचतान के लिए एक अखाड़ा जैसा बनता जाता है. मानसिक तौर पर बिंबों और प्रतीकों के रूप में पुराने अनुभवों की स्मृतियां और आगामी संभावनाओं की कल्पना हमारे लिए हर क्षण कोई न कोई अधूरी और अपरिपक्व परियोजनाएं (प्रोजेक्ट) छोड़ रखती हैं. इन परियोजनाओं का प्रत्यक्ष या परोक्ष नायक व्यक्ति स्वयं होता है क्योंकि हमारी दुनिया स्व को केंद्र में रख कर ही रची जाती है. साथ ही अपने स्व (सेल्फ़) के चटख रंग में रंगे चश्मे से देखने के हम इतने आदी हो चुके रहते हैं कि उसके अलावा कुछ और सूझता ही नहीं है. इसी से होकर या छन कर सूचनाएं हम तक पहुंचती हैं और इसी से पूछ कर और इसी की निगरानी में हम दूसरों और खुद के साथ बर्ताव भी करते हैं. इस तरह अच्छी-बुरी सारी हलचलों और उलझनों के आरकेस्ट्रा से सुमधुर संगीत या कर्णकटु कोलाहल क्या निकलेगा इसका दारोमदार स्व की अपनी अवधारणा पर ही टिका होता है.
सूचनाओं के संग्रह, विश्लेषण, कार्य के लिए दिशा-निर्देश और उन्हें करने की प्रेरणा सब कुछ स्व के ही ज़िम्मे होता है. इस गहमागहमी में उसे विश्राम नहीं मिलता और उसकी ऊर्जा कम होती जाती है. चूंकि दुनिया में स्व ही सबसे •यादा प्यारा होता है. हम उसकी हर बात रखने को बेताब रहते हैं. हमारी पुरज़ोर कोशिश रहती है कि हमारा स्व सबसे आगे और सबके ऊपर रहे (चाहे जैसे!). आत्मलीनता के कारण उसके निर्णय हमेशा ठीक नहीं होते. स्व का ताना-बाना कुछ इस तरह बुना जाता है कि उसकी खामियां हमें नज़र ही नहीं आतीं. स्व को विजयी बनाए रखने के लिए खुद को अच्छा साबित करने के साथ दूसरों को नीचा दिखाने की भी कोशिश की जाती है. वस्तुत: वह हर तरीका हम अपनाते हैं जिससे हम दूसरों से बीस साबित हो सकें. आत्म-मुग्ध हुए जाते हम सब अपने लिए एक सुगठित आख्यान रचते हैं. इसके साथ ही हम आख्यान के कथानक को सही साबित करने की कोशिश भी करते रहते हैं, जिनसे नए आख्यानों की सृष्टि होती है.
हम अपनी ज़रूरतें और महत्त्वाकांक्षाएं भी अपने सामाजिक परिवेश से ही प्राप्त करते हैं. हम ज़िंदगी में नित्य प्रति नए-नए विचार-परिवेश की दुनिया में कदम रखते हैं. आज बड़ी सघनता और तीव्रता के साथ मीडिया हमारी आत्म-छवि को गढ़ रहा है. अब मीडिया के मॉडल हमें बताते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए और कैसे व्यवहार करना चाहिए. वे हमारे संवेगों और भावनाओं पर भी क़ब्ज़ा जमाते जा रहे हैं. संवेगों की शब्दावली, उनकी अभिव्यक्ति और उनके विविध रूप अब मीडिया में ढल रहे हैं. इसका कारण यह भी है कि भावनाओं को उभार कर मीडिया उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ाते हुए बाजार को सशक्त बनाता है. 2437 चलने वाले टीवी चैनलों की संख्या बढ़ती जा रही है और उनके साथ ही तरह-तरह की सूचनाओं का भंडार बढ़ता जा रहा है. व्यापक स्तर पर देखें तो आर्थिक उदारीकरण के साथ बाज़ार तंत्र का शिंकजा हम पर कसता जा रहा है. हम अपने निर्णय की स्वतंत्रता खोते जा रहे हैं क्योंकि विकल्पों पर बाजार की बंदिश लगी है. अब अपने लिए कपड़े सिलवाते नहीं हैं बल्कि सिले-सिलाए कपड़ों में अपने को फि़ट करते हैं.
| Tweet |