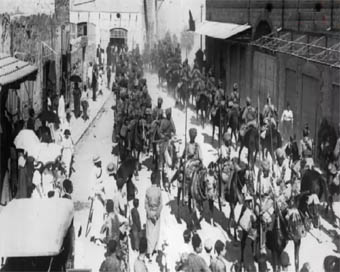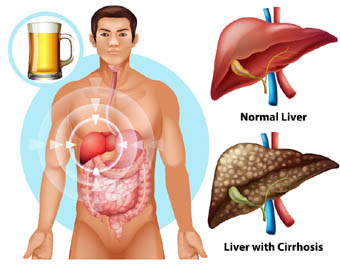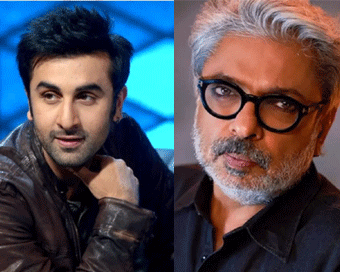प्रसंगवश : शिक्षा परिसर में हिंसा
शिक्षा अर्थात पढ़ाई-लिखाई की दुनिया की एक छवि मन में बनी-बसी है. वह एक सक्रिय, सहज और सृजनशील दुनिया है, जिसमें उत्सुकता, जिज्ञासा और प्रयोग की गुंजाइश होती है.
 प्रसंगवश : शिक्षा परिसर में हिंसा |
.jpg) संयुक्त परिवार टूट रहे हैं. मां-पिता दोनों कामकाजी हो रहे हैं. फलत: अब बड़ी कम उम्र में ही क्रेच, प्ले स्कूल और केजी में पढ़ने के लिए बच्चों को परिवार से दूर स्कूल में भेजने का चलन (और मजबूरी) बढ़ रही है.
संयुक्त परिवार टूट रहे हैं. मां-पिता दोनों कामकाजी हो रहे हैं. फलत: अब बड़ी कम उम्र में ही क्रेच, प्ले स्कूल और केजी में पढ़ने के लिए बच्चों को परिवार से दूर स्कूल में भेजने का चलन (और मजबूरी) बढ़ रही है.
पिछले दिनों रियान इंटरनेशनल स्कूल, गुड़गांव में एक छोटे बच्चे प्रद्युमन की हत्या के मामले ने सबका दिल दहला दिया. इस मामले में अब तक जो खुलासे हुए हैं, वे खतरनाक हैं. खास तौर पर सीबीआई द्वारा प्रस्तुत विवरण कि उसी विद्यालय के ग्यारहवीं कक्षा के एक लड़के ने उम्र में अपने से छोटे एक लड़के की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी कि वह खुद पढ़ाई में कमजोर था, और उस दिन की स्कूली परीक्षा के लिए तैयार न होने के कारण परीक्षा को टलवाना चाहता था. यह सही है तो परीक्षा के भय और उससे जुड़ी मानसिकता कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका उदाहरण है. स्कूलों में यह वाकया और इससे मिलते-जुलते स्कूली हिंसा के दूसरे मामले हमारे सामने कई सवाल खड़े कर रहे हैं, और पूरी शिक्षा-व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं.
यह भी याद आता है कि हर साल पढ़ाई के अंत में परीक्षा में असफलता की पीड़ा न झेलने वाले अनेक छात्र खुदकुशी भी करने लगते हैं यानी परीक्षा से भयभीत हो कर दूसरे की जान ली जा सकती है, या अपनी जान दी जा सकती है. इस तरह की घटनाएं सवाल कर रही हैं कि क्या इसी तरह की रुग्ण मानसिकता के लिए विद्यालय बने हैं? विद्यालय में मिलने वाला ज्ञान तो मुक्त करने वाला और जीवन का उत्सव मनाने वाला माना गया था पर यह सब तो विलक्षण मानसिक बंधन बन रहा है, जिसमें छात्र भविष्य को छोड़ अतीत से बंध कर का अपना अस्तित्व ही दांव पर लगने लगा है. परीक्षा जीवन-मरण का प्रश्न होती जा रही है. हो भी क्यों न? आम आदमी के लिए हाथ की लकीरों की तरह परीक्षा के अंक ही भाग्य-विधाता जो बन रहे हैं. आज परीक्षा ज्ञान का मूल्यांकन से अधिक छंटनी करने का माध्यम बनती जा रही है.
याद रहे एक संस्था का रूप देकर विद्यालय इसलिए बनाए गए कि स्कूल की सीमा में आकर बाहरी दुनिया में छाए हुए ऊंच-नीच और धनी-गरीब जैसे वर्ग-भेद को भुला कर बच्चों को एक समता-समरसता वाले वातावरण में जीने का अवसर मिल सकेगा. यह आशा भी थी कि बच्चों के अनगढ़ मानस को गढ़ते हुए स्कूल सकारात्मक मानव मूल्यों के बीज बोएगा. बहुतों के मन में यह विश्वास भी पनप रहा था कि शिक्षा का विकास करते हुए हम चरित्र और आचरण की दृष्टि से एक सबल समाज की नींव रख सकेंगे. ऐसा इसलिए भी सोचा गया कि यहां की वर्तमान आधुनिक शिक्षा अंग्रेजों की देन है, और उसका सीमित लक्ष्य स्वतंत्र चिंतन की जगह अंग्रेजों की योजना के अनुकूल एक सरकारी अमला खड़ा करना और सोच-विचार का पाश्चात्य नजरिया स्थापित करना था. परिणाम है ऐसे अयोग्य, अनुपयोगी प्रमाणपत्रधारी लोगों की बड़ी जमात तैयार होती गई जो कौशल और क्षमता की दृष्टि से अपेक्षित स्तर के नहीं होने के कारण बेरोजगार हैं.
शिक्षा का व्यावहारिक अर्थ अब परीक्षा में अच्छे अंक पाने तक सिमट गया है. वही सफलता का द्योतक हो चला है, जिसकी चुनौती प्राय: रट कर निपटने की नसीहत दी जाती है. परीक्षा में प्रश्न भी वस्तुनिष्ठ आते हैं, जिनमें पहले से तयशुदा चार उत्तर रहते हैं, जिनमें से एक सही होता है. इसमें सोचने या सृजनशील होने की बहुत कम जगह बचती है. ऐसे में अच्छा अध्यापक वही होगा जो इस पण्राली के लिए छात्रों को तैयार करे. अध्यापक स्वयं इसी पद्धति से तैयार हुए रहते हैं. इस माहौल में शिक्षा से व्यक्ति के ज्ञान और व्यवहार में श्रेष्ठता की दिशा में परिवर्तन लाने की जो आकांक्षा थी, वह धूमिल हो रही है. अभिभावक, अध्यापक, सरकार और प्रशासन अर्थात वे सभी जो शिक्षा से किसी न किसी तरह जुड़े हैं, को सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और क्या किया जाना चाहिए? स्कूली हिंसा की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं. भारत के लिए यह इसलिए और भी चिंताजनक है कि यह युवा देश होता जा रहा है. पैसठ प्रतिशत जनसंख्या पैतीस साल की उम्र के नीचे है. इस मानव पूंजी को लेकर देश युवा-वर्ग को शक्ति के रूप देखना चाहता है, तो उसके लिए शिक्षा के पावन परिसर को कुंठा और अविश्वास से उबारना होगा. इसके लिए समुचित तैयारी भी करनी होगी.
| Tweet |