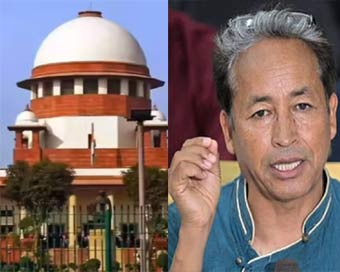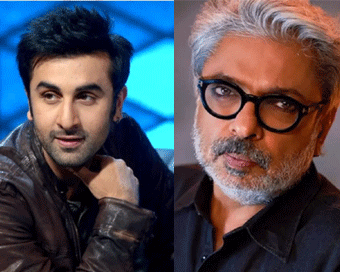प्रसंगवश : साहित्य-समाज के रिश्ते
शिक्षा की भाषा, दैनंदिन कार्यों में प्रयोग की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में हिंदी को उसका जायज गौरव दिलाने के लिए अनेक प्रबुद्ध हिंदीसेवी और हितैषी चिंतित हैं, कई तरह के प्रयास कर रहे हैं, जनमत तैयार कर रहे हैं.
 प्रसंगवश : साहित्य-समाज के रिश्ते |
समकालीन साहित्य की युग-चेतना पर नजर दौड़ाएं तो दिखता है कि समाज में व्याप्त विभिन्न विसंगतियों पर प्रहार करने और विद्रूपताओं को उघारने के लिए साहित्य तत्पर है. इस काम को आगे बढ़ाने के लिए स्त्री-विमर्श, दलित-विमर्श, आदिवासी विमर्श जैसे अनेक विमशरे के माध्यम से हस्तक्षेप किया जा रहा है. इन सबमें सामजिक न्याय की गुहार लगाई जा रही है ताकि अवसरों की समानता और समानता के मूल्यों को स्थापित किया जा सके.
संचार की तकनीक और मीडिया के जाल ने हमारे ऐन्द्रिक अनुभव की दुनिया का विराट फैलाव दिया है. ऐसे में जब इस सप्ताह ‘दद्दा’ यानी राष्ट्रकवि श्रद्धेय मैथिलीशरण गुप्त की एक सौ इकतीसवीं जन्मतिथि पड़ी तो उनके अवदान का भी स्मरण आया. इसलिए भी कि उनके सम्मुख भी एक साहित्यकार के रूप में अंग्रेजों के उपनिवेश बने हुए परतंत्र भारत की मुक्ति का प्रश्न खड़ा हुआ था. उल्लेखनीय है कि गुप्त जी का समय यानी बीसवीं सदी के आरंभिक वर्ष आज की प्रचलित खड़ी बोली हिंदी के लिए भी आरंभिक काल था.
भारतेन्दु युग में शुरु आत हो चुकी थी पर हिंदी का नया उभरता रूप अभी भी ठीक से अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका था. भाषा का प्रयोग पूरी तरह से रवां नहीं हो पाया था. इस नई चाल की हिंदी के महनीय शिल्पी ‘सरस्वती’ पत्रिका के संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गुप्त जी को ब्रज भाषा की जगह खड़ी बोली हिंदी में काव्य-रचना की सलाह दी और इस दिशा में प्रोत्साहित किया. एक आस्तिक वैष्णव परिवार में जन्मे और चिरगांव की ग्रामीण पृष्ठभूमि में पले-बढ़े गुप्त जी का बौद्धिक आधार मुख्यत: स्वाध्याय और निजी अनुभव ही था. औपचारिक शिक्षा कम होने पर भी गुप्त जी ने समाज, संस्कृति और भाषा के साथ एक दायित्वपूर्ण रिश्ता विकसित किया. बीसवीं सदी के आरंभ से सदी के मध्य तक लगभग आधी सदी तक चलती उनकी विस्तृत काव्य यात्रा में उनकी लेखनी ने चालीस से अधिक काव्य कृतियां हिंदी जगत को दीं. राष्ट्रवादी और मानवता की पुकार लगातीं उनकी कविताएं छंदबद्ध होने के कारण पठनीय और गेय हैं. उनकी कविता संस्कृति के साथ संवाद कराती-सी लगती हैं. उन्होंने उपेक्षित चरित्रों को लिया. यशोधरा, काबा और कर्बला, जयद्रथ वध, हिडिम्बा, किसान, पंचवटी, नहुष, सैरंध्री, अजित, शकुंतला, शक्ति, वन वैभव आदि खंड काव्य उनके व्यापक विषय विस्तार को स्पष्ट करते हैं. साकेत और जय भारत उनके दो महाकाव्य हैं. संस्कृति और देश की चिंता की प्रखर अभिव्यक्ति उनकी प्रसिद्ध काव्य रचना भारत-भारती में हुई. उसका पहला संस्करण 1014 में प्रकाशित हुआ था. उसकी प्रस्तावना, जिसे लिखे भी एक सौ पांच साल हो गए हैं, आज भी प्रासंगिक है. गुप्त जी कहते हैं ‘यह बात मानी हुई है कि भारत की पूर्व और वर्तमान दशा में बड़ा भारी अंतर है. अंतर न कह कर इसे वैपरीत्य कहना चाहिए. एक वह समय था कि यह देश विद्या, कला-कौशल और सभ्यता में संसार का शिरोमणि था, और एक यह समय है कि इन्हीं बातों का इसमें सोचनीय अभाव हो गया है. जो आर्य जाति कभी सारे संसार को शिक्षा देती थी, वही आज पद-पद पर पराया मुंह ताक रही है.’
गुप्त जी का मन देश की दशा को देख कर व्यथित हो उठता है, और समाधान ढूंढ़ने चलता है. फिर वह स्वयं प्रश्न उठाते हैं ‘क्या हमारा रोग ऐसा असाध्य हो गया है कि उसकी कोई चिकित्सा ही नहीं है?’ इस प्रश्न पर मनन करते हुए गुप्त जी यह मत स्थिर कर पाठक से साझा करते हैं : ‘संसार में ऐसा काम नहीं जो सचमुच उद्योग से सिद्ध न हो सके. परंतु उद्योग के लिए उत्साह की आवश्यकता है. बिना उत्साह के उद्योग नहीं हो सकता. इसी उत्साह को उत्तेजित करने के लिए कविता एक उत्तम साधन है.’ इस तरह के संकल्प के साथ वह काव्य-रचना में प्रवृत्त होते हैं. उनकी खड़ी बोली हिंदी के प्रसार की दृष्टि से प्रस्थान विन्दु सरीखी तो है ही, उनकी प्रभावोत्पादक शैली में उठाए गए सवाल आज भी मन को मथ रहे हैं : ‘हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी?’ हमें आज फिर इन प्रश्नों पर सोचना और विचारना होगा और इसी बहाने समाज को साहित्य से जोड़ना होगा. शायद ये सवाल हर पीढ़ी को अपने-अपने देश-काल में सोचने चाहिए.
| Tweet |