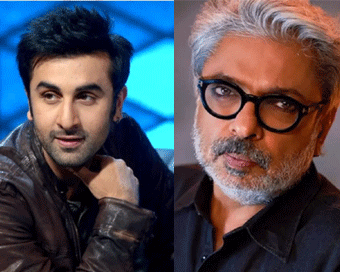विश्लेषण : गांव बचेंगे तो गाय भी
गाय और गोरक्षकों पर विवाद जारी है. देश में गोरक्षा की आड़ में जो हिंसा हो रही है, उसे लेकर संसद में भी चर्चा हो चुकी है.
 विश्लेषण : गांव बचेंगे तो गाय भी |
सरकार की तरफ से जो बयान दिया गया उसमें कई तरह के किंतु-परंतु के साथ हिंसा की आलोचना की गई. ये अलग बहस, विवाद और विचार का विषय है कि क्या प्रधानमंत्री की अपील के बाद जल्द ही गोरक्षा के नाम हिंसा और उन्माद रुक जाएगा. ये तो आने वाला समय बताएगा. पर इस मामले को अलग तरह से देखने की जरूरत भी है, जिसका संबंध गांव और खेती से है.
भारतीय खेती जब से आधुनिक होने की राह पर चली उसके पहले गांव और गाय एक ही संस्कृति के अविभाज्य अंग थे. गोसेवा या गोपालन के लिए से किसी राजनैतिक विचारधारा की जरूरत नहीं थी. किसी गोभक्त मंडली की आवश्यकता भी नहीं थी. गांव में रहने वाले, जिसमें ज्यादातर खेतिहर थे, गाय पालते थे. खेती के अलावा गोपालन-जिसमें गाय के अलावा बैल भी रहते थे, गांव की अर्थव्यवस्था का मूलाधार था. खेती हो नहीं सकती थी अगर आपके पास बैल न हों. बहुत पुरानी बात नहीं है. साठ सत्तर साल पुरानी है, जब गांव के धनी मानी किसान की सामाजिक हैसियत इस बात से मापी जाती थी कि उसकी खेती कितने हल की है. एक हल में दो बैल नथते हैं. बड़े कहे जाने वाले किसान आठ-दस-बीस हल की खेती करते थे. फिर गांव में अनाज को बाजार तक पहुंचाने के लिए बैलगाड़ी की भी बड़ी भूमिका थी. वहां भी बैल चाहिए था. बैलगाड़ी भी ग्रामीण कृषि जीवन का अनिवार्य अंग था. बैलगाड़ी की दूसरी सांस्कृतिक और सामाजिक भूमिकाएं भी थीं. फणीर नाथ रेणु की कहानियों को पढ़ने के क्रम में आज के आधुनिक और शहरी पाठक अनुमान लगा सकते हैं कि बैलगाड़ी किस तरह मेले में जाने के लिए उपयोग में लाया जाता था.
हिन्दी और रेणु की अमर कहानी (जिस पर फिल्म भी बनी) ‘तीसरी कसम’ के केंद्र में हिरामन है (हीराबाई के अलावा) जो बैलगाड़ी चलाता है. वह कहानी अभी भी पढाई जा रही है लेकिन बैल कहां गए, ये सवाल पूछनेवाले कम हो गए हैं. पर आज बैलगाड़ी का विदाई गीत लिखा जा चुका है. बैलगाड़ी के विलोप को औद्योगिक विकास प्रक्रिया के तहत अनिवार्य मान लिया गया है. आज के गांव में या रेलवे स्टेशनों पर हिरामन भी नहीं मिलेगा. कोई हीराबाई आज बैलगाड़ी पर बैठने को तैयार भी नहीं होगी. वैसे हीराबाई या उस जैसी भी अब नहीं मिलेंगी. पचास-साठ बरसों में ग्रामीण संस्कृति पूरी तरह बदल गई है. इसलिए न हिरामन रहा न हीराबाई. कुछ बैलगाड़ियां सुदूर इलाकों में हो सकती हैं. पर ज्यादातर गावों में नहीं है. इस तरह बैलों की सांस्कृतिक हैसियत भी खत्म हो गई. कुछ गरीब किसानों के पास एक हल के लिए दो बैल मिल सकते हैं. पर ऐसे ज्यादातर किसान बटाईदारी का काम करते हैं. पर जो बैल कभी धनी से लेकर मझोले किसानों के लिए आर्थिक हैसियत और सामाजिक शान के प्रतीक हुआ करते थे, वे दयनीय प्राणी बन गए हैं. आज अगर प्रेमचंद भी होते तो उनके लिए ‘दो बैलों की कथा’ जैसी कहानी लिखना असंभव होता. ये हिन्दी में एकमात्र कहानी है, जो बैल के भीतर निहित स्नेह की भावना को दिखाती है.
बहरहाल, विषयांतर होने से बचते हुए ये रेखांकित करना जरूरी है गोवंश-जिसमें गाय और बैल दोनों शामिल हैं, भारतीय कृषि के मेरुदंड कई हजार साल से रहे और इसी कारण वे भारतीय संस्कृति के महत्त्वपूर्ण घटक भी रहे. पर जैसे-जैसे भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण हुआ, ट्रैक्टर और थ्रेसर का उपयोग बढ़ा, बैल हाशिए पर चला गया. इस सिलसिले में पिछले दिनों अखबारों में एक खबर और (उसके साथ के चित्र) का उल्लेख हमें कुछ अंतदृष्टि दे सकता है. खबर (और चित्र) ये थी कि मध्य प्रदेश में एक किसान ने खेती की जुताई में बैलों की जगह अपनी दो बेटियों को लगा दिया. खबर (और चित्र) एक दिन की चर्चा बनी और खो गई. कोई राष्ट्रव्यापी बहस नहीं हुई कि आखिर किसान की हालत क्या हो गई है कि वह बैल रखने में आर्थिक हैसियत भी खोता जा रहा है. करते रहिए आप कागज पर कृषि का आधुनिककरण, जमीनी हकीकत कुछ और है.
खैर, हीरा और मोती (दो बैलों की कथा के बैलों के नाम) के कंधों पर से खेती के जुआठ का बोझ तो कम होता गया, लेकिन गाय का राजनैतिक कद बढ़ गया. वह दूध न या न दे, इसकी चिंता उनको तो है जो गाय पालते हैं लेकिन गोरक्षकों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन गाय पालनेवाले जानते हैं कि वे किस परेशानी में हैं. गांवों में सार्वजनिक चरागाह कम होते जा रहे हैं. कुछ अन्न उपजाने का दबाव और कुछ गावों में भी भू माफिया का प्रवेश दोनों वजहों से पशुओं के लिए चरागाह लगातार कम होते जा रहे है. बाजार से भूसा खरीदिए और गाय को खिलाइए. सुनने में एक छोटी बल्कि मजाकिया समस्या लगती है पर इसकी विकरालता का अनुभव तभी होगा जब आप छोटे गोपालक किसानों की बात सुनेंगे. पिछले हफ्ते मध्य प्रदेश विधान सभा में गांवों में गायों की वजह से फसलों के नुकसान पर भारी चर्चा हुई. पर उस चर्चा में गांव नहीं था.
यानी मूल बात ये कि गाय तभी बचेगी जब गांव बचेंगे. शहरों में प्लास्टिक खाकर मरती गाओं के दृश्य रोज देखने को मिल जाते हैं और सच्चाई तो ये है कि इनको देखते हुए भी लोग नहीं देखते. इस तरह शहरों में तो गाय असुरक्षित है. और गांवों में उसके लिए चारे या भोजन का संकट बढ़ता जा रहा है. गांव का पूरा परिवेश नष्ट हो रहा है. गांव, सिर्फ मशीनी खेती नहीं है. गांव अन्य चीजों के अलावा गोपालन और पशुपालन भी है. कई लोग तर्क दे सकते हैं कि इतिहास के रथ को अब पीछे धकेला नहीं जा सकता और पुराने और पारंपरिक गांव एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के कारण नष्ट होंगे ही. कोई रोक नहीं सकता. पता नहीं, इतिहास की अपरिहार्यता का सिद्धांत सच है या नहीं. पर इतना तो सच है कि आज के उजाड़ हो रहे गांवों में गाय असुरक्षित है. ऐसे में व्यावहारिक तो यही लगता है पहले गांव को बचाइए, गाय अपने आप बच जाएगी. पर क्या यह संभव है?
| Tweet |