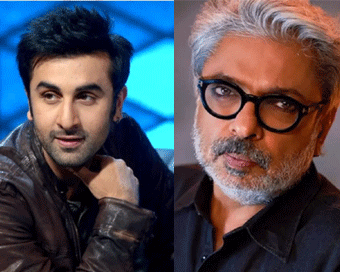मौद्रिक नीति : नीतिगत दरों में कटौती की आस
आज छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) नीतिगत दर पर फैसला करेगी. जून की मौद्रिक समीक्षा में एमपीसी ने खंडित फैसला किया था.
 मौद्रिक नीति : नीतिगत दरों में कटौती की आस |
बहरहाल, एमपीसी के परिचालन पद्धति पर सवाल उठाए जा रहे हैं. बीते महीनों में मुद्रास्फीति के मुद्दे पर एमपीसी के सदस्यों के विचारों में एकरूपता नहीं रही है.
अक्टूबर की मौद्रिक समीक्षा में कहा गया था कि मुद्रास्फीति का लक्ष्य प्राप्त करने योग्य है, लेकिन चिंता अगली मौद्रिक समीक्षा में देखी गई और उसके बाद से एमपीसी इसे लेकर लगातार परेशान है. हालांकि, हालिया मौद्रिक समीक्षा में एमपीसी ने स्वीकार किया कि मुद्रास्फीति के स्तर में कमी आई है. फिर भी वह कोर मुद्रास्फीति को लेकर इंतजार करने की नीति पर चल रहा है. वैसे, ज्यादा मुद्रास्फीति की उम्मीद, मुद्रास्फीति का उल्टा जोखिम, कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती आदि शब्दावलियों की वास्तविकता में नरमी बनी हुई है, जिसे अच्छा संकेत माना जा सकता है. शुरू में विमुद्रीकरण के प्रभाव को एमपीसी के सभी सदस्यों ने अस्थायी माना था, लेकिन इसे पिछले मौद्रिक समीक्षा में केवल एक सदस्य ने ही स्वीकार किया. सच कहा जाए तो अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2017 की दूसरी तिमाही से ही सुस्त पड़ गई थी, लेकिन इस प्रक्रिया में वित्त वर्ष 2017 की तीसरी एवं चौथी तिमाही में तेजी आई. एमपीसी के पहले कार्यवृत्त में अर्थव्यवस्था में मौजूद अप्रयुक्त क्षमता और निजी निवेश को लेकर चिंता जताई गई, लेकिन विमुद्रीकरण के कारण ये मुद्दे हाशिये पर चले गए.
पुनर्मुद्रीकरण के बाद फिर से हाशिये के मसले मुख्यधारा में वापिस आ गए हैं. एमपीसी के अंतिम कार्यवृत में सभी सदस्यों ने अर्थव्यवस्था में अप्रयुक्त क्षमता और निजी निवेश की मौजूदगी के मुद्दे को फिर से उठाया. इधर, ताजा आंकड़े मुद्रास्फीति के उल्टे जोखिम को ज्यादा नहीं बता रहे हैं. लिहाजा, नीतिगत दरों में कटौती की संभावना मौद्रिक समीक्षा में बन सकती है. रिजर्व बैंक ने वर्ष 2007 में विभिन्न देशों के एमपीसी के कामकाज पर एक अनुसंधान पेपर प्रकाशित किया था, जिसमें प्रमुख देशों के एमपीसी के परिचालन से जुड़े चौंकने वाले परिणाम सामने आए थे.
अनुसंधान में यह भी पाया गया था कि एमपीसी का निर्णय हर मामले में सही नहीं हो सकता है. एमपीसी संकल्पना के विविध आधार जैसे, स्वतंत्र सोच, तकनीकी कुशलता, विश्लेषण आदि हैं. वर्ष 2002 से वर्ष 2006 की अवधि के अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि सशक्त एमपीसी के निर्णयों की वजह से मुद्रास्फीति को तो नियंत्रित किया जा सका, लेकिन इससे विकास को गति नहीं मिल सकी. इसके विपरीत वर्ष 2009 से वर्ष 2015 की अवधि में सशक्त एमपीसी के सतर्कता के बावजूद मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी हुई और विकास को भी गति नहीं मिली.
इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि एमपीसी सही तरीके से मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में सफल नहीं रही है. मॉनसून की प्रगति संतोषजनक है. देशभर में लगभग 89 फीसद बारिश हो चुकी है. 27 जुलाई तक 36 में से 32 उपखंडों में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश हो चुकी है. समग्र रूप से देखा जाए तो सामान्य से 4 फीसद अधिक बारिश हो चुकी है. उत्तर-पश्चिम और मध्य क्षेत्र, जो अनाज एवं दाल के सबसे अधिक पैदावार करने वाले प्रदेश हैं, में भी सामान्य से क्रमश: 18 फीसद और 13 फीसद अधिक बारिश हो चुकी है. जीएसटी से आने वाले महीनों में मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की जा सकती है, क्योंकि जीएसटी के तहत 81 फीसद वस्तुओं को 18 फीसद के कर स्लैब में रखा गया है.
एमपीसी शुरू से ही कोर मुद्रास्फीति पर ध्यान केंद्रित किए हुए है, जबकि कोर मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2015 से ही एक ही स्तर पर बनी हुई थी, जो अब गिरकर 4 फीसद के स्तर पर आ गई है. मौजूदा स्थिति नीतिगत दर में कटौती की तरफ साफ तौर पर इशारा करती है. उम्मीद है कि रिजर्व बैंक वर्ष 2013 की तरह भूल नहीं करेगा, जब केंद्रीय बैंक ने मुद्रास्फीति के लंबे समय से 2 अंकों में रहने के बावजूद भी नीतिगत दरों में बढ़ोतरी नहीं की थी. विमुद्रीकरण के कारण बैंकों में जरूर अत्यधिक नकदी जमा हुई थी, लेकिन अधिकांश अतिरिक्त नकदी सरकारी प्रतिभूति के रूप में जमा है, जिसका इस्तेमाल बैंकों द्वारा करना संभव नहीं है. लिहाजा, कारोबार और विकास को गति देने के लिये इस बार नीतिगत दरों में 0.25% की कटौती की जा सकती है.
| Tweet |