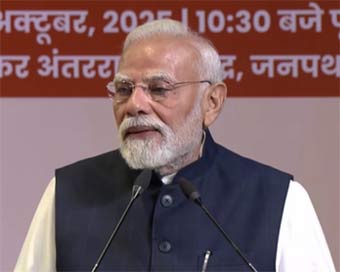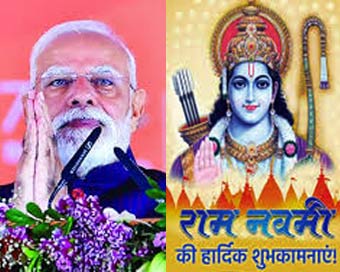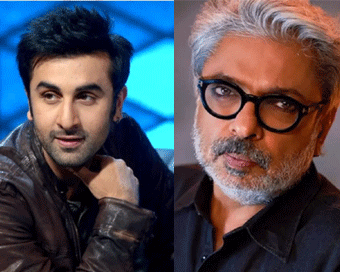विधायिका : नहीं जरूरी विशेषाधिकार
वर्ष 1453 में हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष थॉमस थोर्पे एक मामूली जुर्माना अदा न किए जाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए; सांसद स्ट्रोड को वर्ष 1512 में गिरफ्तार किया गया कि उनने ऐसे बिल संसद में पेश कर दिए थे, जो महारानी को नापसंद थे; इलियट, होल्लिस और वैलेंटाइन वर्ष 1629 में गिरफ्तार किए गए क्योंकि सदन में उनके भाषणों में महारानी को देशद्रोह झलका.
 विधायिका : नहीं जरूरी विशेषाधिकार |
संसदीय विशेषाधिकार लोकतंत्र के लिए चले लंबे संघर्ष का प्रतिफल हैं. राजशाही और संसद के बीच नागरिकों के अधिकारों को लेकर संघर्ष का परिणाम हैं क्योंकि किंग अपने खिलाफ बोलने वालों/बोल सकने वालों को गिरफ्तार करा देते थे. हमारे संसदीय लोकतंत्र में संसद के पास लगभग सर्वोच्च शक्तियां हैं, इसलिए सदस्यों को ऐसा कोई खतरा नहीं है, सो, विशेषाधिकारों की जरूरत नहीं है.
कर्नाटक विधान सभा के स्पीकर जब विधायक थे तो उनके और दो अन्य विधायकों के खिलाफ लिखने पर दो पत्रकारों को कर्नाटक विधान सभा द्वारा जिस तरह सजा सुनाई गई और जर्माना लगाया गया, उससे एक बार फिर विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध किए जाने और विधायिका के विशेषाधिकारों पर नागरिकों की अभिव्यक्ति के अधिकार को वरीयता देने को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. सर्चलाइट मामले में बिहार विधान सभा में कुछ शोरशराबा हुआ. संवाददाता ने अपनी रिपोर्ट भेजी और शाम के अखबार ने उसे छाप दिया. उस समय तक सदन इस समूचे प्रकरण को कार्यवाही से हटा चुका था. संपादक ने अभिव्यक्ति की आजादी के अपने अधिकार की दुहाई दी तो सदन और मुख्यमंत्री ने सदन की कार्यवाहियों पर नियंत्रण और उनके प्रकाशन संबंधी अपने अधिकार की बात कही. दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने विशेषाधिकारों को अभिव्यक्ति की आजादी पर तरजीह दी. इसके कुछेक वर्ष बाद ही उत्तर प्रदेश में एक और विवाद उभरा.
उप्र विधान सभा ने केशव सिंह नाम के व्यक्ति को सात दिन के कारावास की सजा सुनाई. सजा के सातवें दिन दो वकीलों ने केशव सिंह की रिहाई के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की. इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के दो जजों (जस्टिस बेग और जस्टिस सघल) ने केशव सिंह की रिहाई का आदेश करते हुए नोटिस जारी कर दिए. जब यह खबर विधान सभा पहुंची तो स्पीकर ने इसे गंभीरता से लिया. इसे सदन की अवमानना मानते हुए दोनों जजों को हिरासत में लेकर सदन के समक्ष पेश करने को कहा. जैसे ही न्यायाधीशों को इस बारे में पता चला वे तत्काल इलाहाबाद पहुंचे. अगले दिन हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ ने स्पीकर के आदेश पर स्थगनादेश दे दिया. ऐसे नाजुक मौके पर भारत के राष्ट्रपति ने इस जटिल मामले को सुप्रीम कोर्ट के पास भेज दिया ताकि उसकी राय जानी जा सके. शीर्ष अदालत की सात सदस्यीय पीठ ने सर्चलाइट मामले में दिए गए फैसले को एक बार फिर दोहराया. कहा कि प्रेस की आजादी और विधायिका के विशेषाधिकारों के मध्य विवाद के मामले में विशेषाधिकारों को तरजीह देनी होगी लेकिन विशेषाधिकार अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन जीने की आजादी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कमतर नहीं कर सकते.
तथ्य तो यह है कि विसंगतियों के लिए संविधान बनाने वाले दोषी हैं, जिनने विश्व के सर्वाधिक बड़े संविधान का मसौदा तैयार करते समय विधायी विशेषाधिकारों के व्यापक हिस्से को अपरिभाषित छोड़ दिया. राजेन्द्र प्रसाद इस प्रावधान को लेकर खुश नहीं थे, लेकिन उन्हें आस्त किया गया कि यह पूरी तरह से अस्थायी प्रावधान था. अनुच्छेदों 105 तथा 194 में स्पष्ट कहा गया है कि ‘विधायिका की शक्ति, विशेषाधिकार और विशेष संरक्षण विधायिका द्वारा तय और समय-समय पर परिभाषितानुसार तय होंगे, और, अगर उन्हें परिभाषित नहीं किया गया तो वे हाउस ऑफ कॉमन्स पर लागू प्रावधानों के मुताबिक होंगे.’ ‘अगर परिभाषित नहीं किया गया’ का तात्पर्य विशेषाधिकारों को परिभाषित करने की स्पष्ट शक्ति नहीं है. इतना ही नहीं, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वालों ने यह गलती भी कि भारतीय संसद को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के तुल्य रख दिया.
ब्रिटिश संविधान के तहत संसद सर्वोच्च है. भारत में संविधान सर्वोच्च है. इसलिए भारतीय विधायिका और ब्रिटिश संसद न केवल सामान्य राजनीतिक स्थिति बल्कि वैधानिक शक्तियों के मामले में भी भिन्न हैं. इसके अलावा, ब्रिटिश सदन ने स्वयं को अतीत से मुक्त कर लिया है. संसद या इसके सदस्यों के खिलाफ कृत्य और टिप्पणियां अब विशेषाधिकार के सवाल के तौर पर नहीं देखी जातीं. संसद और इसके सदस्यों को अपनी आलोचना सुनने को तैयार रहना पड़ता है. बीती दो सदियों से अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स सजा देने के अधिकार के बिना अच्छे से चल रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 1901 में हाउस ऑफ कॉमन्स जैसे विशेषाधिकार रखने का फैसला किया था, अब अतीत से छुटकारा पा चुका है. उसने 1987 में विशेषाधिकारों को संविदाबद्ध किया है.
हैरत ही तो है कि हमारे विधायक अपने भ्रष्टाचार को ढांपने के लिए न केवल विशेषाधिकारों को ढाल बनाते हैं, बल्कि अदालतों में यह तक दलील देते हैं कि वे ‘सार्वजनिक सेवक’ नहीं हैं. हरद्वारी लाल और एआर अंतुले मामलों में तो अदालत ने भी इस दलील को मानते हुए कहा था कि विधायक ‘सार्वजनिक सेवक’ नहीं हैं. हालांकि, पीवी नरसिंह राव मामले में उन्हें ‘सार्वजनिक सेवक’ करार दिया गया था. बहरहाल, जस्टिस एमएन वेंकटचेलैया की अध्यक्षता वाले संविधान समीक्षा आयोग ने सिफारिश की है कि विशेषाधिकारों को परिभाषित किया जाना चाहिए और विधायिकाओं के स्वतंत्र और निष्पक्ष कामकाज के लिए उनकी हदबंदी की जानी चाहिए. आज जब अदालत ने न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका कानून के जरिए बुनियादी अधिकारों की समूची अवधारणा का उदारीकरण कर दिया है, तो ऐसे में अभिव्यक्ति की आजादी विधायिका के विशेषाधिकारों से कमतर नहीं किए जाने चाहिए. आज की यह तात्कालिक जरूरत है कि प्रेस की आजादी के बरक्स विधायिका के विशेषाधिकारों पर नये सिरे से दृष्टिपात किया जाए.
| Tweet |