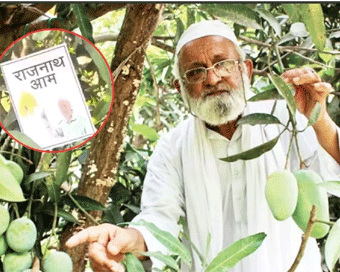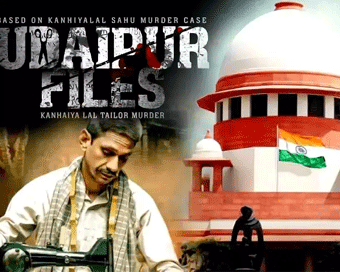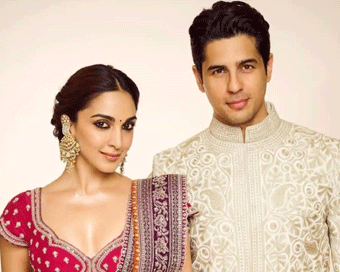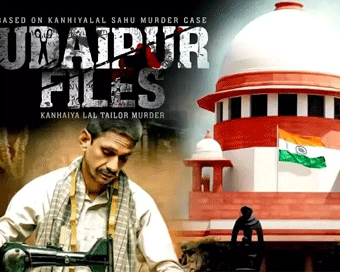विकास : आगे निकलने की होड़
पश्चिमी आधुनिकता के अंधानुकरण के साथ विकास का जो एक सपना पिछले एक-डेढ़ दशक से हमारे देश में जोरशोर से देखा जा रहा है,
 विकास : आगे निकलने की होड़ |
वह यह है कि हम जल्द ही कुछ ऐसा करें कि न्यूयॉर्क, शंघाई और टोक्यो जैसे महानगरों को मात दे सकें और दुनिया को दिखाएं कि आधुनिकता में हमारा कोई सानी नहीं है. विकास की इस होड़ का नतीजा है शहरों का गर्मी के ऐसे द्वीपों में बदल जाना जहां मौसम के अतिरेक लोगों के रहन-सहन को प्रभावित करने की स्थिति में आ गए हैं. पुणो स्थित भारतीय मौसम विभाग की इकाई और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटरोलॉजी ने हीट इंडेस्क के रूप में एक आकलन किया है, जिसमें इंसानों पर तापमान में होने वाली घट-बढ़ के कारण पड़ने वाले असर दर्शाए गए हैं. आकलन कहता है कि देश के ज्यादातर शहरों में मॉनसूनी वष्रा से लेकर गर्मी और नमी की अतिरंजनाएं दिखने लगी हैं, जो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर रही हैं.
देश के 23 शहरों की करीब साढ़े 11 करोड़ आबादी की जरूरतों के मद्देनजर शहरीकरण और उसकी जरूरतों ने शहरों को हीट-ट्रैपिंग ग्रीनहाउस, आसान शब्दों में कहें तो ऐसे गैस चैंबरों में बदल डाला है जो मौसम की अतियों का कारण बन रहे हैं. ये शहर क्यों ऐसे बन गए हैं, इसकी कुछ स्पष्ट वजहें हैं. जैसे, कम जगह में ऊंची इमारतों का अधिक संख्या में बनना और उन्हें ठंडा, जगमगाता व साफ-सुथरा रखने के लिए बिजली का अंधाधुंध इस्तेमाल करना.
मौसमी बदलाव के कारण प्राकृतिक गर्मी से मुकाबले के लिए जो साधन और उपाय आजमाए जा रहे हैं, उनमें कोई कमी लाना कोई नीतिगत बदलाव लाए बगैर संभव नहीं हो सकता है. अभी हमारे योजनाकार देश की आबादी की बढ़ती जरूरतों और गांवों से पलायन कर शहरों की ओर आती आबादी के मद्देनजर आवास समस्या का ही जो उपाय सुझा रहे हैं, उनमें शहरों की आबोहवा को बिगाड़ने वाली नीति ही ज्यादा नजर आती है. जैसे, एक उपाय यह है कि अब शहरों में ऊंची इमारतों को बनाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. पर क्या यह सही नजरिया है? कंक्रीट की ऊंची इमारतें सिर्फ आबोहवा पर ही नहीं बल्कि हमारी सामाजिक संरचना पर भी गहरा असर डालती है, और एक ऐसे समाज का निर्माण करती है, जो अपने आचार-व्यवहार में भी आक्रामक होता है.
वर्ष 2007 में, दिल्ली में इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर ट्रेडिश्नल बिल्डिंग, आर्किटेक्ट एंड अर्बेनिज्म (आईएनटीबीएयू) ने एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसमें भाग लेने आए आर्किटेक्टों और योजनाकारों ने ऊंची इमारतों के रूप में ग्लास टॉवरों और स्काईस्क्रैपरों के विव्यापी चलन को ‘राक्षसी और अमानवीय’ तक कह डाला था. इन विशेषज्ञों ने कहा था कि अगर ख्वाहिश भविष्य के शहरों के निर्माण की है, तो हमें और पीछे जाना चाहिए, जब लोग जमीन पर बने एक ही तल वाले मकानों में रहते थे. मकानों की बनावट भी सादा होती थी.
शहरी-नियोजन से जुड़े मशहूर विचारक लियॉन क्रेअर ने कहा था कि एक दिन दुनिया में ऐसा आना है,
जब न तो बिजली पैदा करने के लिए हमारे पास यूरेनियम और कोयला होगा और न वाहनों के लिए तेल, तो ऐसे में ऊंची इमारतों की लिफ्टें बंद हो जाएंगी. इमारतों की ऊंचाई बढ़ने के साथ ही शहरों के सीवरेज सिस्टम, कचरा निष्पादन व्यवस्था, बिजली और पानी का इंतजाम-इन सब पर भी भारी दबाव पड़ने लगेगा. इमारतों की ऊंचाई बढ़ते ही कचरे की मात्रा भी बढ़ेगी. इन इमारतों में रहने वाले लोग जब अपनी कारों से और सार्वजनिक परिवहन के साधनों से सड़कों पर आएंगे तो ट्रैफिक जाम की समस्या के अलावा ईधन जलने और गैसें निकलने से वातावरण में गर्मी और प्रदूषण में और भी इजाफा होगा. सिर्फ यही नहीं,
बहुमंजिली इमारतों में रहने के कारण सामाजिकता और सामुदायिकता की अवधारणा को गहरा आघात लगने की आशंका भी रहती है. लियॉन क्रेअर तो यहां तक कहते हैं कि तीन मंजिल से ज्यादा ऊंची इमारतें बनाना भावी यानी भविष्योन्मुखी सोच का परिचायक नहीं है. कुछ भारतीय योजनाकारों के मत में भी ऊंची इमारतें भारत के गांधीवादी नजरिये को भी आघात लगाती हैं. आर्किटेक्ट ए.जी.के. मेनन ने इस बारे में एक दफा कहा था कि अच्छा होगा यदि हम भावी शहरों के निर्माण के मामले में विकसित कहे जाने वाले पश्चिमी मुल्कों की नकल न करें. इस प्रवृत्ति से बचते हुए अपनी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाएं.
| Tweet |