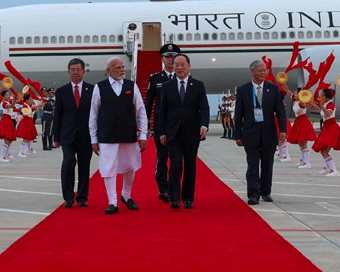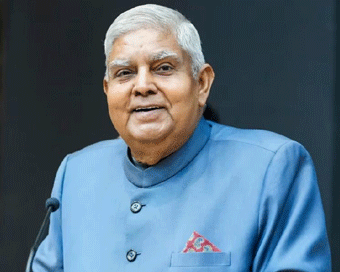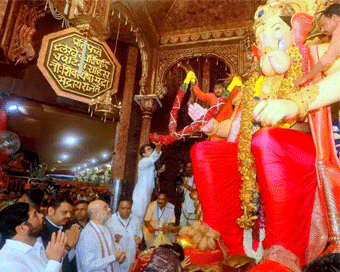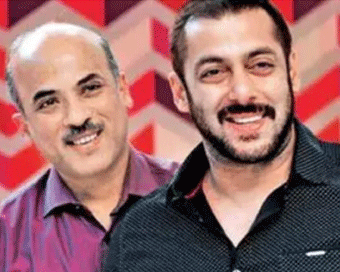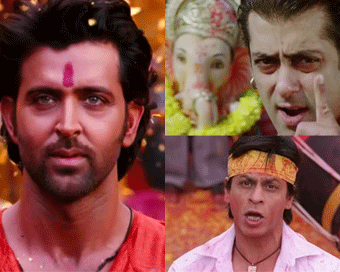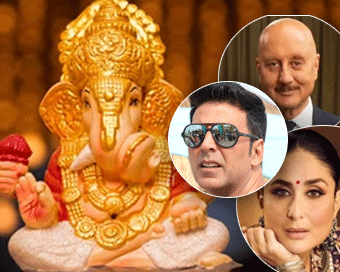बिहार में ई-वोटिंग : रच दिया इतिहास
देशमें मतदान के प्रति अरुचि प्रत्येक चुनाव में देखने में आती रही है। रोगग्रस्त या लाचारों को तो छोड़िए, उच्च शिक्षित वर्ग भी मतदान के प्रति सबसे ज्यादा उदासीन रहता है।
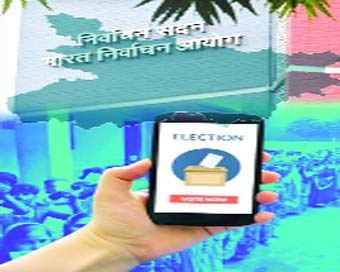 |
वैसे तो निर्वाचन आयोग मतदान का प्रतिशत और सुविधापूर्ण मतदान के लिए अनेक प्रयोग करता रहा है, लेकिन अब बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय के उपचुनाव में पहली बार ई-वोटिंग का प्रयोग करके इतिहास रच दिया है। मोबाइल से ई-मतदान की सुविधा के चलते बिहार के इस चुनाव में 80.60 प्रतिशत और उपचुनाव में 58.38 प्रतिशत मतदाताओं ने मोबाइल के जरिए मतदान किया। पहली महिला ई-वोटर विभा कुमारी और पहले पुरुष मतदाता मुन्ना कुमार बने। राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. दीपक प्रसाद ने मोबाइल से ई-मतदान कराए जाने की प्रेरणा यूरोपीय देश एस्टोनिया से ली थी।
चूंकि अब ई-वोटिंग का सफल प्रयोग हो चुका है, इसलिए भविष्य में इसका उपयोग बढ़ेगा। जो गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, विकलांग, असाध्य रोगों से ग्रसित और अपने मतदान स्थल से दूर रहने वाले लोग मतदान से वंचित रह जाते थे, उन्हें अब लोकतंत्र के इस महायज्ञ में भागीदार बनने की आसान सुविधा मिल जाएगी। समस्या का सामाधान बिना अतिरिक्त खर्च के हो जाएगा। चूंकि मतदान केंद्रों पर विभिन्न दलों का जमावड़ा नहीं होगा इसलिए निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान की संभावना बढ़ जाएगी। मतदान की निजता भी प्रभावित नहीं होगी। मतदान के प्रतिशत में आशातीत सुधार तो होगा ही जातीय और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की संभावनाएं भी न्यूनतम हो जाएंगी। ई-वोटिंग का काम पूर्वी चंपारण जिले की नगर पंचायत पकड़ी दयाल के अलावा पटना, बक्सर, रोहतास, सारण और बांका में सी-डैक और एसईआर के जरिए किया गया था।
बिहार के उपचुनाव में मोबाइल एप से ई-वोटिंग की प्रक्रिया प्रमाणित हो चुकी है। ई-वोटिंग को इसलिए भी अपनाया जाए क्योंकि पोस्टल वोटिंग का वैधानिक प्रावधान पहले से ही है। मतदान संपन्न कराने में जुटे कर्मचारी अपना वोट पोस्टल वोटिंग के जरिए ही देते हैं। अब कोई राजनीतिक दल और नेता बहाना नहीं बना सकता है कि इंटरनेट या बिजली की सुविधा दुर्गम क्षेत्रों में नहीं है। बिजली भले ही प्रत्येक गांव में न हो, लेकिन सौर ऊर्जा से बिजली और मोबाइल टॉवर गांव-गांव पहुंच गए हैं। इनके जरिए इंटरनेट की सुविधा हासिल कराई जा रही है। सौर जैसी वैकल्पिक ऊर्जा दूरदराज के गांवों में बिजली उपलब्ध करा रही है। फिर भी किसी गांव में बिजली नहीं है तो वहां ईवीएम के जरिए मतदान कराया जाए। हालांकि मोबाइल से ई-वोटिंग को लेकर कुछ नेता संदेह जता रहे हैं। उनका कहना है कि मोबाइल एप पर पंजीकरण में कठिनाई आएगी। गांव के प्रभावीशाली लोग दबाव बना कर फर्जी मतदान भी करा सकते हैं।
चुनाव विशेषज्ञों का मानना है कि 45 करोड़ लोग पलायन के चलते मतदान से वंचित हो जाते हैं। इस नजरिए से प्रवासियों के लिए ई-वोटिंग उपयोगी है। हालांकि चुनाव सुधार की दृष्टि से चुनाव आयोग ने घर से दूर रहने वाले अर्थात दूरस्थ मतदाताओं के लिए रिमोट वोटिंग सिस्टम (आरवीएस) तैयार किया है। इस मशीन की मदद से मूल मतदान स्थल से दूर दूसरे राज्य या शहर में रहने वाले मतदाता लोक सभा और विधानसभा चुनाव में मत का प्रयोग कर सकते हैं यानी मतदान के लिए उन्हें अपने मूल निवास स्थल पर आने की जरूरत नहीं रह गई हैं। आयोग द्वारा इसे लागू करने से पहले आने वाली कानूनी, प्रशासनिक और तकनीकी चुनौतियों पर राजनीतिक दलों के विचार भी आमंत्रित किए जाएंगे। चुनाव सुधार की दृष्टि से यह पहल अमल में आती है तो ऐतिहासिक होगी। नतीजतन, उन 45 करोड़ लोगों को वोट डालने का अवसर मिलेगा जो अपने घरों से दूर रहते हैं।
अनेक चुनाव विशेषज्ञ इस प्रणाली को क्रांतिकारी पहल मान रहे हैं। बेशक, आरवीएम की परिकल्पना क्रांतिकारी है। आईआईटी, मद्रास की मदद से ‘मल्टी कॉन्स्टीचुएंसी रिमोट ईवीएम’ के रूप में ऐसा मतदान उपकरण तैयार किया गया है, जो एक रिमोट मतदान केंद्र से 72 निर्वाचन क्षेत्रों में प्रवासियों का मतदान कराने में सक्षम होगा। लोकतंत्र की मजबूती के लिए आदर्श स्थिति यही है कि हरेक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करे। इस नाते 2005 में भाजपा के एक सांसद लोक सभा में ‘अनिवार्य मतदान’ संबंधी विधेयक लाए भी थे लेकिन समर्थन नहीं मिल पाने के कारण यह विधेयक पारित नहीं हो सका। कांग्रेस और अन्य दलों ने इस विधेयक के विरोध का कारण बताया था कि दबाव डाल कर मतदान कराना संविधान की अवहेलना है क्योंकि संविधान में मतदान करना मतदाता का स्वैच्छिक अधिकार तो है, लेकिन वह इस कर्त्तव्य-पालन के लिए बाध्यकारी नहीं है। लिहाजा, वह इस राष्ट्रीय दायित्व को गंभीरता से न लेते हुए उदासीनता बरतता है।
हमारे यहां आर्थिक रूप से संपन्न-सुविधा भोगी जो तबका है, वह अनिवार्य मतदान को संविधान में दी निजी स्वतंत्रता में बाधा मानते हुए इसका मखौल उड़ाता है। मतदान की अनिवार्यता अथवा ई-वोटिंग या आरवीएम से सुविधा का मतदान कथित अल्पसंख्यक व जातीय समूहों को ‘वोट बैंक’ की लाचारगी से भी छुटकारा दिलाएगा। राजनीतिक दलों को भी तुष्टिकरण की राजनीति से निजात मिलेगी क्योंकि जब प्रवासियों को आरवीएम से मतदान की सुविधा मिल जाएगी तो किसी धर्म, जाति या क्षेत्र विशेष से जुड़े मतदाताओं की अहमियत खत्म हो जाएगी। नतीजतन, उनका संख्या बल जीत-हार को प्रभावित नहीं कर पाएगा। लिहाजा, सांप्रदायिक और जातीय आधार पर ध्रुवीकरण की जरूरत नगण्य हो जाएगी। जब पंजाब और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की छाया थी, तब वहां हुए विधानसभा चुनावों में 15 से 20 प्रतिशत मतदान से ही सरकारें बनती रही हैं। साफ है कि यह स्थिति लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। अधिकतम मतदान के हालात ई-वोटिंग एवं आरवीएम के इस्तेमाल से निर्मिंत होते हैं, तो भारतीय राजनीति संविधान के उस सिद्धांत का पालन करती दिखेगी जो सामाजिक न्याय और समान अवसर की बात कहता है।
(लेख में विचार निजी हैं)
| Tweet |